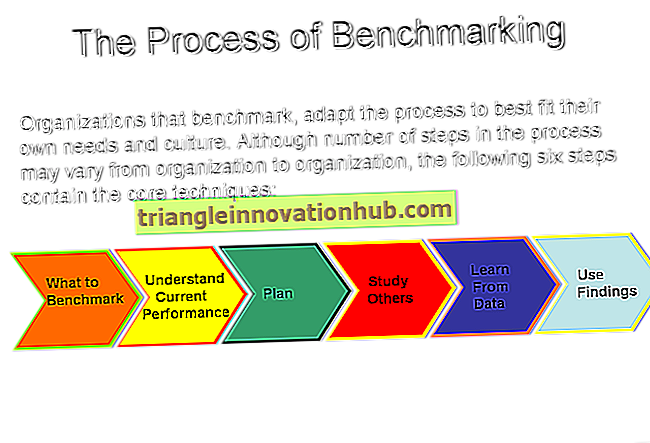राधाकमल मुखर्जी: जीवनी और समाजशास्त्र में योगदान
राधाकमल मुखर्जी: जीवनी और समाजशास्त्र में योगदान!
राधाकमल मुखर्जी (1889-1968), डीपी मुखर्जी के साथ - लखनऊ विश्वविद्यालय में उनके सहयोगी - और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जीएस घोरी को भारत में समाजशास्त्र में एक महान अग्रणी माना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। विजयवर्गीय की छात्रवृत्ति के तहत - राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी और डीएन मजुमदार - लखनऊ जल्द ही सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गए और यह 1960 के दशक के मध्य तक बना रहा। यहां हमारी चर्चा मुख्य रूप से राधाकमल मुखर्जी पर है।
जीवन रेखा:
राधाकमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से देश-शहर बेरहामपुर (मुर्शिदाबाद) में एक बड़े बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले सोलह वर्ष इस कस्बे में बिताए। उनके पिता एक वकील थे और बार के नेता थे। वह इतिहास में बड़ी रुचि के साथ एक कुशल विद्वान थे।
मुखर्जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेरहामपुर में की थी। वह बेरहामपुर के कृषिनाथ कॉलेज गए। उन्हें भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थान - प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में एक अकादमिक छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने इस कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास में अपना सम्मान पाठ्यक्रम लिया। यहां, वे एचएम पेरिवल, एम। घोष, अरबिंदो घोष के भाई और भाषाविद् हरिनाथ डे जैसे विद्वानों के संपर्क में आए।
प्रेसीडेंसी कॉलेज के एक शानदार छात्र, मुकर्जी ने कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, बैजहोट, हॉबहाउस और गिडिंग्स के कार्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ा। लेकिन, समाज के सबसे गरीब तबके की स्थितियों के बीच सामाजिक जीवन को समझने में उनकी रुचि 1905-6 के स्वदेशी के दिनों में जनता के साथ उनके संपर्क का परिणाम थी। उनकी देशभक्ति ने कलकत्ता में झुग्गीवासियों के बीच उनके शैक्षिक कार्यों में अभिव्यक्ति पाई। "जनता के बीच केवल शैक्षिक और सामाजिक कार्य चुपचाप हो सकते हैं ... राजनीतिक उत्पीड़न द्वारा कली में डुबाए बिना पीछा किया जाता है"।
अपने जीवन की इस अवधि के दौरान, मुखर्जी ने वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में खुद को लॉन्च किया, जो अंत तक उनका हित बना रहा। उन्होंने 1906 में कलकत्ता के मेकाहुबाजार की मलिन बस्तियों में एक एडल्ट इवनिंग स्कूल शुरू किया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरल ग्रंथ भी लिखे।
पुनर्जागरण, विशेष रूप से बौद्धिक और राजनीतिक किण्वन, विशेष रूप से लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के कारण, राधाकमल में देशभक्ति की ज्वाला और पीड़ित जनता के लिए कुछ करने की उत्सुकता पैदा हुई। इतिहास की प्राथमिकता में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उनकी रुचि इसी की अगली कड़ी थी।
1910 में, मुखर्जी ने बेरहामपुर में अपने अल्मा मेटर के साथ अर्थशास्त्र में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया। वह वहां पांच साल तक रहे। यह उनके जीवन का सबसे व्यस्त काल था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने आर्थिक, भारतीय अर्थशास्त्र की नींव जैसे अपने शुरुआती कार्यों को लिखा। इस समय, वह प्रसिद्ध बंगाली मासिक, उपासना के संपादक भी बने।
1915 के दौरान, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पीड़न किए गए थे, मुखर्जी को एक दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके सभी वयस्क स्कूलों को समाप्त कर दिया गया था। उसके खिलाफ आरोप थे कि वह एक 'आतंकवादी' था या वयस्क शिक्षा के भेस में आतंकवाद के साथ सहानुभूति रखता था। उनके वकील भाई के प्रयासों से उन्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया गया। उन्हें पंजाब के लाहौर कॉलेज में एक पद की पेशकश की गई थी। वह राजनीति में किसी भी रुचि का अंकुर करते हुए इस प्रकार वहां गया।
वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में वापस चले गए जहाँ पर आशुतोष मुकर्जी ने 1917 में पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल ऑफ़ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना की थी। वे वहाँ पाँच साल रहे और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक दर्शन पढ़ाया। उन्हें 1915 में प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति और 1920 में (कलकत्ता विश्वविद्यालय) की उपाधि “भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन” के अध्ययन के लिए प्रदान की गई।
1921 में, वे लखनऊ विश्वविद्यालय में उस दिन अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में शामिल हुए जब विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू किया। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में 1952 तक लगभग तीस वर्षों तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ाया। वह 1945 से 1947 तक ग्वालियर राज्य सरकार के आर्थिक सलाहकार और 1955 से 1957 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1958 में, वे निदेशक बने। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी और लखनऊ विश्वविद्यालय का मानव संबंध। इस प्रकार, वह अपनी मृत्यु तक लखनऊ में रहे, 1925 से 1940 तक पटना, कलकत्ता और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में अंतर्कलह के साथ।
मुखर्जी ने 1937, 1946 और 1948 में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में व्याख्यान देने के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोलोन, वियना, हार्वर्ड, कोलंबिया, शिकागो, मिशिगन और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालयों का भी दौरा किया। वे एफएओ के अध्यक्ष, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी आयोग में मनोनीत थे। 1946 में कोपनहेगन, 1947 में विश्व खाद्य परिषद, वाशिंगटन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य और इसके शासी निकाय की सीटों के लिए देशों के नामों की सिफारिश करने के लिए ILO की तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।
सैद्धांतिक निरूपण:
रामकृष्ण मुखर्जी (1979) के अनुसार, चूंकि मानव संस्थान व्यक्ति, समाज और मूल्यों की एक अविभाज्य एकता बनाते हैं, इसलिए उनके मूल्य घटक के बिना सामाजिक तथ्यों पर कोई विचार असत्य है; इसके बजाय, 'अनुभवजन्य' और 'मानक' समाजशास्त्र का एक संलयन होना चाहिए, इसलिए, एक मुक्त समाज में समानता और सहयोग के माध्यम से मनुष्य का विकास संभव है, न कि विरोधाभास और संघर्ष के माध्यम से।
राधाकमल मुखर्जी की समाजशास्त्र की दृष्टि, हालांकि भारतीय परंपरा में निहित थी, अभी भी सार्वभौमिक थी। उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत पर आधारित समाजशास्त्र के एक सामान्य सिद्धांत को विकसित करने की संभावना को देखा। भारतीय मामले में यह सिद्धांत भारतीय दर्शन और परंपरा से लिया जाएगा।
पद्धति:
आर्थिक क्षेत्र और भारतीय समाज के संपूर्ण सामाजिक-ऐतिहासिक-सांस्कृतिक क्रम के बीच अन्योन्याश्रयता का पता लगाने के लिए संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हुए, world ट्रांसडिसिप्लिनरी ’दृष्टिकोण का उपयोग भारतीय विश्व संदर्भ में सामाजिक वास्तविकता के व्यापक मूल्यांकन के लिए किया जाना था। मुखर्जी ने भारत में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में तुलनात्मक तरीकों के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा: "हमें नस्ल और संस्कृति की उत्पत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन का लक्ष्य रखना चाहिए।"
सील द्वारा भारत के विशिष्ट संदर्भ में वास्तविकता की जांच करने के लिए, गेड्स द्वारा अपने अनुभवजन्य विवरणों में प्रकट करने के लिए, और अर्थशास्त्र में उनके बुनियादी प्रशिक्षण के प्रकाश में, मुखर्जी ने आर्थिक समाजशास्त्र और मानव पारिस्थितिकी में क्षेत्र की जांच और ग्रंथ सूची अनुसंधान के साथ अपने शोध करियर की शुरुआत की। । उन्होंने अनुभवजन्य क्षेत्र की जांच में अपनी रुचि बनाए रखी और जीवन भर अपने छात्रों को इस संबंध में प्रोत्साहित किया।
हालांकि, समय के साथ, मुखर्जी साम्राज्यवाद बहुआयामी बन गया, जो मानवीय संस्थानों के वैचारिककरण के आसपास केंद्रित था, जो व्यक्ति, समाज और मूल्यों से बनी एक अदृश्य एकता के गठन के रूप में था। अर्थशास्त्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, राधाकमल ने आर्थिक समाजशास्त्र में समस्याओं के सूक्ष्म-स्तरीय विश्लेषण, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि की समस्याओं (1926, 1927), जनसंख्या की समस्याओं (1938) और भारतीय श्रमिक वर्ग की समस्याओं के साथ शुरू किया। (1945)।
1920 के दशक के उत्तरार्ध में, जब महान अवसाद में स्थापित किया गया था, तब उन्होंने बिगड़ते कृषि समाधानों और अवध (1929) में किसानों की स्थितियों की सूक्ष्म-स्तरीय जांच शुरू की थी। यह अध्ययन भारत में कृषि संबंधी अध्ययनों में एक गति-सेटर होना चाहिए था, लेकिन 1940 के दशक में बंगाल में कृषि संरचना पर अध्ययन की एक श्रृंखला का संचालन करने वाले रामकृष्ण मुखर्जी को छोड़कर, भारतीय ग्रामीण समाज के इस पहलू को 1960 के दशक तक उपेक्षित किया गया।
इंग्लैंड में सामाजिक नृविज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, राधाकमल ने स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म-स्तरीय अनुभवजन्य क्षेत्र की जांच में अधिक सक्रिय रुचि ली। इनमें 'अंतर-जाति तनाव' और 'शहरीकरण', विशेष रूप से संक्रमण वाले शहरों (1991, 1952, 1963 और 1964) और जैसे अध्ययन शामिल थे।
मजे की बात यह है कि मानव-समाजों और सामाजिक संस्थाओं के तत्वमीमांसा और बहुआयामी दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रति उनकी भविष्यवाणी के साथ सह-अनुभवजन्य समाजशास्त्र में उनकी भागीदारी मौजूद है। उन्होंने सोचा कि समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान निचले क्रम के अनुभवजन्य वास्तविकताओं द्वारा लॉग इन किया गया था और उच्चतर आदेशों को भूल रहे थे जिनके कानून और प्रक्रियाएं उन्हें नियंत्रित करती थीं।
उन्होंने दार्शनिक नृविज्ञान की वकालत और अभ्यास किया। लगभग मेटा-थ्योरिटिकल परिप्रेक्ष्य में, वह व्यक्तिगत, समाज और मूल्यों को एक स्पष्ट त्रिमूर्ति के रूप में देखने के लिए गए, लेकिन वास्तव में एक अविभाज्य एकता (1931, 1949, 1950, 1956 और 1965)। इस अर्थ में, राधाकमल भारतीय सामाजिक विज्ञान में एक अंतःविषय दृष्टिकोण के अग्रणी थे।
लेखन:
मुखर्जी ने कई मुद्दों पर लगभग 53 किताबें लिखीं। उनके लेखन की मूल प्रकृति सामाजिक विज्ञानों का एकीकरण है। वह कई क्षेत्रों में पथ-प्रदर्शक रहे हैं। उनके कई छात्र और सहयोगी अपने लेखन में इस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
उनका योगदान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है:
(1) अंतःविषय का विकास, बल्कि, समाज का अध्ययन करने में पार-अनुशासनिक दृष्टिकोण,
(२) सामाजिक पारिस्थितिकी और क्षेत्रीय समाजशास्त्र, और
(3) मूल्यों का समाजशास्त्र या मूल्यों की सामाजिक संरचना।
पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक जीवन के बारे में ज्ञान में उनके योगदान के बारे में टिप्पणी करते हुए, प्रसिद्ध दार्शनिक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सही ढंग से देखा: "भारतीय हितों के बारे में उनकी सोच को आधार बनाने के लिए (मुकर्जी की) क्या दिलचस्पी है, उनकी धारणा है कि मानव जीवन संपूर्ण है और नहीं हो सकता है टुकड़ों में अध्ययन किया।
समाजशास्त्र या मनुष्य का विज्ञान मूल्यों के प्रश्न को अनदेखा नहीं कर सकता है। सामाजिक विज्ञान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और यदि इस ज्ञान को मनुष्य की भलाई या भलाई के लिए नियोजित करना है, तो हमें मूल्यों की भावना विकसित करनी चाहिए। मुखर्जी की महान महत्वाकांक्षा बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिए काम करना है। ”
तत्वमीमांसा और 'आदर्शवाद' के प्रति एक पूर्वाग्रह हालांकि मुखर्जी के पहले के लेखन में देखा गया जैसे:
1. तीन तरीके: एक सामाजिक आदर्श के रूप में पारगमन की सूची-धर्म (1929)
2. समाजशास्त्र और रहस्यवाद (1931)
3. द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ़ मिस्टिकिज़्म (1937)
मुखर्जी के अन्य महत्वपूर्ण लेखन इस प्रकार हैं:
1. इंडियन इकोनॉमिक्स की नींव (1916)
2. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था (1926)
3. क्षेत्रीय समाजशास्त्र (1926)
4. भारत की भूमि समस्याएँ (1927)
5. सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय (1928)
6. अवध के क्षेत्र और किसान (1929)
7. मनुष्य का क्षेत्रीय संतुलन (1938)
8. आदमी और उसकी आदत (1940)
9. अर्थशास्त्र का संस्थागत सिद्धांत (1940)
10. भारतीय श्रमिक वर्ग (1945)
11. मूल्यों की सामाजिक संरचना (1949)
12. नैतिकता की गतिशीलता: नैतिकता का एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सिद्धांत (1950)
13. अंतर-जाति तनाव (सह-लेखक) (1951)
14. दौड़, भूमि और भोजन (1946)
15. कला का सामाजिक कार्य (1948)
16. सामाजिक संरचना का मूल्य (1949)
17. सोसाइटी का एक सामान्य सिद्धांत (1956)
18. द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस (1960)
19. मेट्रोपोलिस की सामाजिक रूपरेखा (1963)
20. मानव मूल्यों का आयाम (1964)
21. द डेस्टिनी ऑफ़ सिविलाइज़ेशन (1964)
22. भारतीय कला का फूल (1964)
23. संक्रमण में जिला शहर: गोरखपुर का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण (बी। सिंह के साथ) (1964)
24. मैनकाइंड की एकता (1965)
25. मानवता का मार्ग: पूर्व और पश्चिम (1968)
26. भारत में सामाजिक विज्ञान और योजना (1970)।
हम यहाँ निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, जिन्हें हम मुखर्जी के लेखन में सार्थक पाते हैं:
1. भारतीय संस्कृति और सभ्यता
2. समाज का सिद्धांत
3. सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा
4. आर्थिक लेनदेन और सामाजिक व्यवहार
5. व्यक्तित्व, समाज और मूल्य
6. समुदायों का समुदाय
7. शहरी सामाजिक समस्याएं
8. सामाजिक पारिस्थितिकी
भारतीय संस्कृति और सभ्यता:
मुकर्जी (1964) भारतीय कला और वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति पर विस्तार से लिखते हैं। उनका मानना है कि एशियाई कला का उद्देश्य सामूहिक विकास है। उनके अनुसार, सद्भाव जीवन का मूल मूल्य है। उन्होंने इस सौहार्द को पिछले युगों के जीवन की भारतीय योजना में सचित्र पाया। भारतीय संस्कृति ने मनुष्य को एक समुदाय के जिम्मेदार सदस्य के रूप में देखा है। मनुष्य अलग-थलग नहीं है।
इस संदर्भ में, मुखर्जी लिखते हैं: “एशिया में कला लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल की मशाल वाहक बन गई…। ओरिएंटल कला को समुदाय की भावना के साथ सबसे अधिक गहन रूप से चार्ज किया जाता है और इस प्रकार ओरिएंटल संस्कृतियों की ऐतिहासिक निरंतरता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ”इसके विपरीत, पश्चिम में इस तरह के कलात्मक प्रयास व्यक्तिवाद पर हावी थे या यह महसूस करना कि कला अपने आप में एक अंत था। यह सिर्फ सामाजिक एकजुटता या आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल नहीं था।
भारतीय कला सामाजिक या नैतिक क्षेत्र में अंतर्निहित है। मुखर्जी लिखते हैं: “भारत के असंख्य मंदिर, स्तूप और विहार एक और नैतिकता, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के बीच की कड़ी के साक्षी हैं। भारत में कला एक दूसरे के साथ लोगों की बातचीत का एक स्थायी घटक है जो ठोस रूप में लोगों की आकांक्षाओं और उनकी सामाजिक रचनात्मकता के बीच सक्रिय संबंध बनाता है। ”
भारतीय कला लगातार धर्म से जुड़ी हुई है। मुखर्जी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म जैसे भारतीय धर्मों के बड़े पैमाने पर गैर-आक्रामक स्वभाव से प्रभावित हैं। विविधता की सहिष्णुता की भावना धरमशस्त्रों में भी परिलक्षित होती है। ये कोड समुदायों के जातीय विविधता को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीले हैं।
मान्यताओं या रीति-रिवाजों के एक विशेष सेट के बजाय अंतिम सत्य पर जोर देना, भारतीय धर्मों की निरंतर विशेषता रही है। यह धर्म की शांतिपूर्ण एजेंसी के माध्यम से है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से परे सीलोन (श्रीलंका) और दक्षिण-पूर्व के देशों में फैली हुई है। इसलिए, भारतीय प्रभाव कई देशों में युद्ध या विजय के माध्यम से नहीं बल्कि मित्रता और सद्भावना के माध्यम से फैलते हैं।
समाज का सिद्धांत:
राधाकमल मुखर्जी ने मानव जीवन की समझ के प्रति अंतःविषय या ट्रांस अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने समाज के एक सामान्य सिद्धांत को विकसित करने की मांग की। इसे प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले, उन्होंने मनुष्य के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान और विज्ञान के बीच की बाधाओं को तोड़ने का प्रस्ताव दिया।
दूसरे, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञानों के संकलन को भी टाला जाना चाहिए। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच निरंतर बातचीत होनी चाहिए। भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान मानव व्यक्तित्व के कई आयामों और प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक वातावरण के साथ इसकी बातचीत की पर्याप्त रूप से सराहना करने के लिए आवश्यक है।
सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा:
मुखर्जी का समाज का सामान्य सिद्धांत एक सार्वभौमिक सभ्यता के मूल्यों की व्याख्या करना चाहता है। उन्होंने 'सभ्यता' शब्द का प्रयोग समावेशी अर्थ में किया है; संस्कृति इसका हिस्सा है। उनका प्रस्ताव है कि मानव सभ्यता का तीन परस्पर स्तरों पर अध्ययन किया जाना चाहिए।
य़े हैं:
1. जैविक विकास
2. सर्वांगासन
3. आध्यात्मिक आयाम
1. जैविक विकास:
मानव के जैविक विकास ने सभ्यता के उदय और विकास को सुविधाजनक बनाया है। उनके पास सक्रिय एजेंट के रूप में पर्यावरण को बदलने की क्षमता है। जानवर केवल एक पर्यावरण के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसे विभिन्न तरीकों से ढाल सकते हैं। जैविक प्रजाति के रूप में मानव, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर काबू पाने और सहयोग (सहजीवन) प्राप्त करने में सक्षम हैं।
2. सर्वांगासन:
सामाजिक मनोविज्ञान में, लोगों को अक्सर नस्ल, जातीयता या राष्ट्रवाद के ढांचे के भीतर दर्शाया जाता है। मनुष्यों को छोटे स्वयं या अहंकारियों के कैदी के रूप में देखा जाता है, जिनका दृष्टिकोण पारसवादी या जातीय है। इसके विपरीत, मनुष्यों में संकीर्ण भावनाओं को दूर करने और सार्वभौमिकता प्राप्त करने की क्षमता है, अर्थात स्वयं को बड़ी सामूहिकता जैसे कि एक राष्ट्र या स्वयं ब्रह्मांड के सदस्य के रूप में पहचानना।
इस प्रक्रिया में, सामान्य मूल्य विशिष्ट मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों के अधीन करने में मदद करते हैं। मुखर्जी के लिए, नैतिक सापेक्षवाद, जिसका अर्थ है कि मूल्य समाज से समाज में भिन्न होते हैं, वर्तमान समय में मददगार नहीं है। नैतिक सार्वभौमिकता की आवश्यकता है, जो मानव जाति की एकता की पुष्टि करती है। नए परिप्रेक्ष्य में, पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र नैतिक एजेंट बन जाते हैं जो मानवता को बांधने वाले सामान्य किस्में को पहचानने में सक्षम हैं। वे अब विभाजन या सापेक्षता से निर्धारित नहीं होते हैं।
3. आध्यात्मिक आयाम:
मुकर्जी मानते हैं कि सभ्यता का आध्यात्मिक आयाम है। मानव धीरे-धीरे पारलौकिक ऊंचाइयों को छू रहा है। इसका अर्थ है कि वे भौतिक और भौतिक सीमाओं के आधार पर, बायोजेनिक और अस्तित्व के स्तर की बाधाओं को पार करके आध्यात्मिकता की सीढ़ी तक बढ़ रहे हैं। इस प्रयास में, कला, मिथक और धर्म 'आवेग' या ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बल प्रदान करते हैं।
जैसा कि सामाजिक विज्ञान ने इन सांस्कृतिक तत्वों को नजरअंदाज किया है, वे आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम हैं। मुखर्जी के लिए, मानव जाति की एकता, पूर्णता और पारगमन की खोज सभ्यता की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालती है। इस संबंध में, उन्होंने भारतीय और चीनी सभ्यताओं की प्रशंसा की, जो 6 ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से स्थिर संस्थाओं के रूप में थी। उनकी ताकत उनके सार्वभौमिक मिथकों और मूल्यों से ली गई है जो आध्यात्मिक खोज को बढ़ावा देते हैं।
आर्थिक लेनदेन और सामाजिक व्यवहार:
किसी विशेष अनुशासन में बहुत अधिक विशेषज्ञता मनुष्य के अस्तित्व और व्यवहार का केवल एकतरफा या आंशिक दृष्टिकोण दे सकती है। अर्थशास्त्र के अपने संस्थागत सिद्धांत में, मुखर्जी ने दिखाया है कि भारतीय पश्चिमी अर्थशास्त्र और यह ज्यादातर स्वदेशी व्यापार, हस्तशिल्प और बैंकिंग में पारंपरिक जाति नेटवर्क की उपेक्षा करता है। इसने आर्थिक विकास को मुख्य रूप से मौद्रिक अर्थशास्त्र या बाजार की घटना के विस्तार के रूप में देखा। अर्थशास्त्र में पश्चिमी मॉडल बाजार और औद्योगिक केंद्रों पर केंद्रित था।
भारत जैसे देश में, जहां जाति या जनजाति के ढांचे के भीतर बड़ी संख्या में आर्थिक लेन-देन होते हैं, बाजार का मॉडल केवल एक सीमित प्रासंगिकता है। भारतीय सेटिंग में आर्थिक विनिमय पारंपरिक नेटवर्क से प्रभावित हुआ है। भारत के दोषी और जाति गैर-प्रतिस्पर्धी प्रणाली में काम करते रहे हैं।
आर्थिक विनिमय के नियम काफी हद तक सामाजिक या सामूहिक जीवन के मानदंडों से लिए गए थे। समूहों के बीच अंतर-निर्भरता या गैर-प्रतिस्पर्धा को भारतीय परंपरा के मानदंडों में बल दिया गया है। उन्होंने स्वार्थ को बढ़ावा देने पर जोर नहीं दिया है लेकिन मानव जीवन के समुचित लक्ष्य के रूप में समुदाय की भलाई की पूर्ति पर प्रकाश डाला है।
भारत में आर्थिक मूल्यों को सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सरासर जैविक या भौतिक ड्राइव आर्थिक लेनदेन उत्पन्न नहीं करते हैं। धार्मिक या नैतिक बाधाओं ने हमेशा आर्थिक गतिविधियों को एक दिशा दी है।
मान लोगों के दैनिक जीवन में प्रवेश करते हैं और उन्हें सामूहिक रूप से स्वीकृत तरीकों से कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक भूखी ऊंची जाति के हिंदू गोमांस नहीं खाते; इसी तरह, एक रूढ़िवादी मुस्लिम या यहूदी सुअर का मांस नहीं खाएंगे, हालांकि, भोजन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, आर्थिक व्यवहार को हमेशा सामाजिक जीवन या सामूहिकता से अलग मानना गलत है।
व्यक्तित्व, समाज और मूल्य:
अपनी पुस्तक व्यक्तित्व में, राधाकमल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक एजेंट के रूप में देखते हैं, जो निर्णय लेता है और विकल्प बनाता है, और मूल्य-पूर्ति चाहता है। मनुष्य (i) स्वयं, (ii) अन्य, और (iii) ब्रह्मांड से संबंधित मूल्यों के संदर्भ में विकल्प बनाता है।
बेशक, आदमी दो तरह के प्रभावों के अधीन होता है। एक ओर, प्रकृति, पर्यावरण और जैविक ड्राइव और जरूरतों के प्रभाव हैं। उन्हें जोड़ें मनुष्य के मनोवैज्ञानिक आवेग हैं। दूसरी ओर, समाज या सामूहिकता का दबाव है। मानव व्यक्तित्व इन दो प्रभावों से बहुत प्रभावित होता है।
लेकिन, यह उनके द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। मानव व्यक्तित्व में दोनों प्रकार के दबावों को पार करने का गुण होता है। यह स्वयं को भी पार कर सकता है। वास्तव में, व्यक्तित्व को मुखर्जी द्वारा "विभिन्न आयामों में समायोजन की व्यक्ति की विशिष्ट विधा का योग" के रूप में परिभाषित किया गया है:
(i) जैविक,
(ii) सामाजिक, और
(iii) आदर्श, लौकिक या पारलौकिक ”।
मानव व्यक्तित्व पर्यावरण के साथ एक जैविक और सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवहार करता है। लेकिन, यह उससे कुछ ज्यादा है। यह "लौकिक संपूर्ण के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक संपूर्ण उत्तरदायी" है। मुखर्जी के अनुसार, "व्यक्तित्व अनिवार्य रूप से पारगमन है"। पुरुष या महिला की निजता का एक सामाजिक आयाम है।
लेकिन, वह / वह अपने / अपने साथी प्राणियों से अलगाव चाहते हो सकता है ताकि वे खुद को और खुद के बीच एक साम्य स्थापित कर सकें। उसे अपने भीतर की स्वतंत्रता का एहसास करने के लिए सामाजिक दबावों से मुक्ति की आवश्यकता हो सकती है। समाज और उसके मूल्य प्रणाली का कार्य व्यक्तित्व के विकास को सुविधाजनक बनाने में निहित है जो एक मुफ्त एजेंट होगा।
राधाकमल के अनुसार, "संरचनाओं और कार्यों का योग जिसके माध्यम से मनुष्य खुद को तीन आयामों या उसके स्तरों के स्तर के अनुसार देखता है:
(ए) पारिस्थितिक,
(बी) मनो-सामाजिक, और
(ग) नैतिक ”।
इस प्रकार, समाज "जीवन की स्थिति और मूल्य-पूर्ति की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है"।
मान:
मान “सामाजिक रूप से अनुमोदित इच्छाएँ या लक्ष्य हैं जिन्हें कंडीशनिंग और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। वे व्यक्तिपरक वरीयताओं, मानकों और आकांक्षाओं को उत्पन्न करते हैं। "मान एक निर्धारित पैटर्न में अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को उन्मुख करने में मनुष्य की मदद करते हैं। इस प्रकार, मनुष्य अपूर्ण जैविक ड्राइव के आंतरिक तनावों या संघर्षों को हल करता है। इसके अलावा, वह उचित मूल्यों की मदद से अपने साथी पुरुषों के साथ सामंजस्यपूर्ण सामाजिक भूमिकाओं और व्यवस्थित संबंधों को प्राप्त करने में सफल होता है।
इच्छाओं, लक्ष्यों, आदर्शों और मानदंडों में कटौती की अवधारणा। सामाजिक क्रिया में इच्छाएँ लक्ष्य हैं। आदर्श का निर्माण एक काल्पनिक सामाजिक स्थिति में किया गया है जो लक्ष्यों के टकराव की विशेषता है। आदर्शों के विरोध या विरोधाभास के मानदंड हैं। वे ब्रह्मांड के परे एक मानव, दूरसंचार आदेश को दर्शाते हैं।
मुखर्जी द्वारा सामाजिक रिश्तों को पुरुषों के व्यवहार और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उनके सामान्य लक्ष्यों और मूल्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। समूह, मुखर्जी के अनुसार, समान रूप से सामाजिक संबंधों और संबद्ध व्यक्तियों के व्यवहार हैं जो एकीकरण और उनके सामान्य लक्ष्यों और मूल्यों की पूर्ति से निकलते हैं। समूह की तुलना में संस्थाएं अधिक स्थायी हैं। संस्थानों को अधिक संगठित औपचारिक और स्थायी सामाजिक संबंधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कुछ सामान्य और स्थिर लक्ष्यों और व्यक्तियों के मूल्यों को पूरा करते हैं।
स्थिति संस्थागत सेट-अप के भीतर विशिष्ट स्थिति में व्यक्ति की क्षमता और उपलब्धि को संदर्भित करती है। एक समाज का संस्थागत नेटवर्क मैट्रिक्स प्रदान करता है जहां कई भूमिकाएं पूरक बन जाती हैं और समाज और व्यक्तित्व के लक्ष्यों और मूल्यों की पूर्ति और एकीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं।
आधुनिक समाजों के लिए मूल समस्या मूल्यों का निर्माण और पोषण करना है जो एक ओर मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देगा और दूसरी ओर सद्भाव के आदेश और एकजुटता की व्यापकता।
पश्चिम में विकसित सामाजिक विज्ञानों ने आध्यात्मिक व्यक्तिवाद को प्रतिपादित किया:
मैं। सबसे पहले, यह मनुष्य और उसकी परमाणु इच्छाओं और वरीयताओं को अपने कुल समूह और संस्थागत स्थिति से अलग करने की गलती करता है।
ii। दूसरे, सामाजिक विज्ञानों के परमाणुवाद और तर्कवाद ने मानवीय मूल्यों के विशाल क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया है जो कि आंशिक के बजाय प्रतिस्पर्धी, अभिन्न हैं, और यह व्यक्तित्व के परिपक्वता और सामाजिक संस्कृति में सुधार दोनों को चिह्नित करता है।
iii। तीसरे, तर्कसंगत और परमाणु व्यक्ति की धारणा अनुभवजन्य समाजशास्त्र और नैतिकता या तत्वमीमांसा के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा करती है। अनुभवजन्य समाजशास्त्रीय अध्ययन सामाजिक संरचना और प्राकृतिक विज्ञान और नैतिकता अध्ययन मूल्यों की विधि के माध्यम से कार्य करता है। पश्चिमी सामाजिक विज्ञानों में दो का द्वंद्ववाद गलत धारणा देता है कि मूल्यों का उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
मुखर्जी के अनुसार, मूल्यों और औसत दर्जे के तथ्यों के बीच का अंतर गलत है। मान और मूल्य सामाजिक प्रक्रिया में सत्यापित और मान्य किए जा सकते हैं।
यह तीन पदों द्वारा वहन किया जाता है:
मैं। सबसे पहले, मूल्य एक स्थिर और सुसंगत तरीके से मनुष्य के बुनियादी आवेगों और इच्छाओं को पूरा करने और एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अर्थ है कि स्वार्थी इच्छाओं और हितों को सामूहिक जीवन द्वारा संशोधित किया जाता है, जहां लोग एक दूसरे से देते हैं और लेते हैं।
ii। दूसरे, मूल्य सामान्य दायरे में हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण दोनों से बने हैं। मूल्य उनके प्रतीक के माध्यम से सभी द्वारा साझा किए जाते हैं। प्रतीक आमतौर पर साझा किए गए मूल्यों के संघनित या उपकृत अभिव्यक्ति हैं। राष्ट्रीय ध्वज, उदाहरण के लिए, एक सामान्य प्रतीक है जो एक राष्ट्र का गठन करता है।
iii। तीसरी बात, विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के मूल्यों की विविधता और विचलन के बावजूद, कुछ सार्वभौमिक मूल्य वनीय हैं।
मूल्यों का एक क्रम सामाजिक एकीकरण के चार स्तरों पर पाया जाता है:
(1) भीड़ में एक सहज, हालांकि क्रूर, मूल्य की अभिव्यक्ति है - उदाहरण के लिए, नैतिक आक्रोश, आदि, व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ निर्देशित।
(२) आर्थिक हित समूह में, कुछ मौलिक मूल्य व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि पारस्परिकता, अखंडता, विचार, निष्पक्षता स्तर; वे अवैयक्तिक संघर्ष और प्रतिशोध के लिए अतिसंवेदनशील हैं।
(3) 'समाज' या 'समुदाय' में, इक्विटी और न्याय अभिव्यक्ति पाते हैं।
(४) 'सामान्य' में, मुख्य मूल्य 'सहज प्रेम', और सामाजिक सह-सहयोग हैं। संसार के पुनर्निर्माण के लिए ये मूल्य आवश्यक हैं। संक्षेप में, मुखर्जी कई संदर्भों में मूल्यों से संबंधित हैं।
मान हमेशा अव्यवस्थाओं के साथ होते हैं। किसी व्यक्ति की शिथिलता और सामाजिक कमियों के कारण अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। अव्यवस्थाएं केवल व्यक्तिगत विचलन में ही नहीं बल्कि संस्थागत विचलन (आपराधिक गिरोह आदि) में भी व्यक्त की जाती हैं। मुखर्जी ने अव्यवस्थाओं के उपचार पर जोर दिया। वह कुल सामाजिक स्थिति और व्यक्तियों और समूहों के सामाजिक अनुकूलन पर काम करके धर्मनिष्ठ व्यक्तियों और समूहों को फिर से संगठित करेगा।
अपने दो कामों में, द डायनामिक्स ऑफ मोरल्स एंड द डाइमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मुखर्जी एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य से नैतिकता पर चर्चा करते हैं। वह मनुष्य को स्वार्थ को पार करने और एक सार्वभौमिक भाईचारे को प्राप्त करने की आवश्यकता को संदर्भित करता है। नैतिक अतिक्रमण की ओर आंदोलन लगभग एक अपरिहार्य विकास बन जाता है। यह विशेष रूप से एक दुनिया में सच है, जो हिंसा और कलह से ग्रस्त है।
समुदाय का समुदाय:
मानव विकास के आयाम में:
जैव-दार्शनिक व्याख्या, मुखर्जी ने क्रमिक आयामों में विकास में जीवन, मन और समाज के रचनात्मक, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण सिद्धांतों की खोज की, जबकि द फिलॉस्फी ऑफ़ पर्सनैलिटी और द डाइमेंशन ऑफ़ वैल्यूज़: एक एकीकृत सिद्धांत दोनों में, उन्होंने पारस्परिक प्रकृति पर बल दिया है मानव अस्तित्व और पारगमन, और एकता, आपसी भागीदारी और सभी मूल्यों और संभावनाओं का संलयन।
द कम्युनिटी ऑफ़ कम्युनिटीज़ की पुस्तक मानव सांप्रदायिकता और समुदाय की समझ और व्याख्या के लिए खुले मानव व्यक्ति-संचार में समान समकालीन सेमिनल विचार का उपयोग करने और विकसित करने का प्रयास करती है। मानव व्यक्ति, मूल्य और समुदाय सभी एकता और परिवर्तन हैं।
आम तौर पर, मनुष्य अपने ब्रह्मांड और उसके संसाधनों को जीवन के मूल्यों, संवर्धन और विस्तार के लिए विकसित नहीं करता है, विकास की निरंतर रचनात्मक, पारगमन प्रक्रिया में मूल्य और समुदाय। समुदाय का दर्शन इसे "एक ब्रह्मांड, एक समुदाय" के पैटर्न के रूप में दर्शाता है।
यह विश्व विज्ञान, संचार और सभ्यता की समग्र एकता के भीतर दोनों व्यक्तियों और प्रजातियों के लिए मानव विकास की संभावनाओं को चौड़ा करता है। इस संदर्भ में, समुदाय के दर्शन का अर्थ है, होमो युनिवर्सिसिटी के मूल्यों और संभावनाओं के समुदाय और ब्रह्मांड के साथ मनुष्य की अप्रत्याशित भूमिका का गहन अध्ययन।
विकास में समुदाय का अर्थ निम्न आयामों के स्तर पर भिन्न होता है:
1. जैविक
2. मनोवैज्ञानिक
3. नैतिक
4. दार्शनिक
5. मेटाफिजिकल
जैविक आयाम में सच्चे समुदाय में होमो सेपियन्स की पूरी प्रजाति शामिल होती है जो मानव मूल्यों और संस्कृति के माध्यम से विकास के मनोवैज्ञानिक चरण का मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। मनोवैज्ञानिक आयाम पर सच्चा समुदाय मनुष्य के आत्म-विस्तार और होमो सर्वव्यापी में होमो सेपियन्स के परिवर्तन या परिवर्तन पर निर्भर करता है, जो स्वयं और समुदाय के आत्म मूल्यों और आत्म-अभिव्यक्ति के लिए अनंत मूल्यों और संभावनाओं दोनों के लिए खुद को सुरक्षित करता है।
सभी आयामों और महाद्वीपों से संबंधित, नैतिक आयाम पर, अपने समुदाय के लोगों के साथ सच्चा समुदाय खुद को मनुष्य के महत्वपूर्ण संवाद में शामिल करता है। दार्शनिक आयाम पर सच्चा समुदाय मानव जाति और ब्रह्मांड के आंतरिक सद्भाव और जैविक एकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और आदेश, पूर्णता और अस्तित्व की एकजुटता में विश्वास का प्रतीक है।
अंत में, आध्यात्मिक आयाम पर, सच्चा समुदाय स्वयं और सार्वभौमिक अन्य या समुदाय के समुदाय के बीच पहचान की सच्चाई का एहसास करता है, जिसमें मानव प्रेम सक्षम है, और इस सत्य को प्रत्येक पारस्परिक संबंधों में मानव जीवन में हर लक्ष्य और प्रयास में सक्षम बनाता है। और मान।
समकालीन आदमी के इतिहास को अपने संचार और संवाद को बढ़ाकर और अपने ब्रह्मांड को बढ़ाने और गहरा करने के द्वारा अपने विकासवादी रुझान को मजबूत करना चाहिए, जिससे यह उनके अर्थ, मूल्यों और संभावनाओं के लिए अधिक प्रासंगिक हो।
शहरी सामाजिक समस्याएं:
मुखर्जी ने श्रमिक वर्ग की समस्याओं के लिए एक समृद्ध दृष्टिकोण की परिकल्पना की है। भारत में औद्योगीकरण, जो पिछले कई दशकों से हो रहा है, विविध क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों को एक साथ लाने में सफल रहा। लेकिन, मुंबई, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरी केंद्रों में कामगारों की रहन-सहन की स्थिति स्लम जीवन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। औद्योगिकीकरण के शुरुआती दिनों में, शहरी मलिन बस्तियों ने वेश्यावृत्ति, जुआ और अपराध जैसे दोषों को जन्म दिया। इसलिए, अपनी आर्थिक और नैतिक स्थितियों में सुधार के लिए श्रमिकों के जीवन में भारी बदलाव लाना आवश्यक था।
आज, कई निजी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अपने श्रमिकों को सामाजिक कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों ने विधायी कृत्यों को बढ़ावा दिया है, जो नियोक्ताओं के लिए बाध्यकारी हैं। हालांकि, असंगठित श्रमिक (अर्थात, जो बेरोजगार हैं, या अस्थायी रूप से कार्यरत हैं) मलिन बस्तियों में रहना जारी रखते हैं।
वर्तमान में भारतीय मलिन बस्तियों में व्याप्त समस्याएँ अवैध शराब और नशीली दवाओं, अपराधों, और बिगड़ती आवास स्थितियों और नागरिक सुविधाओं की खपत हैं। इसलिए, मुखर्जी का मजदूर वर्ग का विश्लेषण भारत में वर्तमान औद्योगिक संगठन के लिए भी प्रासंगिक है।
सामाजिक पारिस्थितिकी:
मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उसे समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ रहना चाहिए और प्रकृति या पर्यावरण या पारिस्थितिकी के साथ भी। राधाकमल मुखर्जी का 'सामाजिक पारिस्थितिकी' नामक अध्ययन में योगदान अद्वितीय है। सामाजिक पारिस्थितिकी, एक अनुशासन के रूप में, सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान के एक सदस्य के सहयोग की आवश्यकता है।
भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर पारिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक स्थितियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों द्वारा भी वातानुकूलित हैं। दरअसल, मानव या सामाजिक पारिस्थितिकी मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन है।
अपनी पुस्तक, क्षेत्रीय समाजशास्त्र (1926) में, मुखर्जी ने मानव पारिस्थितिकी के क्षेत्र की व्याख्या "पौधे, पशु और मानव समुदायों के संतुलन के एक सुसंगत अध्ययन के रूप में की है, जो क्षेत्र के संगठन में सहसंबद्ध कार्यशील भागों की प्रणाली हैं" पारिस्थितिक अध्ययन में अमेरिकी अग्रदूतों ने पारिस्थितिक संबंधों की अपनी अवधारणा में संस्कृति के कारक पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।
वे ऐसे संबंधों को देखते थे जो पौधों और जानवरों के बीच होते हैं। मुखर्जी ने तर्क दिया कि मनुष्य के बीच पारिस्थितिक संबंध काफी हद तक निचले जीवों के साथ समान हैं। लेकिन, मानव के मामले में, सांस्कृतिक मानदंडों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव पारिस्थितिकी इस तथ्य को उजागर करती है।
Formation क्षेत्र ’सामाजिक आदतों जैसी एक पारिस्थितिक इकाई के निर्माण में मूल्य और परंपराएँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। समान या समान मूल्यों वाले व्यक्तियों में एकजुटता होती है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण जिसमें मनुष्य के निरंतर प्रयास, आकांक्षाएं और आदर्श पारिस्थितिक बलों और प्रक्रियाओं के साथ चुपचाप मिलते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी मनुष्य और क्षेत्र के बीच कभी जटिल रूप से जटिल संबंध देती है।
पारिस्थितिकी और समाज के बीच एक निश्चित संबंध है। पारिस्थितिक क्षेत्रों का विकास एक गतिशील प्रक्रिया का परिणाम है जो पर्यावरण की चुनौती है और निपटान स्थापित करने वाले लोगों की प्रतिक्रिया है। Ecological balance is not achieved by a mechanical carving out of a territory and setting people therein.
Such an attempt weakens or destroys the social fabric. For example, in building industrial plants or constructing irrigation plants or constricting irrigation dams in India, very often, people of the concerned locations are moved to new settlements. It seriously affects community's life of the people. As a people lives in an area, it develops a symbiotic relationship with the ecology or environment of the area. In the new situation it may fail to develop that kind of relationship with the surrounding.
Mukerjee's ideas about social ecology advocated regional development. He stood for a balance between economic growth and ecological fitness. Traditional crafts and skills like weaving or engraving should be revamped for attaining economic growth of a region without any great damage to its ecology. Deforestation has created havoc. Long back Mukerjee cautioned his countrymen against it. He strongly advocated for conservation of forests and protection of ecological balance.
Mindless urbanization was also lamented by Mukerjee. From the ecological point of view he upheld the idea and process of urbanization. Urban development at the expense of the countryside should be kept in check. Agriculture should be diversified and industries should be decentralized.
Mukerjee notices with concern that (i) overgrazing, (ii) improvident destruction of trees and scrubs, and (iii) faulty method of cultivation brings about a serious imbalance in the biophysical constitution of the entire region. It seriously impairs nature's cycle.
Removal of vegetation brings about a chain of unfavourable reactions such as:
(1) Denudation of the top soil,
(2) Fall in the underground water level,
(3) Diminution of rainfall,
(4) Increase of aridity, and
(5) Acceleration of 'river', sheet or gully and wind erosion. These have led to serious and continuous agricultural deterioration.
Industrial civilization, because of its mindless exploitation of natural resources, finds its “security threatened due to the exhaustion of coal and petroleum” and the diminishing supply of minerals and vitamins, which cannot be synthetically manufactured. The importance of ecological values can hardly be overemphasized even in the industrial society.
Of course, there is no need for loss of nerves. Man's success in his adaptation to the geographical environment rests on certain ideal values, which have their roots in ecological values. But it is necessary that these values should “have reached the level of standards of moral behaviour”.
निष्कर्ष:
It may be viewed from the above analysis that Radhakamal Mukerjee advocated a methodology reflecting the organic interdependence between the economic sphere and the entire socio-historical cultural order [see, eg, A General Theory of Society (1956); The Philosophy of Social Sciences (1968)]. He proposed, therefore, a trans disciplinary approach to social research at a time when some social scientists in India were considering the need for interdisciplinary research.
Mukerjee has pioneered three approaches to social science for which he would always be remembered:
1. Conceiving economics as a specialization, and not as a discipline, in the realm of social science.
2. Introducing the 'institutional approach' to planning which should not be regarded as the exclusive prerogative of the economists but should be treated under the rubric of social science.
3. Raising the sight of appraisal of social reality from the uni-disciplinary or interdisciplinary outlook of the social scientists to a trans disciplinary perspective, bearing in mind the common acceptance of the term 'social sciences' comprising various 'disciplines' like economics, political science, psychology, and sociology and so on.
Mukerjee started his career as an economist who, in those days, defined the framework of reference to the 'discipline' as the relation between man and his exploitation of the natural resources in successively compounded forms.
At that time, the Marxists had raised the issue, but they were not seriously considered by the establishment of economics. Mukerjee was not a Marxist, but he clearly conceived economics as dealing with the relationship among humans with respect to the exploitation of natural resources and the consequent production and appropriation of material goods and services.
In his voluminous writing in this context, Mukerjee examined the nexus of human relationships in the totality of life and living. But that was transcending the boundary of economics as a discipline, which he regarded as a specialization within the unitary discipline of social science. This viewpoint was not acceptable to the contemporaneous mandarins in the 'economic' science; nor was Mukerjee acceptable to the contemporaneous mandarins of sociology or any other social science 'discipline'. Therefore, Mukerjee became a bratya, a marginal man in the realm of social science.
However, Mukerjee's empirical studies on various aspects of life conditions (eg, land problem, working class, town and village life, ecology, food planning, etc.) were more and more appreciated on their own merit; that is, irrespective of the theoretical underpinning to these efforts and achievements of Radhakamal.
But his advocacy of 'institutional planning' was not so readily accepted. As we live in a lunar world, where light is reflected from the sun rising in the West, the social scientists became vocal about institutional planning after Gunnar Myrdal posed it (1971) in terms of transplantation of the 'modernizing ideals' from the First (and the Second) to the Third World.
In his last years, Mukerjee postulated the need for a fusion of 'empirical' and 'normative' sociology in order that social engineering will have its disposal reliable knowledge concerning human behaviour, goals and values as well as means and techniques of analysis and feasible devices for social control [see, eg, A Philosophical View of Civilization (1963); The Oneness of Mankind (1965)].
Although, his last writings were somewhat speculative in nature, however, he is distinguished among the pioneers of Indian sociology as one who clearly specified his factual foundations, arguments and proposals regarding what Indian sociology was in his time and how it should develop.
Mukerjee did not give adequate importance to the part played by conflicts in actual social life. He upheld the cause of harmony between man and man, one nation and another, between different regions, between human groupings and biological environment. His stress on the importance of values of understanding and toleration, moral responsibility of the individual to the community and human responsibility for protecting ecology would be considered very important by the students of sociology, even today.
That intellectual freedom is a precondition for an advancement of science and of the frontiers of knowledge was the basic faith of the founding fathers of Indian sociology and social anthropology. This explains why, despite their own preferences for certain perspectives and methodologies, their students could contribute appreciably to the development of alternative conceptual framework for studying Indian society – its structure and change in the post-1950 period.