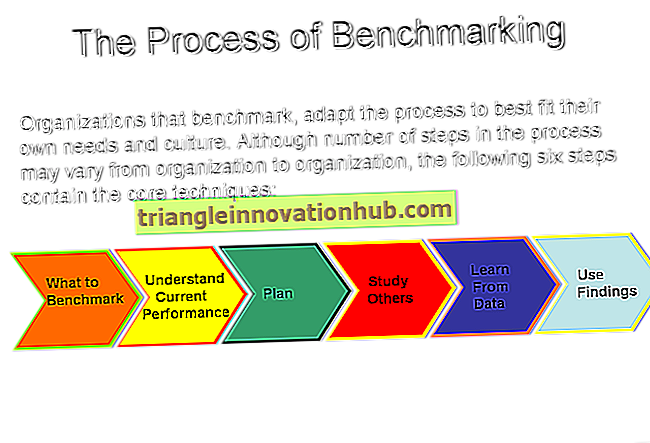धूर्जती प्रसाद मुखर्जी: जीवनी और समाजशास्त्र में योगदान
धूर्जती प्रसाद मुखर्जी: जीवनी और समाजशास्त्र में योगदान!
धूर्जती प्रसाद मुखर्जी (1894-1961), जिन्हें लोकप्रिय रूप से डीपी कहा जाता है, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक पिता में से एक थे। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1894 को पश्चिम बंगाल में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था, जिनकी बौद्धिक गतिविधियों की काफी लंबी परंपरा थी।
प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, सत्येन बोस के अनुसार, जब डीपी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उन्होंने बोस की तरह, विज्ञान का अध्ययन करना चाहा, लेकिन अंतत: अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए बस गए। उन्हें अर्थशास्त्र और इतिहास में एमए मिला, और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप ने इसे रोक दिया।
डीपी ने कलकत्ता के बंगबासी कॉलेज में अपना करियर शुरू किया। 1922 में उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में व्याख्याता के रूप में नव स्थापित लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वह बत्तीस साल की एक लंबी अवधि के लिए वहाँ रहे। डीपी को लखनऊ लाने की जिम्मेदारी विभाग के पहले प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी की थी।
वह 1954 में प्रोफेसर और विभाग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। एक वर्ष (1953) के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान, हेग में समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिस पर उन्होंने अपने पिछले पांच वर्षों के सक्रिय शैक्षणिक जीवन के दौरान बड़े गौरव के साथ कब्जा किया था। वह भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे। वह अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के उपाध्यक्ष भी रहे।
डीपी एक उत्कृष्ट भारतीय थे जिनके बहुमुखी हितों ने न केवल समाजशास्त्र के क्षेत्र में बल्कि अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला में भी स्थान बनाया है। फिर भी, उनके युगानुयुग योगदान से समाजशास्त्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है। डीपी, एक विद्वान होने के अलावा, एक बेहद संस्कारी और संवेदनशील व्यक्ति थे।
उनका व्यक्तित्व उनके संपर्क में आने वाले युवाओं को प्रभावित करने और ढालने में अपनी शक्ति के लिए उल्लेखनीय था। वह एक मार्क्सवादी थे, लेकिन उन्हें मार्क्सवाद के एक सामाजिक वैज्ञानिक यानी मार्क्सवादी कहलाना पसंद करते थे। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का विश्लेषण किया।
एक विद्वान के रूप में:
शायद उनके लेखन की तुलना में अधिक महत्व उनके व्याख्यान, चर्चा और वार्तालाप थे। यह उनके माध्यम से था कि उन्होंने युवाओं के दिमाग को आकार दिया और उन्हें अपने लिए सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। "शेपिंग मैन मेरे लिए काफी हैं", उन्होंने अक्सर अपने छात्रों से कहा।
ज्ञान के विविध क्षेत्रों पर उनकी आज्ञा अतुलनीय थी; उन्होंने दर्शन की प्रणालियों की सूक्ष्मताओं, आर्थिक विचारों के इतिहास, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और कला, साहित्य और संगीत के सिद्धांतों पर समान सुविधा के साथ बात की।
उन्होंने एक अनूठे तरीके से एक बहुत अच्छी तरह से विकसित महत्वपूर्ण संकाय के साथ एक गहन छात्रवृत्ति को संयुक्त किया, जिसने उन्हें आज पुरुषों और संस्कृति के सामने आने वाली समस्याओं के लिए सभी विद्वानों के विवरणों से संबंधित होने में सक्षम बनाया। विचार की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की प्रतिभा में, उनके पास कोई सहकर्मी नहीं था। डीपी के इन गुणों ने असंख्य छात्रों को प्रेरित किया है और वे जो कुछ भी करते हैं, उसमें उनका गहरा प्रभाव है।
डीपी संस्कृति के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी था। यह काम एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास है, जो उसके दिल के लिए प्रिय था। यह केवल एक मामूली प्रयास है और इसमें कई कमियां हो सकती हैं लेकिन हमें लगता है कि विचारों का एक अभिसरण है जो एक एकीकृत विषय बनाते हैं। आशा है कि यह कार्य संबंधित क्षेत्रों में समाजशास्त्रियों और विद्वानों के बीच रुचि पैदा करेगा।
भारतीय इतिहास पर उनके काम में:
ए स्टडी इन मेथड, डीपी इतिहास को समझने के लिए मार्क्सवादी पद्धति की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। वह किसी भी समाज को समझने के लिए दर्शन और ऐतिहासिक मैट्रिक्स की आवश्यकता पर जोर देता है। वह मानव के बारे में प्रमुख दार्शनिक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी परिसर की जांच करने में विफल रहता है, जो आदर्शवादी, जैविक या यांत्रिकी से मार्क्सवादी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित करता है कि मनुष्य क्या है।
एक शिक्षक के रूप में:
एक बुद्धिजीवी के रूप में डीपी का करियर, सबसे प्रमुख रूप से, एक शिक्षक के रूप में उनका योगदान। लिखित, शब्दों के बजाय, बोलने के माध्यम से उनका दूसरों पर बहुत अधिक और अधिक प्रभाव पड़ता है। क्लास रूम, कॉफ़ी हाउस, या ड्रॉइंग रूम की आज़ादी ने उसे विचारों का पता लगाने के लिए दिया और तत्काल प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से मुद्रित पृष्ठ के माध्यम से उपलब्ध नहीं थी।
इसके अलावा, उनके लेखन की गुणवत्ता असमान थी, और न ही उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उससे लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद की जा सकती थी। इसलिए, वह एक शिक्षक बनना पसंद करते थे और अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने छात्रों के साथ संवाद और विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार, वह एक सह-छात्र, एक सह-निर्धारक था, जिसने कभी सीखना नहीं छोड़ा। उनके छात्रों पर उनका ऐसा प्रभाव था कि वे आज भी अपने छात्रों के मन में रहते हैं।
पद्धति:
डीपी मुकर्जी संभवतः भारतीय समाजशास्त्र में अग्रदूतों में सबसे लोकप्रिय थे। उन सभी की तरह, उन्होंने सामाजिक विज्ञान में ज्ञान के कम्प्यूटरीकरण के किसी भी प्रयास का विरोध किया। वह सामाजिक दार्शनिक के रूप में समाजशास्त्र में अधिक आए। हालाँकि, वह आध्यात्मिक भावनाओं को शामिल करते हुए, अनुभववाद के अधिवक्ता के रूप में अधिक समाप्त हो गया।
भारतीय परंपरा में निहित भारतीय सामाजिक यथार्थ के स्वरूप और अर्थ को समझने में उनकी गहरी रुचि थी। भारतीय परंपरा की विशिष्टता के लिए आधुनिकता की ताकतों को अपनाकर आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसे कैसे बदला जाए, इसके तरीके खोजने में उनकी समान रूप से रुचि थी। उन्हें मार्क्सवादी होने के लिए स्वीकार किया गया था।
फिर भी, उन्होंने खुद को सिद्धांतवादियों या सिद्धांतवादी मार्क्सवादी के रूप में पेश किया। यह निहित है कि उन्होंने एक राजनीतिक विचारधारा के बजाय मार्क्सवाद का विश्लेषण करने की एक विधि के रूप में अनुसरण किया। भारतीय इतिहास के उनके द्वंद्वात्मक विश्लेषण ने सुझाव दिया कि परंपरा और आधुनिकता, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और सामूहिकता को समकालीन भारत में एक दूसरे के साथ द्वंदात्मक रूप से बातचीत के रूप में देखा जा सकता है।
डीपी ने भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में योगदान दिया। वह पश्चिमी विचारों, अवधारणाओं और विश्लेषणात्मक श्रेणियों के प्रति सहनशील था। उन्होंने देखा कि एक स्वदेशी समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से पश्चिमी सामाजिक परंपराओं से भारत में इन विषयों को प्रेरित नहीं करना चाहते थे।
जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, डीपी ने खुद को 'मार्क्सवादी' के बजाय 'मार्क्सवादी' कहना पसंद किया और भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की एक द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया, जिसने उपनिवेश काल के दौरान सांस्कृतिक विरोधाभासों की कई ताकतों को उजागर किया (सिंह, 1973: 18) -20)।
उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक विशिष्टता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जो कि 'वर्ग संघर्ष' से कम और मूल्य अस्मिता और सांस्कृतिक संश्लेषण से अधिक था, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ के परिणामस्वरूप हुआ (देखें मदन, 1977: 167-68) ।
व्यापक दृष्टिकोण के अलावा, राधाकमल मुखर्जी और डीपी में बौद्धिक रूप से बहुत कम था। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में डीपी का योगदान राधाकमल मुखर्जी और डीएन मजुमदार से काफी भिन्न है जो लखनऊ में उनके समकालीन थे। डीपी सर्वेक्षणों के डेटा संग्रह के किसी भी अनुभवजन्य अभ्यास में शामिल नहीं था।
ऐसा नहीं है, वह अनुभववाद के निहित मूल्य में विश्वास नहीं करता था। यह सिर्फ इतना ही था कि स्वभाव से वह एक सामाजिक, सामाजिक दार्शनिक और संस्कृतिशास्त्री थे। उनकी अकादमिक रुचियां विविधतापूर्ण थीं: उन्होंने 'संगीत और ललित कलाओं को भारतीय संस्कृति की अजीबोगरीब रचनाओं' से लेकर 'आधुनिकता के संबंध में भारतीय परंपरा' (मुकर्जी, 1948, 1958) तक कहा। वह लखनऊ में अपने समकालीनों की तरह एक विपुल लेखक नहीं थे। फिर भी, एक बौद्धिक और एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में, उन्होंने एक शक्तिशाली विरासत को पीछे छोड़ दिया जिसने बाद के पीढ़ी के भारतीय समाजशास्त्रियों को बिना किसी छोटे उपाय के प्रभावित किया।
भारतीय समाज, संस्कृति और परिवर्तन की समझ के लिए डीपी के दृष्टिकोण के बारे में, दो बिंदुओं पर बल दिया जाना चाहिए। पहला, राधाकमल की तरह, वह एक सामाजिक विज्ञान अनुशासन और दूसरे के बीच कठोर बाधाओं को बनाए रखने के खिलाफ था, और दोनों ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को साझा किया। हालाँकि, हालांकि, घुरे की तरह, दोनों को भारतीय समाज में संरचना और परिवर्तन के अध्ययन में एक गहरी दिलचस्पी थी, उनके कार्यों में, हमें इस तरह के रूप में एक नया वैचारिक ढांचा नहीं मिला (उन्नीथन एट अल।, 1965: 15-16)।
लेखन:
डीपी एक बहुमुखी विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने उन्नीस पुस्तकें लिखीं, जिसमें विविधताएं (1958) शामिल हैं; बंगाली में दस और अंग्रेजी में नौ। उनके शुरुआती प्रकाशनों में शामिल हैं: समाजशास्त्र में बुनियादी अवधारणा (1932) और व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान (1924)। अन्य प्रकाशनों में से कुछ हैं: आधुनिक भारतीय संस्कृति (1942, 1948 में संशोधित संस्करण), भारतीय युवाओं की समस्याएं (1942), और दृश्य और साक्षात्कार (1946)।
आधुनिक भारतीय संस्कृति (1942) और विविधता (1958) को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान को उनके अन्य योगदानों जैसे टैगोर: ए स्टडी (1943), ऑन इंडियन हिस्ट्री: ए स्टडी इन मेथड (1943) और इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक (1945) से देखा जा सकता है। इनके अलावा, उन्हें उपन्यासकार, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक के रूप में भी बंगाली साहित्य में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है।
परिप्रेक्ष्य:
डीपी शैक्षणिक दुनिया में बहुत कम सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने मानव समाज में सक्रिय सामाजिक-आर्थिक बलों का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवाद के महत्व को मान्यता दी। उन्होंने मार्क्सवाद को एक सिद्धांत के रूप में माना, जिसे समाज और समूह की प्राथमिकता पर स्थापित किया गया था जो अलग और बाहरी हैं मनुष्य के लिए, एक प्रकार का पर्यावरण को सुविधाजनक बनाने के लिए और स्वायत्त व्यक्तिगत अलगाव के बलात्कारों को उजागर करने में बाधा।
किसी भी हठधर्मिता के बजाय डीपी की गहरी दिलचस्पी मार्क्सवादी पद्धति में थी। अपने दृश्य और प्रतिवेदनों (1946: 166) में शामिल 'ए वर्ड टू इंडियन मार्क्सिस्ट' नामक एक छोटे से पेपर में उन्होंने चेतावनी दी थी कि 'अन-हिस्टोरिक माइंडेड' युवा मार्क्सवादी ने 'फासीवादी' के रूप में समाप्त होने का जोखिम उठाया था, और मार्क्सवाद स्वयं 'नारों के चक्रव्यूह में अपनी प्रभावशीलता खो सकता है।'
फिर भी, यह कहना भ्रामक नहीं होगा कि डीपी ने वास्तव में विभिन्न तरीकों से मार्क्सवाद को गले नहीं लगाया, संस्कृति के निर्माण में आर्थिक कारक पर एक साधारण जोर से लेकर सिद्धांत के परीक्षण की स्थिति तक। यह एक करीबी लेकिन असुविधाजनक आलिंगन था।
व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान (1924) और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन सोशियोलॉजी (1932) में अपनी बुनियादी दो पुस्तकों में, डीपी ने सामाजिक विज्ञान की पर्याप्त अवधारणा तैयार करने के लिए अपने प्रयास के 'व्यक्तिगत दस्तावेजों' उत्पादों पर विचार किया। शुरुआत से ही, उन्होंने व्यक्तित्व की धारणा के आसपास अपने विचारों को व्यवस्थित किया।
उन्होंने यह स्थिति संभाली कि अमूर्त व्यक्ति को सामाजिक विज्ञान सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक समग्र, मनोवैज्ञानिक-समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की याचना की। यह व्यक्तित्व की दोहरी प्रक्रिया और व्यक्तिगत जीवन की विशिष्टता के समाजीकरण का यह संश्लेषण था कि एक व्यक्तित्व को समझा जा सकता है (मुकर्जी, 1924)।
अपने जीवनकाल के काम को देखते हुए, डीपी ने 1955 में पहले भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वह अर्थशास्त्र और इतिहास से समाजशास्त्र में आए थे क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व को ज्ञान (1958: 228) के माध्यम से विकसित करने में रुचि रखते थे।
एक व्यापक सामाजिक विज्ञान का कार्यालय, सामाजिक विज्ञानों के प्रचलित कम्पार्टमेंटलाइज़ेशन को पार करते हुए, उनके द्वारा एक एकीकृत हालांकि कई मुखर व्यक्तित्व के विकास की कल्पना की गई थी। यह एक विचार है, जैसा कि एके सरन (1962: 167) ने बताया है, मूर द्वारा उनकी प्रिंसिपिया एथिका में सुझाए गए आदर्श के समानांतर कुछ मायनों में।
डीपी ने कहा कि ज्ञान और ज्ञाता को एक साथ देखा जाना चाहिए। अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर ज्ञान को दार्शनिक होना चाहिए। इसमें पारलौकिक अनुशासनात्मक सीमाएँ हैं। पश्चिमी उदारवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय बुद्धिजीवियों ने विश्वदृष्टि उधार ली थी। Is उद्देश्य ’के तत्व पर जोर दिया गया है क्योंकि of प्रगति’ स्वचालित स्व-उत्पन्न विकास में एक चरण नहीं है। प्रगति स्वतंत्रता का आंदोलन है। डीपी प्रगति के लिए मूल्यों का संतुलन शामिल है और वह धार्मिक शास्त्रों से मूल्यों के पदानुक्रम की पहचान करने के लिए आकर्षित करता है।
यहाँ, हम निम्नलिखित में DP के योगदान पर प्रकाश डालना चाहेंगे:
1. व्यक्तित्व
2. आधुनिक भारतीय संस्कृति
3. परंपरा
4. समाजशास्त्र की प्रकृति और विधि
5. नए मध्य वर्गों की भूमिका
6. भारतीय इतिहास का निर्माण
7. आधुनिकीकरण
8. संगीत
1. व्यक्तित्व:
डीपी ने एक बार मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने 'शुद्ध' की थीसिस को प्रतिपादित किया। 'पुरुष' समाज और व्यक्ति से अलग-थलग नहीं है। न ही वह समूह मन की पकड़ में है। परुष एक सक्रिय एजेंट के रूप में दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है और जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उनका तर्क है कि दूसरों के साथ उनके संबंधों के परिणामस्वरूप 'शुद्ध' बढ़ता है और इस प्रकार, मानव समूहों के बीच एक बेहतर स्थान रखता है।
डीपी स्वीकार करता है कि भारतीय सामाजिक जीवन मधुमक्खियों और बीवरों के जीवन की तरह है और भारतीय लगभग एक प्रतिगामी लोग हैं। लेकिन "इसकी सुंदरता" यह है कि हम में से अधिकांश को प्रतिगामी महसूस नहीं होता है। डीपी को संदेह है कि क्या बाजार प्रणाली में वर्चस्व रखने वाले पश्चिमी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता है।
वह विज्ञापनों, प्रेस-चेन, चेन स्टोर्स में हेरफेर के संपर्क में है और उसका पर्स लगातार खाली किया जाता है। यह सब व्यक्ति की पसंद और उपभोक्ता की संप्रभुता के अधिकार के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं छोड़ता है। इसके विपरीत, एक औसत भारतीय की आकांक्षा का निम्न स्तर, जिसे समूह मानदंडों द्वारा संचालित किया जाता है, जीवन में अधिक से अधिक वृद्धि करता है।
यह हमारी इच्छा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्री को इस समूह को अपनी इकाई के रूप में स्वीकार करना होगा और व्यक्ति को बाहर करना होगा। उसके लिए भारत की परंपरा है। भारतीय समाजशास्त्रियों को इस परंपरा की विशिष्ट प्रकृति को समझना होगा।
2. आधुनिक भारतीय संस्कृति:
समय बीतने के साथ उनके कामों पर जोर दिया गया है। डीपी बहुत संवेदनशील था और अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित था। उन्होंने पारंपरिक संस्कृति के साथ-साथ आधुनिकता से भी रूबरू कराया। आधुनिक भारतीय संस्कृति: 1942 में पहली बार एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रकाशित हुआ था और 1947 में इसका संशोधित संस्करण था - विभाजित स्वतंत्रता का वर्ष। संश्लेषण भारतीय संस्कृति का प्रमुख आयोजन सिद्धांत रहा है। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को एक वास्तविक मोड़ प्रदान किया।
मध्य वर्ग ने भारत में ब्रिटिश शासन के एकीकरण में मदद की, लेकिन बाद में इसे सफलतापूर्वक चुनौती दी। भारत की डीपी की दृष्टि विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों के विविध तत्वों के 'संघ' से पैदा हुआ एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील भारत था। परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुनर्संरचना एक अनिवार्य शर्त थी। डीपी ने इनकार किया कि वह मार्क्सवादी था; उन्होंने केवल एक 'मार्क्सवादी' होने का दावा किया।
राष्ट्रीय आंदोलन बौद्धिक विरोधी था, हालांकि इसने आदर्शवाद और नैतिक उत्थान पैदा किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला: "राजनीति ने हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया है।" डीपी का मानना था कि नकल के माध्यम से कोई वास्तविक आधुनिकीकरण संभव नहीं है। उन्हें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की आशंका थी। आधुनिकीकरण पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक पैटर्न के विस्तार, उन्नयन, पुनरोद्धार की एक प्रक्रिया है। परंपरा निरंतरता का एक सिद्धांत है। यह हमें विभिन्न विकल्पों में से चुनने की स्वतंत्रता देता है। आधुनिकता के संबंध में परिभाषित किया जाना चाहिए, और परंपरा के खंडन में नहीं।
डीपी के तर्कों की आलोचना की गई। सरन ने बताया है कि डीपी समाजवादी आदेश का विश्लेषण करने के लिए खुद ही नहीं आता है और अपने सौम्य चरित्र को भरोसे में लेता है। वह यह महसूस करने में विफल है कि एक प्रौद्योगिकी-उन्मुख समाज आसानी से गैर-शोषक नहीं हो सकता है और न ही विरोधी; और पारंपरिक और आधुनिक विश्व साक्षात्कार समय की विभिन्न धारणाओं में निहित हैं। डीपी की चिंता को पश्चिमी हिंदू बौद्धिकता के रूप में देखा जाता है। डीपी को पढ़ने, उनके कार्यों को पुनर्मुद्रित करने और उनके विचारों की जांच करने की आवश्यकता है (मदन, 1993)।
3. परंपरा:
परंपरा से क्या अभिप्राय है? डीपी बताते हैं कि यह परंपरा 'परंपरा' से आई है, जिसका अर्थ है "प्रसारित करना"। परंपरा के समतुल्य संस्कृत या तो परम्परा है, जो उत्तराधिकार या अनित्य है, जिसकी जड़ इतिहस, या इतिहास है।
परंपराओं का एक स्रोत माना जाता है। यह शास्त्र, या चरणों के कथन (apta vakya), या पौराणिक नायकों के नाम के साथ या बिना हो सकते हैं। जो भी स्रोत हो सकता है, परंपराओं की ऐतिहासिकता को ज्यादातर लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्हें उद्धृत किया जाता है, वापस बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। वास्तव में, उनकी आयु लंबी उत्तराधिकार सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक एकजुटता सुनिश्चित करती है।
परंपरा की गतिशीलता:
इस प्रकार, परंपरा संरक्षण का कार्य करती है। लेकिन यह जरूरी रूढ़िवादी नहीं है। डीपी ने कहा कि परंपराएं बदलती हैं। भारतीय परंपरा में परिवर्तन के तीन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है: श्रुति, स्मृति, अनुभाव। यह शुभ या व्यक्तिगत अनुभव है, जो क्रांतिकारी सिद्धांत है। कुछ उपनिषद पूरी तरह से इस पर आधारित हैं।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विभिन्न संप्रदायों या पंथों के संत-संस्थापकों का व्यक्तिगत अनुभव जल्द ही प्रचलित सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन का सामूहिक अनुभव बन गया है। इन संतों और उनके अनुयायियों के प्रेम या सहजता या सहजता का अनुभव मुसलमानों के बीच सूफियों में भी ध्यान देने योग्य है।
पारंपरिक प्रणाली ने धीरे-धीरे असंतुलित आवाज़ों को समायोजित किया। भारतीय सामाजिक कार्रवाई ने संविधान की सीमाओं के भीतर विद्रोही संरेखित करने के लिए अक्षांश दिया है। इसका परिणाम वंचितों की वर्ग-चेतना को कुंद करने वाला जाति समाज रहा है।
परंपरा और आधुनिकता की बोली:
भारतीय परंपरा की ताकत पुरुषों और महिलाओं के जीवन की आदतों और भावनाओं में पिछले घटनाओं से उभरने वाले मूल्यों के क्रिस्टलीकरण में निहित है। इस तरह, भारत ने निश्चित रूप से कई मूल्यों का संरक्षण किया है: कुछ अच्छे और दूसरे बुरे। हालाँकि, यह बात उन ताकतों का उपयोग करने के लिए है, जो भारतीय परंपराओं, जैसे, प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र, शहरीकरण, नौकरशाही, आदि के लिए विदेशी हैं।
डीपी आश्वस्त है कि समायोजन निश्चित रूप से होगा। यह लगभग गारंटी है कि भारतीय गायब नहीं होंगे, जैसा कि आदिम जनजातियों ने पश्चिमी संस्कृति के स्पर्श में किया है। उनके पास इसके लिए पर्याप्त लचीलापन है। भारतीय संस्कृति ने आदिवासी संस्कृति और इसके कई अंतर्जात विघटन को आत्मसात कर लिया था। इसने हिंदू-मुस्लिम संस्कृतियों को विकसित किया था और आधुनिक भारतीय संस्कृति एक जिज्ञासु सम्मिश्रण है, वर्णसंकर। "परंपरागत रूप से, इसलिए, समायोजन में रहना भारत के रक्त में है, इसलिए बोलने के लिए"।
डीपी परंपरा की पूजा नहीं करता। "पूर्ण पुरुष" या "अच्छी तरह से संतुलित व्यक्तित्व" का उनका विचार (1) नैतिक उत्साह और सौंदर्य और बौद्धिक संवेदनशीलता के साथ (2) इतिहास और तर्कसंगतता की भावना का मिश्रण है। दूसरी श्रेणी के गुणों पर भारतीय परंपरा की तुलना में आधुनिकता से अधिक जोर दिया गया है। इसलिए, परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्ववाद परंपरा को समझने की आवश्यकता में निहित है। डीपी का मानना है कि "परंपराओं का ज्ञान उन्हें कम से कम सामाजिक लागत के साथ तोड़ने का रास्ता दिखाता है"।
'परंपरा और आधुनिकता' पर डीपी के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण लेखन इन दो द्विध्रुवी अवधारणाओं की प्रामाणिक माप को समझने में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की परंपरा और आधुनिकता, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद और व्यक्तिवाद और सामूहिकता, यानी संघ के बीच द्वंद्वात्मक संबंध हैं।
उनकी बोलियों की अवधारणा उदार मानवतावाद में लंगर डाले हुए थी। उन्होंने अपने सभी कार्यों के माध्यम से तर्क दिया कि परंपराएं भारतीय समाज की समझ के लिए केंद्रीय हैं। ब्रिटिश काल और परंपराओं के दौरान भारत में आए आधुनिकीकरण के संबंध द्वंद्वात्मक हैं। यह द्वंद्वात्मकता के इस दृष्टिकोण से है, डीपी ने तर्क दिया, हम परंपराओं को परिभाषित करेंगे।
आधुनिकीकरण के साथ परंपरा की मुठभेड़ ने कुछ सांस्कृतिक विरोधाभासों, अनुकूलन और कुछ मामलों में संघर्ष की स्थितियों को भी पैदा किया। परंपरा-आधुनिकता मुठभेड़ के परिणामों के बारे में बताते हुए, योगेंद्र सिंह (1986) लिखते हैं:
डीपी मुकर्जी के लेखन में हमें भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ के द्वंद्वात्मक फ्रेम से विश्लेषण के साथ कुछ व्यवस्थित चिंता का पता चलता है। वह मुख्य रूप से पश्चिम के साथ परंपरा की मुठभेड़ पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक तरफ, सांस्कृतिक विरोधाभासों के कई कारकों को उकसाता है और दूसरी तरफ, एक नए मध्य वर्ग को जन्म देता है। उनके अनुसार, इन शक्तियों का उदय, संघर्ष और संश्लेषण की एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करता है, जिसे भारतीय समाज के वर्गीय ढांचे की संरक्षित ऊर्जाओं को निभाने में एक धक्का दिया जाना चाहिए।
परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़, इसलिए दो परिणामों में समाप्त होती है: (1) संघर्ष, और (2) संश्लेषण। भारतीय समाज, डीपी की परिकल्पना के रूप में, परंपरा और आधुनिकता के बीच बातचीत का परिणाम है। यह यह द्वंद्वात्मकता है, जो हमें भारतीय समाज का विश्लेषण करने में मदद करती है।
डीपी की परंपरा की अवधारणा वर्ष 1942 में पहली बार दिखाई दी जब उनकी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी प्रकाशित हुई। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में परंपरा का उनका चरित्र वर्णन नीचे दिया गया है:
एक सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में…। भारतीय संस्कृति कुछ सामान्य परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने कई सामान्य दृष्टिकोणों को जन्म दिया है। उनके आकार देने में प्रमुख प्रभाव बौद्ध, इस्लाम और पश्चिमी वाणिज्य और संस्कृति रहे हैं। यह इस तरह की बदलती ताकतों के आत्मसात और संघर्ष के माध्यम से था कि भारतीय संस्कृति वह बन गई है जो आज न तो हिंदू है और न ही इस्लामिक, न तो जीवन और विचार की पश्चिमी पद्धति की प्रतिकृति है और न ही शुद्ध रूप से एशियाई उत्पाद (1948: 1)।
पुस्तक की केंद्रीय थीसिस यह थी कि भारत के इतिहास की कुंजी सांस्कृतिक संश्लेषण थी - आंतरिक और बाहरी राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया - और यह कि भारत का इतिहास हेगल और मार्क्स के विचारों के बावजूद अतीत से अधिक था विषय। डीपी ने ब्रिटिश शासन के विघटन को स्थायी चोट नहीं माना: यह केवल एक रुकावट थी।
उन्होंने माना कि संज्ञानात्मक श्रेणियों के स्तर पर हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक संश्लेषण सबसे कमजोर था, लेकिन साझा आर्थिक हितों, और संगीत, वास्तुकला और साहित्य में उपलब्धियों की सराहना की। डीपी ने उप-महाद्वीप के विभाजन को अपने भू-राजनीति में एक घटना से अधिक नहीं माना। भविष्य, वह लगभग आश्वस्त था, वर्तमान को एक सच्चे द्वंद्वात्मक आंदोलन में बदल देगा। हम संस्कृति का राजनीतिकरण न करें, वह कहते थे।
टैगोर अध्ययन डीपी की थीसिस को जड़ों के महत्व के बारे में बताता है। बंकिमचंद्र चटर्जी के साथ टैगोर की तुलना करते हुए, वह लिखते हैं: “भारतीय परंपराओं के साथ उनका [टैगोर का] संतृप्ति गहरा था; इसलिए वह अधिक आसानी से पश्चिमी विचारों की एक बड़ी खुराक को आत्मसात कर सकता था। "और फिर:" टैगोर पर पश्चिम का प्रभाव बहुत अच्छा था ... लेकिन यह अतिरंजित नहीं होना चाहिए ...। उनके गद्य, कविता, नाटक, संगीत और उनके व्यक्तित्व के विकास में प्रत्येक स्तर पर हम टैगोर को मिट्टी के कुछ बुनियादी भण्डार पर, लोगों की, आत्मा की, और बड़े निवेश की क्षमता के साथ उभरते हुए पाते हैं ”(मुकर्जी), 1972: 50)।
परंपराओं की संरचना:
भारतीय परंपरा कुछ ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। वे वास्तव में भारतीय संस्कृति की संरचना का निर्माण करते हैं। ये परंपराएँ कई विचारधाराओं से संबंधित हैं जैसे कि बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, आदिवासी जीवन और पश्चिमी आधुनिकता। इसलिए, संश्लेषण की प्रक्रिया ने इन परंपराओं का निर्माण किया है। इस संबंध में, यह मानना गलत होगा कि परंपराएं केवल हिंदू हैं। वास्तव में, वे देश के विभिन्न जातीय समूहों की परंपराओं को जोड़ते हैं।
विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के सिद्धांतों को भारतीय परंपराओं के अनुसार टीएन मदान ने कैसे समझा है:
इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में, संश्लेषण हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम का प्रमुख आयोजन सिद्धांत रहा है, जिन्होंने मिलकर एक विश्वदृष्टि को आकार दिया था, जिसमें डीपी के अनुसार, 'होने का तथ्य स्थायी महत्व था'। उपनिषदों से उनका पसंदीदा उद्धरण चरैवेति था, आगे बढ़ते रहे। इसका मतलब यह था कि क्षणिक और संवेदना के प्रति उदासीनता और 'सर्वोच्च वास्तविकता' में अंततः इसके विघटन के लिए थोड़ा स्वयं के अधीनता के साथ एक पूर्वाग्रह था (1948: 2)।
डीपी ने तीन सिर, अर्थात, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के तहत भारतीय परंपराओं का वर्गीकरण प्रदान करने का प्रयास किया। भारतीय समाज में प्राथमिक परंपराएँ प्रधान और प्रामाणिक रही हैं। द्वितीयक परंपराओं को दूसरी रैंकिंग दी गई, जब देश में मुसलमान पहुंचे। और, ब्रिटिश आगमन के समय तक, हिंदुओं और मुसलमानों ने अभी तक अस्तित्व के सभी स्तरों पर परंपराओं का एक पूर्ण संश्लेषण हासिल नहीं किया था।
प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और विनियोजन और सौंदर्य और धार्मिक परंपराओं के संबंध में कुछ हद तक उनके बीच समझौते का एक बड़ा उपाय था। वैचारिक विचारों की तृतीयक परंपराओं में, हालांकि, मतभेद प्रमुख रूप से जीवित रहे।
परंपराओं के स्रोत:
भारतीय समाजशास्त्रियों ने परंपराओं के बारे में पर्याप्त बात की है, लेकिन परंपराओं के स्रोतों और सामग्री की पहचान करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। और यह बहुत अच्छी तरह से हो जाता है जब हम डीपी मुकर्जी के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि भारत की परंपराओं और आधुनिकीकरण के किसी भी विश्लेषण में परंपराओं का केंद्रीय स्थान है।
लेकिन डीपी ने इन परंपराओं की सामग्री नहीं दी है। परंपराओं के प्रमुख स्रोत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और पश्चिमी संस्कृति हैं, लेकिन उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म या इस्लाम की जो परंपराएं हैं, वे व्यापक भारतीय परंपराओं को डीपी द्वारा विशिष्ट नहीं बनाया गया है।
इस संबंध में उनकी कमजोरी की पहचान टीएन मदान ने की है जो कहते हैं कि डीपी के अनुसार भारतीय परंपराओं का सामान्य निर्माण वेदांत, पश्चिमी मुक्ति और मार्क्सवाद का संश्लेषण हो सकता है। लेकिन, इस्लाम और बौद्ध धर्म के संश्लेषण के बारे में क्या? डीपी अन्य प्रमुख परंपराओं के किसी भी ऐसे संश्लेषण को प्रदान करने में विफल रहता है।
मदन (1993) डीपी की इस विफलता पर टिप्पणी इस प्रकार है:
एक समान रूप से महत्वपूर्ण और कठिन उपक्रम परंपरा की सामग्री के अपने गर्भाधान का विस्तार और विशिष्टता होगा। जबकि वह स्थापित करता है, मुझे विश्वास है कि सिद्धांत के स्तर पर आधुनिकता के लिए परंपरा की प्रासंगिकता, वह सामान्य श्रेणियों के अलावा अपनी अनुभवजन्य सामग्री को नहीं छोड़ता है। एक को यह महसूस करने में असहजता होती है कि उसने खुद को ग्रंथों के गहन अध्ययन की तुलना में संस्था और सामान्य ज्ञान के संदर्भ में अधिक संचालित किया है। मानवविज्ञानी के रूप में क्षेत्र के काम के माध्यम से परंपरा के साथ टकराव, निश्चित रूप से, उसके द्वारा शासित था, कम से कम खुद के लिए।
4. समाजशास्त्र की प्रकृति और विधि:
डीपी एक अर्थशास्त्री को प्रशिक्षित करके था। हालाँकि, वह अन्य अर्थशास्त्रियों की प्रथाओं की सीमाओं से अवगत था। वे पश्चिमी मॉडल के बाद परिष्कृत तकनीकों और अमूर्त सामान्यीकरण में महारत हासिल करने और लागू करने में रुचि रखते थे। वे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में भारत में आर्थिक विकास को देखने में विफल रहे। उन्होंने इस चिंता के साथ ध्यान दिया कि हमारे प्रगतिशील समूह बुद्धि के क्षेत्र में और आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में भी विफल रहे हैं, "मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक वास्तविकता में उनकी अज्ञानता और अज्ञानता के कारण"।
सामाजिक वास्तविकता के कई और अलग-अलग पहलू हैं और इसकी परंपरा और भविष्य है। इस सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए, व्यक्ति को (i) अपने विभिन्न पहलुओं के अंतःक्रियाओं की प्रकृति और (ii) अपनी परंपरा और एक बदले हुए भविष्य की ओर अग्रसर करने वाली शक्तियों का एक व्यापक और समकालिक दृष्टिकोण होना चाहिए।
विशेष विषयों में संकीर्ण विशेषज्ञता इस समझ में मदद नहीं कर सकती। समाजशास्त्र यहां बड़ी मदद कर सकता है। "समाजशास्त्र में किसी भी अन्य अनुशासन की तरह एक मंजिल और छत होती है।" हालांकि, समाजशास्त्र की विशेषता "इसके तल में सभी प्रकार के सामाजिक विषयों की आधारभूत मंजिल होती है और इसकी छत आकाश की ओर खुली रहती है"।
सामाजिक आधार की उपेक्षा से हाल के अर्थशास्त्र की तरह अमूर्तता पैदा होती है। दूसरी ओर, नृविज्ञान और मनोविज्ञान में अनुभवजन्य अनुसंधान के बहुत से इसके संकीर्ण दायरे के कारण बेकार हो गया है। समाजशास्त्र हमें जीवन और सामाजिक वास्तविकता का अभिन्न दृष्टिकोण रखने में मदद करता है।
यह विवरण में दिखेगा लेकिन यह पेड़ों के पीछे की लकड़ी की खोज भी करेगा। डीपी ने अपने शिक्षकों से सीखा और सामाजिक जीवन के विशाल कैनवस के एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विचार किया। इसलिए, उन्होंने सामाजिक विज्ञानों के संश्लेषण पर लगातार चोट की। समाजशास्त्र इस प्रयास को संश्लेषित करने में मदद कर सकता है।
समाजशास्त्र का पहला काम बलों की विशिष्ट प्रकृति को समझना है जो समय के साथ एक विशेष समाज को बनाए रखते हैं। इस कारण से, डीपी ने जोर दिया कि भारत के समाजशास्त्रियों को परंपरा की प्रकृति को समझना चाहिए, जिसने सदियों से भारतीय समाज को संरक्षित किया है। लेकिन समाजशास्त्र यथास्थिति का बचाव नहीं है। डीपी का दावा है कि "समाजशास्त्र को अंततः परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करके सामाजिक प्रणाली से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए"।
भारतीय समाज के डीपी के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में यह दिखाने का गुण है कि भारतीय समाज बदल रहा है, लेकिन बहुत अधिक विघटन के बिना। इसलिए, उन्हें पता था कि भारतीय सामाजिक प्रणाली के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि इसकी परंपरा, इसके विशेष प्रतीक और संस्कृति और प्रतीकों में आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के इसके विशेष पैटर्न हैं। डीपी अवलोकन करता है: "मेरे विचार में, परिवर्तन प्रति से अधिक वास्तविक और वस्तुपरक है।"
डीपी ने घोषणा की कि “भारतीय समाजशास्त्री के लिए समाजशास्त्री होना पर्याप्त नहीं है। उसे एक भारतीय होना चाहिए, अर्थात्, उसे इस सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए लोकगीतों, कथाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं को साझा करना है और इसके नीचे और इसके बाहर क्या निहित है ”।
भारतीय समाजशास्त्री दो दृष्टिकोणों के संश्लेषण की कोशिश करेंगे: वह एक तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। वास्तव में तुलनात्मक दृष्टिकोण भारतीय समाज द्वारा अन्य समाजों के साथ साझा की गई विशेषताओं और इसकी परंपरा की विशिष्टता को उजागर करेगा। इस कारण से, समाजशास्त्री परंपरा के अर्थ को समझने के उद्देश्य से होगा। वह इसके प्रतीकों और मूल्यों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। साथ ही, वह संरक्षण और परिवर्तन के विरोधी बलों के संघर्ष और संश्लेषण को समझने के लिए एक द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण भी अपनाएगा।
मार्क्सवाद और भारतीय स्थिति:
डीपी को मार्क्सवाद पर बहुत भरोसा था। मार्क्सवाद मानव समाज के विकास में एक वांछनीय उच्च स्तर का विचार देता है। उस उच्च अवस्था में, व्यक्तित्व समाज में दूसरों के साथ एक नियोजित, सामाजिक रूप से निर्देशित, ऐतिहासिक रूप से समझे जाने वाले सामूहिक प्रयास के लिए एकीकृत हो जाता है, जिसका अर्थ है समाजवादी व्यवस्था। लेकिन, उन्होंने मार्क्सवादियों द्वारा भारतीय सामाजिक घटना के विश्लेषण की प्रभावकारिता पर संदेह व्यक्त किया।
उन्होंने इसके तीन कारण बताए:
(१) मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष के संदर्भ में हर चीज का विश्लेषण करेंगे। लेकिन, हमारे समाज में, वर्ग संघर्ष लंबे समय से जाति परंपराओं से ढका है और नए वर्ग संबंध अभी तक तेजी से नहीं उभरे हैं।
(२) उनमें से कई भारत के सामाजिक-आर्थिक इतिहास से अनभिज्ञ हैं।
(३) जिस तरह से आर्थिक दबाव काम करते हैं, वह यांत्रिक बल किसी मृत पदार्थ को ले जाने में नहीं है।
परंपराओं में प्रतिरोध की महान शक्तियां होती हैं। उत्पादन के तौर-तरीकों में बदलाव से यह प्रतिरोध दूर हो सकता है। केवल हिंसक क्रांतियों द्वारा इस प्रकृति का गति परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन, अगर कोई समाज सहमति से और बिना खून-खराबे के क्रांति का विरोध करता है, तो उसे आर्थिक बदलाव और परंपरा की बोली पर धैर्य से काम लेना चाहिए।
डीपी का जोर है कि भारतीय परंपराओं का अध्ययन करना भारतीय समाजशास्त्रियों का पहला और तत्काल कर्तव्य है। और, यह आर्थिक ताकतों के संदर्भ में भारतीय परंपराओं में बदलाव की समाजवादी व्याख्याओं से पहले होना चाहिए।
पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के प्रत्यक्षवाद की अस्वीकृति:
डीपी पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के प्रत्यक्षवाद के खिलाफ था। इसके लिए व्यक्तियों को जैविक या मनोवैज्ञानिक इकाइयों में कम कर दिया। पश्चिम की औद्योगिक संस्कृति ने व्यक्तियों को स्वयं-चाहने वाले एजेंटों में बदल दिया था। पश्चिम में समाज जातीय हो गया था। व्यक्तीकरण पर जोर देने से, अर्थात, व्यक्ति की भूमिकाओं और अधिकारों की मान्यता, प्रत्यक्षवाद ने मनुष्य को उसके सामाजिक संकटों से उखाड़ फेंका। डीपी देखता है, "मनुष्य की हमारी धारणा शुद्ध है और व्यक्ति या शक्ति नहीं है"।
हमारे धार्मिक ग्रंथों में या संतों के कहने पर व्यक्ती शब्द बहुत कम आता है। पुरुष या व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के साथ जीवन के मूल्यों और हितों को साझा करने के माध्यम से, अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ सहयोग के माध्यम से विकसित होता है। भारत की सामाजिक प्रणाली मूल रूप से समूह, संप्रदाय या जाति की कार्रवाई का एक आदर्श अभिविन्यास है, लेकिन स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्रवाई की नहीं। नतीजतन, एक आम भारतीय को हताशा के डर का अनुभव नहीं होता है। डीपी इस मामले में हिंदू और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध के बीच कोई अंतर नहीं करता है।
5. नए मध्य वर्गों की भूमिका:
The urban-industrial order, introduced by the British in India, set aside the older institutional networks. It also discovered many traditional castes and classes. It called for a new kind of social adaptation and adjustment. In the new set-up the educated middle classes of the urban centres of India became the focal point of the society.
They came to command the knowledge of the modern social forces, that is, science, technology, democracy and a sense of historical development, which the west would stand for. The new society of India calls for the utilization of these qualities and the services of the middle classes have been soaked with the western ideas and lifestyles.
And they remained blissfully, and often contemptuously, ignorant of Indian culture and realities. They are oblivious to the Indian traditions. But traditions have “great powers of resistance and absorption”. Even “on the surface of human geography and demographic pattern, traditions have a role to play in the transfiguration of physical adjustments and biological urges”.
In India, for example, things like city planning and family planning are so tied up with traditions that the architect and the social reformer can ignore them only at the peril of their schemes. India's middle classes, thus, would not be in a position to lead the masses to build India along modern lines. They were uprooted from their indigenous traditions. They have lost contact with the masses.
India can move on to the road of modernity only by adapting it to her traditions if the middle classes re-establish their link with the masses. They should not be either apologetic for or unnecessarily boastful of their traditions. They should try to harness its vitality for accommodating changes required by modernity. A balance between individuation and association will be achieved thereby. India and the world will be enriched with the new experience.
6. Making of Indian History:
At this point it seems just pertinent enough to point out that, while DP followed Marx closely in his conception of history and in his characterization of British rule as uprooting, he differed significantly not only with Marx's assessment of the positive consequences of British rule, but also with his negative assessment of pre-British traditions.
It is important to note this because some Marxists have claimed on their side, despite his denials that he was a Marxist; he jestingly claimed to be only a 'Marxologist' (Singh, 1973: 216). Some non-Marxists also have, it may be added, described him as Marxist.
It will be recalled that Marx had in his articles on British rule in India asserted that India had a strong past but “no history at all, at least no known history”; that its social condition had “remained unaltered since its remotest antiquity”; that it was 'British steam and science' which “uprooted, over the whole surface of Hindustan, the union between agriculture and manufacturing industry”.
Marx had listed England's 'crimes' in India and proceeded to point out that she had become 'the unconscious tool of history' whose action would ultimately result in a 'fundamental revolution' (see Marx, 1853). He had said: “England had to fulfill a double mission in India: one destructive and the other regenerating – the annihilation of old Asiatic society, and the laying of the material foundations of western society in India (1959: 31).
Thus, for Marx, as for so many others since his time, including intellectuals of various shades of opinion, the modernization of India has to be its westernization.
As has already been stated above, DP was intellectually and emotionally opposed to this view about India's past and future whether it came from Marx or from liberal bourgeois historians. He refused to be ashamed or apologetic about India's past.
The statement of his position was unambiguous:
Our attitude is one of humility towards the given fund. But it is also an awareness of the need, the utter need, of recreating the given and making it flow. The given of India is very much in ourselves. And we want to make something worthwhile out of it (1945: 11). Indian history could not be made by outsiders; it has to be enacted by the Indians themselves. In this endeavour, they not only had to be firm of purpose but also clear headed.
उसने लिखा:
Our sole interest is to write and enact Indian history. Action makes making; it has a starting point – this specificity called India; or if that be too vague, this specificity of contact between India and England or the West. Making involves changing, which in turn requires (a) a scientific study of the tendencies which make up this specificity, and (b) a deep understanding of the crisis (which marks the beginning no less than the end of an epoch). In all these matters, the Marxian method … is likely to be more useful than other methods. If it is not, it can be discarded. After all, the object survives (1945: 46).
'Specificity' and 'crisis' are the key words in this passage: the former points to the importance of the encounter of traditions and the latter to its consequences. When one speaks of tradition, or of 'Marxist's specification', he/she means in DP's words, “the comparative obduracy of die culture pattern”. He expected the Marxist approach to be grounded in the specificity of Indian history (1945: 45; 1946: 162ff), as indeed Marx himself had done by focusing on Indian capitalism, the dominant institutions of western society in his times.
Marx, it will be said, was interested in precipitating the crisis of contradictory class interest in capitalist society (1945: 37). DP, too, was interested in the study of tradition and modernity in India. This could be done by focusing first on tradition and then only on change.
The first task for us, therefore, is to study the social traditions to which we have been born. This task includes the study of the changes in the traditions by external and internal pressures. The latter are most economic…. Unless the economic force is extraordinarily strong – and it is only when the modes of production are altered – traditions survive by adjustments.
The capacity for adjustment is the measure of the vitality of traditions. One can have full vitality of this treasure only by immediate experience. Thus, this is that I give top priority to the understanding (in Dilthey's sense) of traditions even for the study of their changes. In other words, the study of Indian traditions … should proceed the socialist interpretations of changes in Indian traditions in terms of economic forces (1958: 232).
He hovered between Indian traditions and Marxism and his adherence to Marxist solutions to intellectual and practical problems gained salience in his later work, which was also characterized by heightened concern with tradition.
7. Modernization: Genuine or Spurious?
For DP the history of India was not the history of her particular form of class struggle because she had experienced none worth the name. The place of philosophy and religion was dominant in his history, and it was fundamentally a long-drawn exercise in cultural synthesis. For him, “Indian history was Indian culture” (1958: 123). India's recent woes, namely, hatred and partition, had been the result of arrested assimilation of Islamic values (ibid.: 163); he believed that history halts until it is pushed (ibid.: 39).
The national movement had generated much moral fervour but DP complained, it had been anti-intellectual. Not only had there been much unthinking borrowing from the west, there had also emerged a hiatus between theory and practice as a result of which thought had become impoverished and action ineffectual. Given his concern for intellectual and artistic creativity, it is not surprising that he should have concluded: “politics ruined our culture” (1958: 190).
What was worse, there were no signs of this schism being healed in the years immediately after independence. When planning arrived as state policy in the early 1950s, DP expressed his concern, for instance, in an important 1953 paper on 'Man and Plan in India' (1958: 30-76), that a clear concept of the new man to formulate a negative judgment about the endeavours to build a new India, and also diagnosed the cause of the rampant intellectual sloth. He said in 1955: “I have seen how our progressive groups have failed in the field of intellect, and hence also in economic and political action, chiefly on account of their ignorance of and unrootedness in India's social reality” (1958: 240).
The issue at stake was India's modernization. DP's essential stand on this was that there could not be genuine modernization through imitation. A people could not abandon their own cultural heritage and yet succeeded in internalizing the historical experience of other peoples; they could only be ready to be taken over. He feared cultural imperialisms more than any other.
The only valid approach, according to him, was that which characterized the efforts of men like Ram Mohan Roy and Rabindranath Tagore, who tried to make “the main currents of western thought and action … run through the Indian bed to remove its choking weeds in order that the ancient stream might flow” (1958: 33).
DP formulated this view of the dialectics between tradition and modernity several years before independence, in his study of Tagore published in 1943, DP views the nature and dynamics of modernization. It emerges as a historical process which is at once an expansion, an elevation, a deepening and revitalization – in short, a larger investment – of traditional values and cultural patterns, and not a total departure from them, resulting from the interplay of the traditional and the modern.
From this perspective, tradition is a condition of rather than obstacle to modernization; it gives us the freedom to choose between alternatives and evolve a cultural pattern which cannot but be a synthesis of the old and the new. New values and institutions must have a soil in which to take root and from which to imbibe character. Modernity must, therefore, be defined in relation to and not in denial of tradition. Conflict is only the intermediate stage in the dialectical triad: the movement is toward coincidentia oppositorum.
Needless to emphasize, the foregoing argument is in accordance with the Marxist dialectic which sees relations as determined by one another and therefore bases a 'proper' understanding of them on such a relationship. Synthesis of the opposites is not, however, a historical inevitability; it is not a gift given to a people consciousness (1958: 189); it is a “dynamic social process and not another name for traditionalism” (ibid.: 100-2).
History for DP was a going concern (1945: 19), and the value of the Marxist approach to the fully awakened endeavour. The alternative to self-conscious choice-making is mindless imitation and loss of autonomy and, therefore, dehumanization, though he did not put it quite in these words.
Self-consciousness, then, is the form of modernization. Its content, one gathers from DP's writings in the 1950s, consists of nationalism, democracy, the utilization of science and technology for harnessing nature, planning for social and economic development, and the cultivation of rationality. The typical modern man is the engineer, social and technical (1958: 39-40).
DP believed that these forces were becoming ascendant:
This is a bare historical fact. To transmute that fact into a value, the first requisite is to have active faith in the historicity of the fact…. The second requisite is social action … to push … consciously, deliberately, collectively, into the next historical phase. The value of Indian traditions lies in the ability of their conserving forces to put a brake on hasty passage. Adjustment is the end-product of the dialectical connection between the two.
Meanwhile (there) is tension. And tension is not merely interesting as a subject of research; if it leads up to a higher stage, it is also desirable. The higher stage is where personality is integrated through a planned, socially directed, collective endeavour for historically understood ends, which means … a socialist order. Tensions will not ease there. It is not the peace of the grace. Only alienation from nature, work and man will stop in the arduous course of such high and strenuous endeavours. (1958: 76)
In view of this clear expression of faith (it is what, not a demonstration), it is not surprising that he should have hold Indian sociologists (in 1955) that their 'first task' was the study of 'social traditions' (1958: 232), and should have reminded them that traditions grow through conflict.
It is in the context of this emphasis on tradition that his specific recommendation for the study of Mahatma Gandhi's views on machines and technology, before going ahead with 'a large scale technological development' (1958: 225), was made. It was not small matter that from the Gandhian perspective, which stressed the value of wantlessness, non-exploitation and non-possession, the very notions of economic development and underdevelopment could be questioned (ibid.: 206).
But, this was perhaps only a gesture (a response to a poser), for DP maintained that Gandhi had failed to indicate how to absorb the new social forces which emerged from the West”; moreover, “the type of new society enveloped in the vulgarized notion of Ramarajya was not only non-historical but anti-historical” (ibid.: 38). But he was also convinced that Gandhian insistence on traditional values might help to save Indians from the kind of evils (for example, scientism and consumerism) to which the west had fallen prey (ibid.: 227).
The failure to clearly defined the terms and rigorously examine the process of synthesis, as already noted above, re-appears here again and indeed repeatedly in his work. The resultant 'self-cancellation', as Gupta (1977) puts it, provided certain honesty and certain pathos to DP's sociology. In fact, he himself recognized this when he described his life to AK Saran as a 'series of reluctances' (Saran, 1962: 162). Saran concludes: DP did Vedanta, western liberalism, Marxism – which all beckoned to him 'do not mix'.
8. Music:
DP's Introduction to Music (1945) is a sociological piece which can be compared with The Rational and Social Foundations of Music by Max Weber (tr. and ed. by Don Martindale, London, 1958). DP's work even today remains only of its kind. It shows that “Indian music, being music, is just an arrangement of sounds; being Indian, it is certainly a product of Indian history”.
He further shows both the similarities and differences between Indian music and western music. In both regions, religious and folk music had been the inevitable context of classical music. In both, classical music at moments of crisis had drawn from people's music for fresh life, elaborated its leisure, and imposed sophisticated forms upon it in return.
Music was equally intimate with functions of collective living and equally susceptible to the genuine influences that worked upon the culture pattern. So long as the princely courts, the priestly dignitaries and strongly entrenched guilds fixed the rule of living, Indian and I European music alike betrayed the rudiments of melody and harmony.
Since then, the tempo of change has been slower in India than in Europe, according, partly, at least, for the so-called 'spiritually' of her music. In fact, the community and the homogeneity of Indian music are astonishing (1945: 8).
निष्कर्ष:
Dhurjati Prasad Mukerji was one of the founding fathers of sociology in India. He had fairly long tradition of intellectual pursuits. Being an intellectual meant two things to DP. First, discovering the sources and potentialities of social reality in the dialect of tradition and modernity, and, second developing an integrated personality through pursuit of knowledge.
Indian sociologists, in his opinion, suffered from a lack of interest in history and philosophy and in the dynamism and meaningfulness of social life. Paying attention to specificities in a general framework of understanding was the first principle derived from Marx. DP developed this methodological point in an important essay on the Marxist method of historical interpretation.
He embraced Marxism in various ways, ranging from a simple emphasis upon the economic factor in the making of culture to an elevation of practice to the status of a test of theory.
We found an explanatory exposition of a selected aspect of DP Mukerji's sociological writings, using as far as convenient to his own words. The theme of 'tradition' and 'modernity' occupies an important place in his work and also survives as a major concern of contemporary sociology.
Taking DP's work as a whole, one soon discovers that his concern with tradition and modernity, which became particularly salient during the 1940s and remained so until the end, was in fact a particular expression of a larger, and it would seem perennial concern of westernized Hindu intellectuals. This concern manifested in a variety of ways. There is an urge for a synthesis of Vedanta, western liberalism and Marxism.
The work of DP Mukerji is quite significant in building sociology of India. He was deeply influenced by Marxian thought as is evident in his emphasis on economic factors in the process of cultural change. We find that how he looks at the impact of the west on the Indian society as a phase in the social process of cultural assimilation and synthesis. In his view, Indian culture has grown by a series of responses to the successive challenges of so many races and cultures, which has resulted in a synthesis.
Mukerji's basic ideas remain relevant for sociology in India even today. He showed that development of man or person is conditioned by the social milieu. Therefore, national independence, economic development and the resolutions of class contradiction within society are necessary conditions for human development in countries like India.
Nevertheless, they are not sufficient conditions. Appropriate values for integrating autonomy of the self with collective interests, rationality with emotionality and care for tradition will have to be created. A study of Indian tradition and its dialectical relation with the forces of modernity may suggest how such values are generated.
DP's greatest contribution lies in his theoretical formulations about the role of tradition in order to analyse social change. He reminded us that the Indian social reality could be properly appraised only in terms of “its special traditions, special symbols and its special patterns of culture and social actions”.