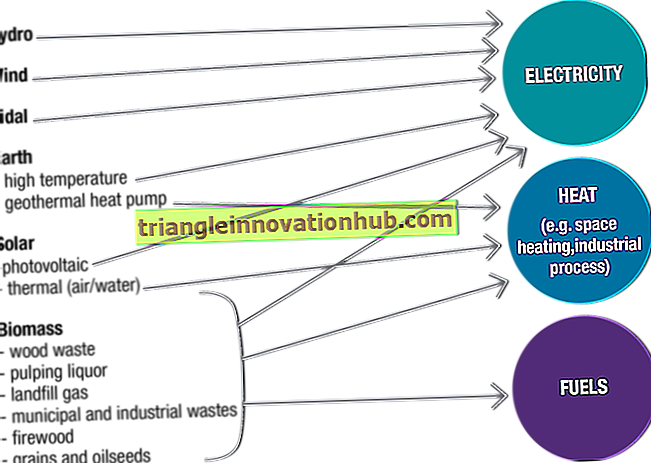ऋग्वेदिक समाज में स्तरीकरण
ऋग्वेदिक समाज में स्तरीकरण!
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के लिए आलोचना के आधुनिक ऐतिहासिक और दार्शनिक तरीकों के आवेदन के बाद से, बड़ी संख्या में विद्वानों और गैर-विद्वानों ने ऋग्वेद के आधार पर प्रारंभिक वैदिक समाज के पुनर्निर्माण का प्रयास किया है; अभी तक ऋग वैदिक समाज की तस्वीर धुंधली और विवादास्पद बनी हुई है। हाल के वर्षों में, पांच वर्षों के थोड़े समय में, तीन प्रख्यात विद्वानों-जीएस घुरे, आरएस शर्मा और रोमिला थापर ने इस विषय से संबंधित मोनोग्राफ प्रकाशित किए हैं और उनमें से प्रत्येक ने इतिहास और सामाजिक नृविज्ञान द्वारा प्रदान किए गए टूल का उपयोग किया है।
फिर भी, वे बहुत अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ब्रूस लिंकन का काम, जो उसी समय के बारे में प्रकाशित होता है, विषय में पश्चिमी मानवविज्ञानी के निरंतर हित को दर्शाता है। यह एक क्रॉस-सांस्कृतिक पद्धति के माध्यम से ऋग वैदिक धर्म और समाज के पारिस्थितिक संदर्भ को स्थापित करने का प्रयास करके एक नया आयाम जोड़ता है। प्रतिमानों की बहुलता और साक्ष्य की परस्पर विरोधी व्याख्याएं इन ऐतिहासिक-मानवशास्त्रीय आधारों के सैद्धांतिक और अनुभवजन्य आधारों का मूल्यांकन करती हैं, जो एक आवश्यक डिसाइडेरेटम हैं।
जीएस घोरी समाजशास्त्रियों की उस दुर्लभ नस्ल से संबंधित हैं जो ऐतिहासिक अभिलेखों के व्यापक अध्ययन के साथ नृवंशविज्ञान के अपने ज्ञान को बाधित करते हैं। उनका वैदिक भारत एक स्वैच्छिक कार्य है जो वैदिक भारत के लगभग हर पहलू का अध्ययन करने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक और नृवंशविज्ञान संबंधी डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है, जो प्रारंभिक भारत-यूरोपीय लोगों के सांस्कृतिक परिसर से शुरू होता है, जो उन क्षेत्रों के गैर-साक्षर लोगों द्वारा कवर नहीं किया जाता है वैदिक लोग और उनका साहित्य।
वह इस कथन के साथ शुरू होता है कि वैदिक काल C.2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है, लेकिन बाद में यह निष्कर्ष निकालने के लिए इस दृष्टिकोण को संशोधित करता है कि रिग वैदिक इंडो-आर्यन ने 2200 ईसा पूर्व के आसपास भारत में प्रवेश किया था। उनके अनुसार, ऋग वैदिक भजनों की रचना की गई थी चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और तेरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व की पहली छमाही; कुछ 2000 ईसा पूर्व के आसपास और कुछ देर से 1000 ईसा पूर्व के आसपास रचे गए थे
वह परगिटर से सहमत हैं कि ऋग्वेद का संकलन लगभग 980 ईसा पूर्व में हुआ था; और वैदिक और महाकाव्य-पुराणिक स्रोतों से भाषाई साक्ष्य के साथ-साथ "पारंपरिक इतिहास" के आधार पर वह पूर्व-ऋग-वैदिक इंडो-यूरोपीय लोगों की एक पूर्व लहर के आगमन को दर्शाता है, जो पूर्व में बसने के लिए चले गए मगध और कोसल के क्षेत्र।
वैदिक काल के बाद की ब्राह्मणवादी संस्कृति, उनके विचार में, मुख्य रूप से भारत-आर्यों की इन दो लहरों के बीच बातचीत का परिणाम थी। हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक स्थलों की अपनी चर्चा में वे भारत से बाहर स्थित उन लोगों को छोड़ देते हैं, जो कि भरत हैं, और यद्यपि वे शुरुआती वैदिक चरण को हड़प्पा संस्कृति के एक समकालीन समकालीन मानते हैं, उन्हें नहीं लगता कि बाद वाले ने पूर्व को प्रभावित किया था ; उनके विचार से दोनों का सांस्कृतिक वातावरण एक-दूसरे से बिलकुल अलग था।
यह अजीब बात है कि यद्यपि घोरी की पुरातात्विक सामग्री में व्यापक जांच से स्पष्ट है कि वैदिक जनजातियों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में शहरी बस्तियों का शायद ही कोई निशान है, उन्हें मुखरता से कोई संकोच नहीं है, केवल ऋग वैदिक की अपनी व्याख्याओं के आधार पर। भजन, कि ऋग वैदिक समाज की संस्कृति "अनिवार्य रूप से एक शहरी" थी।
लेकिन ये सवालों के घेरे में हैं और इस संबंध में उद्धृत किए गए भजनों की व्याख्या अलग तरीके से की जा सकती है, जो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त चित्र के अनुरूप है। उनके कुछ निष्कर्ष काफी भड़कीले हैं, हालांकि उनके तर्क में उन्हें बहुत अधिक वजन दिया गया है। इस प्रकार घुरे का तर्क है कि ऋग्वेद में दो-घोड़ों और यहां तक कि चार-घोड़ों के रथ के संदर्भ में संकेत मिलता है कि ऐसे वाहन काफी संख्या में थे और यह "काफी चौड़ी और अच्छी सड़कों" और "काफी बड़ी बस्तियों" के अस्तित्व को बनाए रखता है।
हालांकि, एक मोबाइल फाइटिंग प्लेटफॉर्म और योद्धा कुलीनता के लिए एक वाहन के रूप में घोड़े से तैयार रथ का उपयोग भारत-यूरोपियों के साथ पूर्व और पश्चिम दोनों में फैल गया; और जो कुछ भी उनकी उत्पत्ति का स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे एक शहरी नहीं थे, बल्कि एक पशुपालक खानाबदोश लोग थे, जो बेहतर चरागाहों की तलाश में अपनी गाड़ियों और रथों के साथ आगे बढ़ रहे थे।
वैरी इंडेक्स के लेखक घोरी ने मैकडोनेल और कीथ ने कहा कि घुड़दौड़ वैदिक भारतीयों का पसंदीदा शगल था। लेकिन कुइपर, हेस्टरमैन और स्पैरम्बूम जैसे विद्वानों के हालिया शोधों ने यह स्थापित किया है कि प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता ने मूल यज्ञ अनुष्ठान का एक आंतरिक हिस्सा बनाया, जो आर्यन खानाबदोशों की ट्रैकिंग और पुनर्वास गतिविधियों के साथ निकटता से जुड़ा था। रथ-रेसिंग लोकप्रिय उत्सव या खेल का एक रूप नहीं था, लेकिन एक गंभीर चिंता का विषय था।
यह बलिदान के आर्य अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ था और बैंड के नेतृत्व के सवाल, उनके भटकने के दौरान उनके अस्थायी निवास के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन, और इस तरह के मुद्दों को हल करने में एक मौलिक भूमिका निभाई। इस चरण में पवित्र और सांसारिक पूरी तरह से एकीकृत और अविभाज्य थे।
घुरे को इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हस्तिनापुर में खुदाई वैदिक युग में गंगा-यमुना क्षेत्र में रहने वाले शहरी लोगों को चित्रित करने और पेंट्री ग्रेवेयर की तारीखों को प्रदान करने में विफल रही है, जो वैदिक आर्यों के साथ कुछ पुरातत्वविदों से जुड़े हैं, वे नहीं कर सकते। एक सबसे उदार अनुमान पर भी 1100 ईसा पूर्व से परे धकेल दिया। अधिकांश पीजीडब्ल्यू साइटों ने 800-500 ईसा पूर्व के बीच की तारीखों का उत्पादन किया है और जैसे कि बाद में वैदिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं।
यूपी की ताम्रयुगीन संस्कृतियों के लिए, घोरी अपने उपयोगकर्ता की धारणा "असभ्य" और "खानाबदोश" होने पर विवाद करता है, लेकिन यह मानता है कि वे शहरी नहीं थे। घुरे के दृष्टिकोण से भरतपुर जिले के नोह और राजस्थान के अहर में की गई खुदाई अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी राय में भरतपुर पर ऋग-वैदिक काल में मत्स्य द्वारा कब्जा किया गया था; लेकिन ये फिर से, उसकी शहरी परिकल्पना का समर्थन नहीं करते हैं।
अठारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, अपने शुरुआती स्तरों पर, अहर की बनस संस्कृति, तांबे की संस्कृति है, जिसमें लोहे का कोई निशान नहीं है। नोह में लोहे की वस्तुएं 725 ईसा पूर्व के लिए उपयोग करने योग्य हैं, लेकिन इन पुरातात्विक लाखुनी घोरी का दावा है कि ऋग्वैदिक आर्य न केवल लोहे से परिचित थे, बल्कि लोहे के किलों को रखने के लिए कम से कम वांछित थे।
ऋग्वेद में लोहे के संदर्भों को अयस शब्द की व्याख्या लोहे के रूप में की गई है। प्रारंभ में, घुरे कुछ हिचकिचाहट दिखाता है, क्योंकि वह "या तो कांस्य या लोहे" के रूप में अयमाया का अनुवाद करता है। लेकिन जब वह ऋग्वैदिक काल की एक उच्च परिष्कृत गतिहीन शहरी संस्कृति की कल्पना करता है, जब कस्बे की महिलाएं नग्न अवस्था में महिलाओं की सुंदर प्रतिमाओं से सुशोभित होती हैं, तो वह अधिक से अधिक आश्वस्त हो जाता है कि अयस का मतलब केवल लोहे से होना चाहिए। हालांकि, ऋग्वेद में महत्वपूर्ण अंशों की एक परीक्षा एसए डांगे, एक संस्कृतिकर्मी का नेतृत्व करती है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि ऋग्वेद में अय्यस "लोहे को इंगित नहीं करता है ..." (यह) स्पष्ट रूप से लाल भूरे रंग की धातु (तांबा या कांस्य) को इंगित करता है। ।
ऋग वैदिक समाज की एक तस्वीर के पुनर्निर्माण में एक बड़ी समस्या इस तथ्य से उपजी है कि यद्यपि यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि ऋग वैदिक भजनों की रचना की अवधि लगभग पांच सौ साल से अधिक है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक फैली हुई है- घुरे इसे एक हज़ार साल तक विस्तारित किया गया है - भजन के सापेक्ष कालक्रम के आधार पर सामाजिक विकास पर आंतरिक साक्ष्य को निचोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं।
कुछ हद तक यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि, जैसा कि ब्लूमफील्ड ने बताया कि ऋग वैदिक भजन काफी हद तक पात्र में "एक अस्थायी अनाम साहित्य के अंशों से निर्मित" हैं, जैसा कि वाक्यांश नव्यम सन्यास की लगातार घटना से संकेत मिलता है, "एक प्राचीन देवता के लिए पुराने गीत का नवीनीकरण"।
ब्लूमफील्ड ने चेतावनी दी कि यहां तक कि परिवार की पुस्तकों को कालानुक्रमिक इकाइयों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने और नए भजन उनमें से हर एक में निहित हैं। फिर भी, हमारी राय में, सावधानी के ये शब्द भजन के सापेक्ष कालक्रम को स्थापित करने और उस आधार पर सामान्यीकरण करने के सभी प्रयासों के त्याग को उचित नहीं ठहराते हैं। इस तरह का एक अभ्यास आवश्यक रूप से कुछ सैद्धांतिक परिसरों पर आधारित होगा, जो कि उपलब्ध अनुभवजन्य साक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए।
उदाहरण के लिए, ब्रूस लेमोनोन दर्शाता है कि प्रथम बलिदान में आदिम लोगों के मारे जाने और उनके विघटित शरीर से ब्रह्माण्डों का फैशन करने का मिथक भारत-यूरोपीय समय में वापस चला जाता है और इसके नॉर्स, रोमन और इंडो-आर्यन में पता लगाया जा सकता है। संस्करण, अंतिम उल्लेख ऋग्वेद के एक्स मंडला में प्रसिद्ध पुरुषसूक्त भजन है। लेकिन यद्यपि यह मिथक निस्संदेह पुराना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पुरुषसूक्त भजन में व्यक्त किए गए सभी विचारों में एक इंडो-यूरोपीय अतीत है।
पूरे ऋग्वेद में यह एकमात्र ऐसा भजन है जो समाज के जाने-माने चार गुना वर्जन विभाजन की बात करता है और “राज्य” और “सुद्र” शब्दों का उल्लेख करता है। स्पष्ट रूप से इस भजन के संगीतकार ने एक नई सामाजिक स्थिति को धार्मिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक पुराने मिथक को याद किया। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि एक्स मंडला और ऋग्वेद के I मंडला के पहले पचास भजन लगभग पाँच सौ साल या S05 .5 से पारिवारिक पुस्तकों, यानी II-VII मंडलों से अलग किए गए हैं। परिवार की पुस्तकों में सबसे पुरानी परत शामिल है।
एक मध्यवर्ती चरण भी था जब संहिता संग्रह आठवीं मंडली के साथ समाप्त हो गया था और वालखिल्य भजनों के रूप में एक समय के बाद इसके साथ एक पूरक जुड़ा हुआ था। I मंडला के भजन ५१-१९ १ को उसी तिथि का माना जाता है जिसे VIII मंडला और IX मंडला कहा जाता है, और इसे X मंडला की तिथि के करीब माना जाता है। कृषि गतिविधियों के संदर्भ ज्यादातर पुस्तकें I और X में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ एक पूर्व-हल चरण को दर्शाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को एक व्रक के साथ मोड़ते हैं, अर्थात एक खुदाई छड़ी या कुदाल, लेकिन अक्सर हल से गलती से अनुवाद किया जाता है ।
कित्सरापति (खेतों का स्वामी) को समर्पित पुस्तक, IV का एक भजन, मोना-विलियम्स के अनुसार सुआ-सिरा ("हल" और "साझा" की शक्तियां) और सीता (फर्रा) को हॉपकिन्स द्वारा एक देर से प्रक्षेप के रूप में माना जाता है। किसी भी दर पर, ऋग्वेद के बाद के खंडों में होने वाले हल कृषि के संबंध में गैर-आर्यन ऋण शब्द का उपयोग यह बताता है कि ऋग्वेदिक आर्यों ने इस प्रथा को स्वदेशी लोगों से सीखा था, हालांकि इस तरह के उधार एक निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं हैं ऋग्वेद में "आर्यन और गैर-आर्यन के अभिसरण" का सिद्धांत, जैसा कि माधव एम। देशपांडे द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
गैर-आर्यों के साथ कुछ संपर्क, संघर्ष और टकराव के सबूत हैं, लेकिन ऋग्वेद पूर्व-आर्यन दस्तावेज़ के रूप में पूर्व में बना हुआ है। इसकी पुष्टि भी एफ.बी.जे. कुइपर, जिन्होंने दिखाया है कि वीआईई मंडला में होने वाली बोअर मिथक एक ऑस्ट्रो-एशियाटिक मिथक का आर्यनाइज्ड संस्करण है। कुइपर कहते हैं कि यद्यपि गैर-आर्यों के ब्राह्मणवादी हलकों में आत्मसात करने और ऋग्वेद के बाद के मंडलों में कुछ विदेशी मिथकों के अनुकूलन के कुछ सबूत हैं, "हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इस तरह के कॉर्पोरा अलीना को वास्तव में स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया था। पहले से ही ऋग्वेदिक काल में। "
उनके विचार में, जबकि पुजारी परिवारों के नाम जिन्हें पुस्तकों II-VII के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, आर्यन हैं, कण्व, जिन्हें आठवीं मंडली के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, स्पष्ट रूप से एक गैर-आर्यन नाम है, और बोअर मिथक, जो बरकरार रखता है प्रोटो-मुंडा मूल के निशान, विशेष रूप से कण्व परिवार के भजनों में पाए जाते हैं।
यह भी दिलचस्प है कि पके हुए चावल-दूध (ksirapakam odanam) का उल्लेख केवल दो बार और केवल इस मिथक के संबंध में होता है। एक्स मंडला के लेखकों में गैर-आर्यन विदेशी नाम अधिक हैं, जैसा कि अनुक्रमणी में दिया गया है, लेकिन "ऋग वैदिक पौराणिक कथाओं पर आदिवासी प्रभाव शायद ही बहुत व्यापक रहा हो"।
इस प्रकार, ऋग वैदिक भजनों की रचना और संकलन द्वारा कवर लंबी अवधि यह अनिवार्य बना देती है कि कोई ऋग वैदिक साक्ष्य की विभिन्न परतों को भेदने की कोशिश करता है और एक इंडो-यूरोपीय विरासत का गठन करने से पहले सभी तर्कों को ध्यान से तौलता है और जिसे समझाया नहीं जा सकता है। रिग वैदिक समाज की आंतरिक गतिशीलता के संदर्भ में, लेकिन एक गैर-आर्यन स्रोत से उधार के रूप में देखा जाना चाहिए।
समस्या को इस तथ्य से जटिल किया जाता है कि शब्द सामाजिक संदर्भ में परिवर्तन में अपने अर्थ बदलते हैं और नई बारीकियों को उनके मूल अर्थों से काफी अलग करते हैं, लेकिन वैदिक छात्रवृत्ति अक्सर एक स्थिर दृष्टिकोण से ग्रस्त होती है जो बाद के बदलावों को देखती है, वैदिक काल में केवल विस्तार के मामलों के रूप में। बिना किसी मूलभूत अंतर के "आदेशित विकास"।
हालांकि, जैसा कि वैदिक अनुष्ठान के कुछ हालिया अध्ययनों से पता चला है, विचारों और प्रथाओं के दायरे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, और एक अर्ध-खानाबदोश देहाती लोगों के जीवन में होने वाले भौतिक परिवर्तनों के साथ निकटता से जुड़े थे, जो इस प्रक्रिया में थे गतिहीन जीवन और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तन बनाने की।
अभ्यास जो उनके निर्वाह के पहले मोड के लिए आंतरिक थे, बाद के वैदिक अनुष्ठान में औपचारिकता प्राप्त की और उनके विश्लेषण से उनके मूल महत्व को दिलचस्प सुराग मिलते हैं। यह बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल की समाप्ति के दौरान परंपरा में पले-बढ़े लोगों के लिए भी कुछ भजन अवैध हो गए थे।
यदि यह अनुष्ठान और पवित्र विद्या के क्षेत्र में स्थिति है, तो यह पहले के सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को पहले के अतीत के साथ पेश करने के प्रलोभन के खिलाफ रक्षा करने के लिए आवश्यक है। एमिल बेनेविस्टे ने तर्क दिया है कि 'बिक्री' और 'खरीद' की धारणा भारत-यूरोपीय लोगों के बीच बिक्री के संदर्भ में उभरी है, जो उन पुरुषों की नीलामी के जरिए हुई है जो युद्ध के कैदी हो सकते हैं या जुए में अपनी स्वतंत्रता खो सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक डेटा इसकी पुष्टि करता है।
वासना और सुल्का जैसे शब्द जो ऋग्वेद में 'मूल्य' या 'मूल्य' को दर्शाते हैं, का उपयोग माल या वस्तुओं के संबंध में नहीं किया जाता है, बल्कि मनुष्य और देवताओं को किया जाता है जो मनुष्यों के बाद मॉडलिंग करते हैं। इस प्रकार एक स्थान पर "दो दासों, वरसीन और सांबरा को वासनायता के रूप में वर्णित किया गया है, " फिरौती की मांग करना "जाहिरा तौर पर युद्ध के कुछ कैदियों को ले जाने के लिए, और इंद्र द्वारा मारे गए।
एक अन्य स्थान पर वसन एक हाइमर की बोली को बेचने के संदर्भ में होता है और बाद में अपने इंद्र को बेचने के लिए पुनर्खरीद करता है, जो कि उसे खरीदता है। हालांकि भजन का महत्व अस्पष्ट है, लेन-देन की प्रकृति स्पष्ट रूप से मनुष्यों की बिक्री और छुटकारे के बाद बनाई गई है।
III मंडला के एक भजन में भक्तों को और उनके 'तीतर जानवरों' (पसेव) को नमकीन भोजन देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें शर्त के साथ-साथ चौपाया भी शामिल है। मा या ऋण का संदर्भ आमतौर पर उन लोगों से संबंधित होता है, जो वैदिक सूचकांक में अनुबंधित हैं और वैदिक इंडेक्स के लेखक इसे "वैदिक भारतीयों की एक सामान्य स्थिति" के रूप में बोलते हैं।
यह सही माना जाता है कि ऋग्वेद में व्यावसायिक गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं है। विशेष रूप से कीमती धातु या "प्रतिष्ठा" सामान प्राप्त करने के लिए बस सरप्लस सामानों का बार्टर हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यापारी या बिचौलिये धन के प्रसार और उत्पादन में भूमिका नहीं निभाते।
कभी-कभी ऋग्वेद में वर्णित पनीस को अमीर, स्वार्थी, "शत्रुतापूर्ण भाषण" और लालची के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्हें "व्यापारियों के लिए श्रेष्ठता" कहा जाता है, जो सूदखोरी करते थे। लेकिन इस दृष्टिकोण का कोई ठोस आधार नहीं है। एक मैकडोनेल और कीथ के साथ सहमत होने के लिए इच्छुक है कि "यह शायद ही पानिस के संबंध में अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है क्योंकि गायकों द्वारा इष्ट देवताओं की पूजा नहीं की जाती है" और यह शब्द पर्याप्त रूप से आदिवासियों या शत्रुतापूर्ण आर्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त है राक्षसों के रूप में भी।
इस प्रकार, ऋग-वैदिक आंकड़ों की एक अधिक खोज और तर्कसंगत व्याख्या, वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में घोरी के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है; और उनकी मान्यता है कि ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पहले से ही 'लगभग एक जाति' या वर्ग जैसी श्रेणी के थे।
आरएस शर्मा और रोमिला थापर द्वारा समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, दोनों ऋग वैदिक समाज को अनिवार्य रूप से देहाती के रूप में देखते हैं। फिर भी, उनके विचारों में महत्वपूर्ण अंतर हैं कि ऋग्वेदिक लोगों में सामाजिक विभेद किस हद तक हुआ था; और इन्हें कुछ विस्तार से जांचना होगा।
आरएस शर्मा का तर्क है कि यद्यपि ऋग्वेद में 'बैंड' प्रणाली के कुछ सबूत हैं, एक पूर्व-आदिवासी मंच जिसमें रक्त से संबंधित लोगों का एक समूह भोजन-सभा, शिकार या लड़ाई, समाज के लिए एक साथ नहीं आता है पूरा 'आदिवासी, देहाती और बड़े पैमाने पर समतावादी' था। जीविका का मुख्य स्रोत मवेशी थे न कि कृषि उत्पाद।
पशु-चरवाहों के अलावा, अंतर-आदिवासी युद्धों में लूट पर कब्जा आजीविका का एक प्रमुख स्रोत था। उन्होंने मार्क्स की बहुचर्चित टिप्पणी को उद्धृत करते हुए कहा कि मानव-शिकार पशु-शिकार का तार्किक विस्तार था और यह तर्क देता है कि रिग वैदिक जनजातियों के समतावादी लोकाचार को आदिवासी प्रमुख द्वारा लूट के असमान वितरण द्वारा रेखांकित किया गया था।
ऋग्वेद में रथ पर सवार अमीर लोगों और बड़ी संख्या में मवेशियों को रखने का उल्लेख है; लेकिन समाज न तो धन के अंतर पर और न ही श्रम के सामाजिक विभाजन पर संगठित था। यह परिजनों पर आधारित था, जो विभिन्न आकारों और आकारों की परिजनों की जरूरतों की एक किस्म को पूरा करने के लिए था, और रैंकों का विभेदीकरण था, लेकिन कोई वर्ग भेदभाव नहीं था।
संक्षेप में, यह एक पूर्व-राज्य की राजनीति थी, जो धीरे-धीरे अधिक से अधिक भेदभाव की ओर बढ़ रही थी, जैसा कि ऋग वैदिक साहित्य के नवीनतम स्तर से संबंधित डैनस्टुटिस द्वारा इंगित किया गया है। ये इंगित करते हैं कि लूट का एक बड़ा हिस्सा प्रमुखों और पुजारियों द्वारा एक असमान पुनर्वितरण प्रणाली के लिए अग्रणी था; लेकिन दूसरे वर्ग के श्रम से दूर रहने वाले एक वर्ग की घटना अभी तक 'किसी भी महत्वपूर्ण डिग्री' में उभरने की नहीं थी।
इसकी व्यापक रूपरेखा में ऋग वैदिक समाज का शर्मा पुनर्निर्माण काफी प्रशंसनीय है। हाल ही में युद्ध के आर्थिक महत्व और 'लूट-उत्पादन' को अस्वीकार करने का प्रयास किया गया है, जैसा कि शर्मा कहते हैं, ऋग वैदिक समाज में इस आधार पर कि युद्ध दैनिक दिनचर्या का विषय नहीं हो सकता था क्योंकि इसमें विनाश शामिल था। जीवन और संपत्ति।
फिर भी, धारणा के पास अच्छा सैद्धांतिक और साथ ही डेटा-आधारित समर्थन है। वीर युग के ग्रीस की उनकी चर्चा में मार्क्स और एंगेल्स एक ऐसे मंच के रूप में 'सैन्य लोकतंत्र' की बात करते हैं, जब पुरानी सज्जन प्रणाली अभी भी जोश से भरी हुई थी, लेकिन क्षय शुरू हो गया था और आंतरिक युद्ध प्रणालीबद्ध एड्स के रूप में पतित हो गया था " मवेशियों, दासों और खजाने को एक आजीविका प्राप्त करने के नियमित साधन के रूप में कैप्चर करना। मार्शल डी। सहलिन्स ने इस अवधारणा को और तर्क देकर विकसित किया कि खंड वंशावली प्रणाली शिकारी विस्तार का एक संगठन थी। Th खंड वंश ’शब्द मार्क्स और एंगेल्स के आख्यानों में गेंस’ के आधुनिक मानवशास्त्रीय समकक्ष है।
रोमिला थापर द्वारा भी मवेशियों के छापे के महत्व पर जोर दिया जाता है, और वंशावली से लेकर राज्य तक के उनके मोनोग्राफ में वह रिग वैदिक समाज के लिए कुछ मानवशास्त्रीय मॉडल और अवधारणाओं को लागू करने का एक अग्रणी प्रयास करता है। वह 'आदिवासी' शब्द के प्रयोग से बचती है, उन मानवशास्त्रियों की आलोचना से सहमत है जो इस अवधारणा को थोड़ा विश्लेषणात्मक मूल्य मानते हैं। लेकिन उनके काम में प्रयुक्त 'वंश समाज' की वैकल्पिक अवधारणा हमें कोई कम अस्पष्ट और एक 'पकड़' अवधारणा नहीं लगती है; क्योंकि वह इसे न केवल एक वंशज वंश समूह के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि एक स्थिति जिसे वह अपने कार्य की शुरुआत में अपनाता है - लेकिन यह भी कबीले और अन्य परिजन-समूह, 'वंश समाज' केवल परिजनों के लिए एक मौखिक विकल्प बन जाता है। 'या' आदिवासी 'समाज।
एक सक्षम समीक्षा लेख में एएम शाह ने ऋग वैदिक लोगों के लिए सामाजिक-मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से 'वंश समाज' के मॉडल की वैधता पर सवाल उठाया है; लेकिन उन्होंने उत्पादन के वंश मोड की संबद्ध अवधारणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। शाह ने थापर द्वारा निर्विवाद रूप से उद्धृत आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा कि वे इस आधार पर इतिहासकार नहीं हैं। लेकिन हमारी राय में थापर द्वारा ऋग वैदिक समाज पर लागू की गई उत्पादन की वंशावली पद्धति की बहुत धारणा, अवधारणा के गलत उपयोग और डेटा की अशुद्धि दोनों के कारण गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है।
थापर वंशावली की सटीक परिभाषा के साथ शुरू होता है जैसा कि मध्य- टन और टैट द्वारा दिया गया है:
वंशानुक्रम अधिकार के एक औपचारिक प्रणाली के साथ असभ्य परिजनों का एक कॉर्पोरेट समूह है। इसके अधिकार और कर्तव्य हैं और बंधन कारक के रूप में वंशावली संबंधों को स्वीकार करता है। इसे छोटे समूहों या खंडों में विभाजित किया जा सकता है। कई अविनाशी वंश समूह एक कबीले बनाने के लिए जाते हैं जो इसके मूल को एक वास्तविक या पौराणिक पूर्वज का पता लगाता है।
इस तरह की प्रणाली में मूल इकाई तीन या चार पीढ़ी के वंश पर आधारित विस्तारित परिवार है जो सबसे बड़े पुरुष द्वारा नियंत्रित होती है जो इसे अनुष्ठान और राजनीतिक अवसरों पर प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की प्रणाली में सबसे व्यापक राजनीतिक इकाई को तंत्रिका समुदाय कहा जाता है।
थापर अवलोकन:
न्यायिक समुदाय निर्णय लेता है और प्रमुख प्रामाणिक वंश खंडों से गठित किया जाता है। उत्पादन के वंश मोड में, तंत्रिका समुदाय का उत्पादन पर कुछ नियंत्रण होता है और इसकी अंतर्निहित शोषणकारी प्रवृत्ति इसे अधिक समतावादी बैंड और रैंक वाले समाज से अलग करती है। शोषण उन लोगों के रूप में होता है जो अधिकार में परिजनों के कनेक्शन और धन के आधार पर शक्ति का दावा करते हैं और उन लोगों को छोड़कर जो असंबंधित हैं। इस बहिष्करण को गैर-परिजन समूहों में श्रम के लिए व्यक्त किया जा सकता है।
ऐसी प्रणाली में उत्पादन, चाहे वह श्रम के माध्यम से या छापे से प्राप्त किया गया हो, को पुनर्वितरण के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसमें स्वैच्छिक श्रद्धांजलि और उपहार देना एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। रिश्तेदारी के संबंध वंशावली आधार होते हैं और साथ ही वंश, खंड और विस्तारित परिवारों के अनुसार एक इकाई उत्पादन होते हैं। कुलीन समूहों और आम लोगों के बीच एक स्पष्ट अलगाव में, रिश्तेदारी वंशावली कनेक्शन के माध्यम से सत्तारूढ़ वंश के अधिकार की स्थापना के लिए एक चार्टर का गठन करती है।
थापर ने इमैनुएल टेरय को अपना ऋण स्वीकार किया, जिन्होंने उत्पादन के वंश मोड की अवधारणा को प्रतिपादित किया, और पीपी रे, मौरिस गोडेलियर और क्लाउड मीलासौक्स के विचार, जिन्होंने इस पर टिप्पणी की। लेकिन यह स्पष्ट है कि उत्पादन की वंश विधा की उसकी धारणा ऊपर उल्लिखित विद्वानों से काफी भिन्न है। उदाहरण के लिए, टेरेट के मॉडल में सत्ता और धन से बाहर रखते हुए "दूसरों के लिए श्रम न करने वाले समूहों" के शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। Terray और Meillassoux दोनों स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उत्पादन का वंश मोड स्व-निर्वाह और अल्पकालिक उत्पादन तकनीकों पर आधारित है।
इसलिए उत्पादन और उपभोग की इकाइयाँ एक ही तंत्र के माध्यम से समान सिद्धांतों पर गठित की जाती हैं, और 'श्रम का शोषण' विशिष्ट रूप से अनुपस्थित है। टेरियर ने इन विशेषताओं को "उत्पादन की पद्धति की प्राप्ति में एक तत्व के रूप में कार्य करने के लिए रिश्तेदारी के लिए आवश्यक शर्त" के रूप में माना है।
उत्पादन के वंश मोड के भीतर शोषण की समस्या को उठाया जाता है और बड़ों या बूढ़ों की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के संबंध में बहस की जाती है, जो अपने स्वयं के वंश इकाइयों के कनिष्ठ सदस्यों और पुरुषों से अलग-अलग वर्गों में देखी जाने वाली महिलाओं के विपरीत होती हैं। विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए।
उत्पादन के मुकाबले प्रजनन के क्षेत्र में शोषण का प्रश्न अधिक है और महिलाओं के विवाह और आदान-प्रदान पर उनके नियंत्रण के माध्यम से बहस के केंद्र सामाजिक संरचना के प्रजनन को नियंत्रित करने में बड़ों की भूमिका निभाते हैं।
अलग-अलग पद लिए गए हैं। जबकि कुछ ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि मार्क्स द्वारा परिभाषित शोषण को इन रिश्तों में देखा जा सकता है, अन्य लोगों ने ठीक ही कहा है कि आयु और लिंग की जैविक घटनाओं पर आधारित समूहों को सर्वहारा वर्ग की वर्गों के समान ही समझ सकते हैं। और पूंजीवादी एक औद्योगिक समाज में हैं। लेकिन इन चर्चाओं में कहीं भी कबीले के वरिष्ठ सत्तारूढ़ वंशजों का जिक्र नहीं है, जो कबीले के वंशजों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि या 'आम लोगों' द्वारा दी गई श्रद्धांजलि के आधार पर काम कर रहे हैं और पूर्व की खपत के लिए देहाती और कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, थापर के प्रतिमान के साथ मामला।
दूसरे शब्दों में, जबकि फ्रांसीसी मानवविज्ञानी वंश के समाज में सामाजिक भेदभाव को सीमित करते हैं, जो वंश और कनिष्ठों के बुजुर्गों के बीच, थापर इसका विस्तार शासकों और आमजन के विशिष्ट रूप से स्तरीकृत समूहों को शामिल करने के लिए करते हैं, जिन्हें बाद के एक रूप के रूप में जाना जाता है। पुनर्वितरण शोषण। कोई आश्चर्य नहीं कि थापर के कथन से एएम शाह को संदेह होता है कि रजनीश और योद्धाओं के योद्धा समूह "पहले से ही ऋग्वेदिक काल में वर्ण-वर्ग थे।"
थापर के उत्पादन के वंश मोड की अवधारणा आम तौर पर 'चीफडोम' और 'शंकुधारी कबीले' के प्रतिमान के साथ आम है, जो कि टाय द्वारा प्रस्तावित उत्पादन के वंश मोड के साथ है। एक प्रमुख वंशावली में और न केवल कुछ व्यक्तियों को एक पदानुक्रमित क्रम में वर्गीकृत किया जाता है, और पुरुष अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं की परवाह किए बिना जन्म से मुख्य रूप से 'सामान्य' होते हैं।
सहलिंस इसे "आदिम समानता के परे एक मंच" के रूप में मानते हैं, लेकिन अभी तक एक वर्ग समाज के रूप में नहीं "यह उत्पादन या राजनीतिक सामंजस्य और एक उपेक्षित अंडरक्लास के रणनीतिक साधनों की कमान में एक शासक तबके में विभाजित नहीं है"। फिर भी, इसकी एक संरचना है जिसमें रैंक को वंश-वास्तविक या सक्रिय से जोड़ा जाता है, और धन और शक्ति तक पहुंच, अन्य सेवाओं के लिए दावे आदि 'पारिवारिक' प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं।
यह बताया गया है कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में कहीं और नहीं है, जिसमें पुरुषोत्तम का अपवाद है। यह लगभग उसी तिथि की एक देर की रचना है जो अथर्ववेद के बाद के भागों में है, जो बाद में वैदिक पाठ था। हालांकि, ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तकों में भी यह शब्द कई बार आता है, हालांकि ज्यादातर मामलों में इसका मतलब सिर्फ 'एक-एक' ही हो सकता है, क्योंकि यह एक या दूसरे प्रमुख देवता पर लागू होता है।
किसी भी दर पर, ऋग्वेदिक भजनों में रजन शब्द की घटना केवल यह दर्शाती है कि ऋग्वेदिक वंशों में 'बड़े आदमी', नेता या प्रमुख थे; यह स्वचालित रूप से साबित नहीं होता है कि राजा वरिष्ठ राजवंश वंश के प्रतिनिधि थे। एक्स मंडला के कुछ छंदों में बहुवचन में राजन का उल्लेख है। "सबसे महत्वपूर्ण होने के नाते हम प्रमुखों (रजवाहे) और हमारे बैंड के माध्यम से (सेनानियों, वृजन) के माध्यम से खजाने को जीत सकते हैं!"
एक अन्य कविता, आदिवासी विधानसभा में प्रमुखों की उपस्थिति की बात करती है। लेकिन इनमें से कोई भी संदर्भ बाकी जनजाति के ऊपर मौजूद वरिष्ठ वंश के अस्तित्व को साबित करने के लिए नहीं माना जा सकता है। 'राजन्य' शब्द की अनुपस्थिति, जिसका अर्थ है कि राजन के परिजन और जैसे कि प्रमुख के साथ वंशावली लिंक पर जोर देते हैं, इस संबंध में महत्वपूर्ण है।
यहाँ तक कि वामा शब्द, जो थापर द्वारा 'वंश' के समान है, ऋग्वेद में इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है। गोत्र, जो बाद के साहित्य में 'वंश' या 'वंश' का प्रतीक है, आमतौर पर ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक वंश समूह के बजाय 'काउपेन' के अर्थ में व्याख्यायित होता है।
इसके अलावा, थापर की राय में गोत्र प्रणाली केवल ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट थी और ब्राह्मण आर्यन वंश समाज के लिए एक 'एडेंडा' थे, जिसमें रजनीश और विज़ शामिल थे, तथाकथित वरिष्ठ और कनिष्ठ वंश। उस मामले में वंश की संस्था ऋग्वेद में बिना किसी पहचान चिह्न के होगी।
यह महत्वपूर्ण है कि उसकी थीसिस के समर्थन में थापर ऋग्वेद से कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन लगभग पूरी तरह से वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से सप्तपथ ब्राह्मण पर निर्भर करते हैं। एकमात्र ऋग वैदिक भजन ने उन्हें इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए उद्धृत किया कि 'जिन लोगों ने राजा को चुना है वे विज़ से अलग हैं- X.173.1 है।
लेकिन एक करीबी परीक्षा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस कविता के आधार पर ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जिसमें पुजारी उच्चारण करता है: “मैंने तुम्हारा (राजा) से अभिवादन किया है, हमारे बीच आओ, स्थिर और निर्लिप्त रहो; हो सकता है कि ये सभी विषय आपको (उनके राजा के लिए) (visastva sarva vanchantu), हो सकता है कि राज्य (या नियम? rastram) कभी भी आपसे न मिले ”।
एक अन्य तर्क ने इस दृष्टिकोण के समर्थन में आगे बताया कि "धन के अधिकारी बाकी जनजाति से अलग थे" एचडब्ल्यू बेली द्वारा अपने लेख में 'ईरानी आर्य और दाहा' नामक शीर्षक से निर्मित आंकड़ों की गलतफहमी पर आधारित है।
थापर लिखते हैं कि बेली का विश्लेषण "उन्हें यह बताता है कि आर्य (आर्या) स्वामी या धन के स्वामी के रूप में जाना जाता है", लेकिन वास्तव में बेली का अर्थ इंडो-ईरानी आर्य या आर्य से है, और लम्बी आर्या के लिए नहीं। । वह कहते हैं कि 'आर्य' शब्द (संक्षिप्त 'ए') एक जातीय नाम को बताने के लिए बहुत संकीर्ण था, लेकिन भारत में वैश्य जैसे समृद्ध वर्ग के लिए उपयुक्त था और निघंटु (11.6) और पाणिनी के रूप में इस तरह समझाया गया है अष्टाध्यायी (III.I.103)।
वह आगे कहते हैं कि 'आर्य' नैतिक अर्थों में 'अच्छी तरह से जन्मे' या 'कुलीन' का एक माध्यमिक अर्थ रखता है। दूसरे शब्दों में, बेली के अनुसार, आर्य ने मूल रूप से एक रईस को बदनाम किया था, जिसके पास 'धन' था, लेकिन बाद में इसका मतलब था कि जिसके पास कोई महान गुण था।
'आर्य' से व्रद्धी द्वारा प्राप्त अलंकृत आर्या 'रईसों से जुड़ा हुआ' था। बेली स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहाँ तक आर्या शब्द का संबंध है, एक प्रारंभिक अर्थ 'रईसों से जुड़ा' इस प्रकार एक जातीय नाम और गैर-जातीय उपयोग से लिया गया है। ' इस प्रकार बेली अनार्य को आर्य के द्वितीयक अर्थ से जोड़ती है न कि 'स्वामी, धन के स्वामी' के प्राथमिक अर्थ के साथ। लेकिन थापर आर्य और आर्या के बीच भ्रमित हो जाते हैं और गलती से सोचते हैं कि निघंटु और अष्टाध्यायी के संदर्भ आर्य का उल्लेख करते हैं।
उसके बाद वह तर्क देती है कि चूंकि इन ग्रंथों में 'आर्या' (लम्बी 'क' के साथ) का अर्थ है धन का स्वामी, या कुलीनता का सदस्य, यह अर्थ स्पष्ट रूप से ऋग वैदिक काल और आर्या से अस्तित्व में है। ऋग्वेद ने सामान्य आदिवासियों-आम लोगों से अलग एक बड़प्पन का गठन किया। इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्या शब्द "सामाजिक स्थिति और धन से संबंधित था और दौड़ के लिए नहीं"। आर्य और महान के बारे में बेली की व्याख्या आर्यन महान सदन की उनकी दृष्टि से जुड़ी हुई है, आर्य (संक्षिप्त 'a') 'संपत्ति', 'संपत्ति का धारक' ईरानी दाता या पुराने भारतीय के साथ बड़े करीने से विपरीत था दासा का अर्थ होता है 'सेवक' या 'निर्वाहकर्ता'। लेकिन 'जोरोस्टर की दृष्टि', जैसा कि वे कहते हैं, ऋग वैदिक भारत के समाज को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि अवेस्ता समय-समय पर ऋग्वेद से दूर है। बेली ने वैदिक चरण के अंत तक होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा है, और उनकी थीसिस बाद के ग्रंथों में पाए गए धारणाओं के पीछे प्रक्षेपण पर एक अच्छा सौदा है।
फिर भी, बेली रिग-वैदिक दासा और दस्यु को इंडो-ईरानी बेस दास / देहा तक ट्रेस करने में काफी आश्वस्त है। प्राचीन ईरानी दाहा का अर्थ है 'आदमी', और दाहू 'भूमि' या 'देश'। लोगों के जातीय नाम के रूप में दाहा का ज़ेरक्स के एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है, और बेली ने जातीय नामों को जन्म देते हुए 'आदमी' या 'नायक' शब्दों के कई उदाहरणों का उल्लेख किया है।
दाहू शब्द, जिसे दाहा के निवास स्थान को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था, ऋग्वेद में "दस्यु" बन गया और शत्रुतापूर्ण ईरानी लोगों को संदर्भित किया गया जिन्हें बर्बर और बाहरी लोगों के रूप में माना जाता था। इससे पता चलता है कि दास और डासियस आर्यों की एक पुरानी लहर का प्रतिनिधित्व करते थे। यह माना जाता है कि ऋग-वेद V.29.10 में डासियस पर लागू अनस शब्द का अर्थ 'नासमझ' या 'फ्लैट-नोज' नहीं है, जैसा कि पहले के विद्वानों द्वारा व्याख्या की गई थी, लेकिन 'बिना मुँह के', केवल इन लोगों को प्रभावित करता है एक विदेशी भाषा बोली जाती है (जरूरी नहीं कि गैर-आर्यन), और इसलिए उन्हें इस तरह की अवमानना के रूप में वर्णित किया गया था।
यहां तक कि डासियस पर लागू एपिथेट मर्दवाचाहा उनके गैर-आर्यन चरित्र का संकेत नहीं दे सकता है, क्योंकि यह पुरुस पर भी लागू होता है, और जाहिर है इसका मतलब है 'भ्रष्ट या दुष्ट जीभ के बोलने वाले'। फिर भी, ऋग्वेद दो बार काली त्वचा (tvacam krsnam) के लोगों की बात करता है और कम से कम एक सफल छंद में यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डासियस ऊपर के रूप में हैं।
एक अन्य स्थान पर, किलों (पुराण- दारा) को नष्ट करने वाले इंद्र को कहा जाता है कि उन्होंने दासों के काले-वोमेद (कृष्णयोनि) किले को बिखेर दिया था, और दासों की काली त्वचा के संदर्भ में इसे देखना संभव है। यह सुझाव दिया जाता है कि दास और डासियस इंडो-आर्यन बोलने वालों के पूर्व-ऋग-वैदिक समूह थे और हड़प्पा संस्कृति के लोगों के संपर्क में आए थे।
एक नस्लीय और सांस्कृतिक संलयन हुआ था जो दासों के गहरे त्वचा के रंग की व्याख्या करता है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, कम से कम कुछ डूसियस ऑस्ट्रो-एसियाटिक थे। आर्य और दसा-दस्यु लोगों के बीच एक मजबूत जातीय विपरीत ऋग्वेद, V.30.9 द्वारा इंगित किया गया है, जो हमें सूचित करता है कि 'दसा ने महिलाओं को अपने हथियार बना लिया' (स्ट्रायो हाय दासा आयुधनी सकरे)।
नतीजतन, इंद्र ने टिप्पणी की, "उसकी दुर्बल (अबला) सेना (सेना) मुझे क्या कर सकती है", और हमें बताया गया है कि "इस (इन्द्र) की दो महिला स्तन की खोज की है, (इंद्र) दस्यु से लड़ने के लिए उन्नत।" यह श्लोक दासों और डासियस के प्रति पितृसत्तात्मक आर्यों की अवमानना को दर्शाता है जिनकी सेनाओं में महिला-योद्धा थे। यह एक और कविता द्वारा आगे की पुष्टि की जाती है जिसमें इंद्र दावा करते हैं कि एक लड़ाई के बिना वह अपने विपक्षी के धन को विभाजित करेगा, जो यहां लड़ने के लिए महिलाओं (स्ट्रिबिह) के साथ आए हैं।
जाहिर तौर पर दासों और डासियस महिलाओं के बीच युद्ध में भाग लिया। उनके पास कुछ निश्चित मातृसत्तात्मक लक्षण हो सकते हैं। ऋग्वेद में केवल एक महिला योद्धा का नाम है, जिसका नाम विसपाला है, जिसने "कंघों की लड़ाई" (सहस्रमिलिध) में अपना पैर खो दिया था, जिसे खेला की लड़ाई कहा जाता है। जुड़वाँ देवताओं अस्विन ने उसे अगस्त्य की प्रार्थना पर एक धातु पैर दिया, जिससे वह फिर से आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण था जिसे कई भजनों में मनाया गया। क्या हमारे यहाँ असवासियों पर उपजाए गए दसा मूल के मिथक हैं? यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि मिथक का उल्लेख केवल पहले और दसवें व्यक्ति- दलाओं में है।
हालाँकि, जो भी हो दासों और दस्युओं की जातीय पहचान, उनके और ऋग वैदिक आर्यों के बीच के अंतर स्पष्ट रूप से कम से कम प्रारंभिक चरणों में जातीय हैं और न कि सामाजिक पदानुक्रम के मामले में जिनके पास संपत्ति और गैर-अधिकारी हैं। आर्य की हत्या के साथ-साथ दशा शत्रुओं के लिए प्रार्थना और दसा के किले के संदर्भ से संकेत मिलता है कि आर्य और दसा दो अलग-अलग जातीय समूह थे न कि एक नागरिक स्तरीकृत समाज के हिस्से। यह ऋग वैदिक काल के अंत की ओर है कि दासा पूरी तरह से अधीन, गुलाम और आत्मसात कर लिया गया है और इस शब्द का अर्थ गुलाम होना शुरू हो गया है।
ऋग्वेद की पुस्तक आठवीं से तीन गुना सामाजिक भेदभाव के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पर असिविंदों को प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे ब्रह्म (प्रार्थना) को बढ़ावा दें और हमारे विचारों को जानें, राक्षसों को मारें (रक्मासी) और ड्राइव करें दूर रोग…। हमारी katra (सत्ता) शक्ति को बढ़ावा देने, हमारे नायकों (nrrn) को बढ़ावा देने, राक्षसों को मारने और बीमारी दूर ड्राइव…। हमारे दुधारू-कीन (dhenurjinvatam) को बढ़ावा देने, हमारे visah को बढ़ावा देने, राक्षसों को मारने और बीमारी दूर ड्राइव ”।
यहाँ एक त्रिपक्षीय कार्यात्मक विभाजन को एक पदानुक्रमित क्रम में उल्लेखित देखा जा सकता है। इस संदर्भ में वर्ण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद केवल दो वर्णों के जानता है, आर्य और दसा; और केन को पकड़ना सही है कि वर्ण-शब्द का अर्थ ऋग्वेद के अधिकांश अंशों में 'रंग' या 'प्रकाश' है, और "आर्य और दास दोनों को उनकी खाल के रंग के कारण वर्ना निर्दिष्ट किया गया था"। एक स्थान पर दसा वरनाम के विरोध में है, जिसका उपयोग आर्यों को स्पष्ट रूप से उनके अच्छे रंग या रंग में भ्रम के लिए किया जाता है। हालांकि, एक अन्य स्थान पर वर्णम को दशम द्वारा योग्य किया जाता है और इंद्र को कम छिपने के स्थान (दशम गुहक) में दशा वामा रखने के लिए प्रशंसा की जाती है।
डूमज़िल और बेनवेन्सिट ने तर्क दिया है कि पुजारियों, योद्धाओं और आम लोगों ने भारत-ईरानी और शुरुआती वैदिक लोगों के बीच तीन अलग-अलग सामाजिक समूहों का गठन किया और त्रिपक्षीय सामाजिक व्यवस्था भारत-यूरोपीय लोगों की विशेषता थी। हालांकि, जीएस किर्क की टिप्पणी के अनुसार, हालांकि यह विभाजन "शायद ही आश्चर्य की बात" हो, सबसे प्रमुख इंडो-यूरोपीय संस्कृति, ग्रीक, "कार्यों के त्रिपक्षीय विभाजन के लिए एक शर्मनाक अपवाद है। विभाजन केवल ग्रीक संस्कृति और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण होने के लिए किसी भी रूप में विशिष्ट रूप से कम से कम नहीं होता है ... "
दूसरी ओर, जॉन ब्रॉट ने दिखाया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में चित्रित सेमेटिक सोसाइटियों में इस तरह के तीन गुना विभाजन को देखा जा सकता है। ब्रूस लिंकन का तर्क है कि तीसरी कार्यात्मक श्रेणी को एक विशेष व्यवसाय के रूप में माना जाना बहुत सामान्य है और "सामान्य" के लिए समान है; और जहां तक पुरोहित और योद्धा वर्गों के बीच अंतर का सवाल है, यह पूर्वी अफ्रीका के देहाती नीलोटिक जनजातियों में भी पाया जाता है, पुजारियों के साथ योद्धाओं पर एक पदानुक्रमित श्रेष्ठता का आनंद लिया जाता है।
वह दावा करते हैं कि पुरोहित और योद्धा समूहों के अलगाव की जड़ें पशुपालकों के धर्म की पारिस्थितिकी में हैं और यह इंडो-आर्यन समाज के संगठन में द्विआधारी विरोधों के प्रतिमान का निर्माण करता है। हालांकि, अपर्याप्त और गलत आंकड़ों पर प्रतिमान बनाना जोखिम भरा मामला है। लिंकन ने इस आधार पर अपने सिद्धांत का निर्माण किया है कि प्राचीन भारत-ईरानियों के बीच पुरोहित और योद्धा समूहों के अलगाव को "संप्रभु भगवान", "असुरों" के रूप में, जो कि वह "दैवीय धर्म" के बीच दिव्य स्तर पर इसके प्रक्षेपण में देखा जा सकता है। स्कटसुरा = अव.हुरा-) और "योद्धा-देवता", दैवस (Skt deva = Av.daeva-Old Persian daiva)।
असुरों के रूप में वर्णित खगोलीय संप्रभु में आकाश देवता, दोहरे देवता मित्र-वरुण, आदित्य और ताम्रस्त थे। योद्धा देवताओं (देवों) में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे। अन्य थे वायु, पवन, मारुत और रुद्रों की पहचान। हालाँकि, हाल के शोधों ने स्पष्ट रूप से भारत-ईरानी काल में देवों और असुरों के तथाकथित द्वंद्ववाद पर सिद्धांतों के निर्माण की गिरावट को दर्शाया है और यह इंगित किया जाता है कि लिंकन द्वारा देवता के रूप में माने जाने वाले इंद्र को योद्धा-देवता की उत्कृष्टता के रूप में माना जाता है, asura के रूप में नामित किया गया है चार बार से कम नहीं; और ऋग्वेद के कम से कम नौ भजनों में उन्हें एक असुर के गुणों के रूप में वर्णित किया गया है।
यह वरुण के साथ तुलना नहीं करता है जो लिंकन द्वारा एक असुर, मुख्य 'आकाशीय संप्रभु' के रूप में रैंक किया गया है। उसे पांच बार से अधिक नहीं एक असुर कहा जाता है, और डेरिवेटिव आश्रम और असुर उसे दो छंदों में लागू किया जाता है। लेफ्टिनेंट कुछ भजनों में दोहरे देवत्व मित्रा-वरुण को असुर कहा जाता है या असुरसिप की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
लेकिन ऐसा ही रुद्र और मारुत के साथ हुआ, जो लिंकन की राय में दैवीय स्तर पर सांसारिक योद्धा बैंड के अनुमान हैं। देवों के देवनाम असुर, और महाद-देवमानसुरत्त्वमेकम जैसे महान "देवताओं के अद्वितीय आसनशीप" हैं, अगर देवों और असुरों ने मिथक-निर्माण के विभिन्न चक्रों से संबंधित देवताओं के विशेष समूहों का प्रतिनिधित्व किया, तो यह समझाना मुश्किल होगा।
वास्तव में, एक ऋग्वेदिक भजन में रूद्र को एक ही समय में देव और असुर दोनों कहा जाता है। यह कहना सही है कि शुरू में असुर शब्द का अर्थ केवल एक 'स्वामी', मानव या परमात्मा था, और जैसा कि मानव पर लागू होता है इंद्र के विरोधी भी, जैसे कि वरसीन, पिपरू और वृकद्वारा। इनमें से कुछ की पहचान दास के रूप में भी की जाती है। लेकिन बाद में जब इन मानव असुरों के साथ इंद्र के संघर्ष की ऐतिहासिक प्रकृति को भुला दिया गया और इसे एक पौराणिक अर्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, तो असुर शब्द ने एक अद्भुत अर्थ हासिल कर लिया और एक दानव का संकेत करना शुरू कर दिया। लोकप्रिय व्युत्पत्ति ने इसे एक नकारात्मक शब्द माना और यहां तक कि इसके सकारात्मक प्रतिरूप सुरा का भी आविष्कार किया, जिसका अर्थ है भगवान।
हेल का मत है कि भारत और ईरान में देव / दैव और असुर / अहुरा शब्द के शब्दार्थ एक दूसरे से स्वतंत्र थे। यह सुझाव आगे जांच के योग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद के वैदिक काल में पुराने ईरानी विचारों में कुछ घुसपैठ हुई थी। लेकिन हेल ने काफी हद तक आश्वस्त कर दिया है कि ऋग्वेदिक काल में असुर / देव विचित्रता का पता नहीं लगाया जा सकता है।
बेनवेनिस्ट के शोध बताते हैं कि यद्यपि प्राचीन ईरानी के साथ-साथ होमरिक भाषाएं दोनों इंडो-यूरोपीय लेक्सिकल जड़ों को आकर्षित करती हैं, ताकि परिवार, कबीले, जनजाति आदि के लिए शब्द तैयार किए जा सकें, वे समान नहीं हैं और स्वतंत्र विकास दिखाते हैं।
यह इस प्रकार है कि प्रत्येक इंडो-यूरोपीय भाषा समूह अपने विशिष्ट तरीके से सामाजिक संस्थानों को विकसित करने के लिए आया था और इंडो-यूरोपीय जड़ों पर आकर्षित करके उन्हें शब्दों के रूप में तैयार किया, लेकिन इस संबंध में कोई एकरूपता नहीं हो सकती है। एक इंडो-यूरोपियन विरासत की परिकल्पना विशिष्ट सामाजिक समूहों या सामाजिक संगठन की इकाइयों के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
ऋग्वेद पुजारियों और योद्धाओं के एक कार्यात्मक समूह के अस्तित्व का संकेत देता है और पुजारियों के एक पूर्ण विशिष्ट वर्ग में एक भ्रूण पुजारी के विकास को दर्शाता है, लेकिन, बेनिवेनिस्ट की टिप्पणी के अनुसार, यह समूह "राजनीतिक" प्रकृति या वंशावली का नहीं था। निर्धारित। सामाजिक संगठन एक अलग प्रकार के वर्गीकरण पर, परिवार, कबीले, जनजाति और देश के संकेंद्रित हलकों के तरीके से उचित विश्राम करते हैं। दूसरी ओर, सामाजिक स्तरीकरण की समस्या वैदिक लोगों के बीच एक विशिष्ट पुरोहित वर्ग के उदय के साथ जुड़ी हुई है।
यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि यद्यपि यज्ञ का अनुष्ठान इंडो-यूरोपीय काल में वापस जाता है, लेकिन पुरोहिती का कार्य किसी व्यक्ति, परिवार या वंश तक सीमित नहीं था। कई भजनों में सामान्य रूप से पुरुषों को अर्पण करने और यज्ञ करने के लिए कहा जाता है। एक स्थान पर पाँच जनजातियों या पक्का जना को अग्नि में बलिदान लाने का श्रेय दिया जाता है। यह दिलचस्प है कि 'भरत' और 'कुरु' शब्दों के बहुवचन को निघंटु में रतिविज शब्द के पर्यायवाची के रूप में दिया गया है और वैदिक संस्कृत में रतिविज का अर्थ है "उचित मौसम में या नियमित रूप से बलिदान करना।"
ऐसा लगता है कि किसी पुजारी के लिए सबसे पहला शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो बलि चढ़ाते थे। अवेस्ता में इसकी संज्ञानात्मक रथवी है और इसमें इंडो-यूरोपीय जड़ें हो सकती हैं। भरत और कौरवों का उल्लेख, संहिता से लिए गए शब्दों की पारंपरिक सूची में rtvij के पर्यायवाची के रूप में किया गया है, यह इंगित करने के लिए सही रूप से लिया गया है कि एक समय में इन जनजातियों का कोई भी सदस्य पुरोहिती कार्य कर सकता है।
श्रौतसूत्रों में से कुछ ने द्वादाशाह बलिदान की एक किस्म का उल्लेख भरत द्वादशाह के रूप में किया है। जाहिर तौर पर बलिदान का नाम भरत जन या उसके संस्थापक के नाम पर रखा गया था। हमें सूचित किया जाता है कि दवदाहा एक अतीना होने के साथ-साथ एक सत्तरा भी हो सकता है, दो प्रकार के यज्ञों के बीच का अंतर इस तथ्य में निहित है कि एक सत्त्व केवल ब्राह्मण द्वारा ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि तीन वर्णों में से एक आहिना भी कर सकता है। ।
हालांकि, दोनों में समूह की भागीदारी है। हमारी राय में यह अंतर बाद के मूल का है, जो पहले के चलन को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था के क्रिस्टलीकरण के साथ बना है, जो शायद भारतवासियों के बीच जारी रहा है। महाभारत और पुराणों में, भरत और कौर क्षत्रिय कुलों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन पहले के रिवाज के निशान देवपति और संतनु की कहानी में जीवित हैं। ऋग्वेद में देवापि को संतनु और पुरोहिता (मुख्य पुजारी) के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने देवताओं को बारिश जारी करने के लिए आमंत्रित किया था।
यास्का हमें बताता है कि देवपति संतनु का बड़ा भाई था और जंगल में तपस्या करने के लिए गया था जब उसके छोटे भाई ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस अपराध ने उन देवताओं को प्रसन्न किया जो बारिश को रोक देते थे। संतनु ने इसके बाद देवपति से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन बाद में मना कर दिया और अपने छोटे भाई की ओर से अपने पुजारी के रूप में काम करने के लिए देवताओं को प्रस्ताव दिया। कहानी को ब्राह्देवदेवता, महाभारत और कई पुराणों में दोहराया गया है, जो एक कुरु 'राजकुमार' के अपने भाई के पुजारी के रूप में अभिनय करने की असामान्य प्रथा के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार करते हैं, लेकिन बाद के स्रोतों के वंचित प्रयासों से देवपति को समझाने की कोशिश करते हैं उनके भाई के पुजारी के रूप में भूमिका इंगित करती है कि किंवदंती का वास्तविक आधार था और बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें दूर किया जाना था, जब पुजारी वंशानुगत वर्ग का विशेष कार्य बन गया था।
देवपति और संतनु का मामला अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऋग्वेद एक और मामला दर्ज करता है, जिसने किसी तरह विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार देवसराव और देवता, जिन्हें आईई मंडला के तेईसवें भजन के संगीतकार के रूप में माना जाता है और उन्हें भरत के रूप में वर्णित किया जाता है, अर्थात, भजन में भरत जन से संबंधित हैं, को भाई कहा जाता है।
जैसे देवतावों के नाम देवत्व के ऊपर दिए गए हैं, यह माना जा सकता है कि देवश्रव सबसे बड़े थे। अगला श्लोक देवश्रवाओं से अग्नि दैवत्व की स्तुति करने का आग्रह करता है, अर्थात देवताव की अग्नि, जिसे "लोगों का स्वामी" कहा जाता है, जनमानस वासी।
हमारी राय में, जनजाति की बलि की आग को आम तौर पर आदिवासी प्रमुख के नाम से पहचाना जाता था और इसलिए इस मामले में हम पाते हैं कि छोटा भाई, देवता, आदिवासी प्रमुख के रूप में काम कर रहा था, जबकि उसका बड़ा भाई उसके पुजारी के रूप में कार्य करता था। यहाँ उद्धृत छंद के अग्निम दैवत्तम की तुलना दैवदास अग्नि, दिवोदास की अग्नि के साथ कहीं और की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर दिवोदास की अग्नि को सप्तपति कहा जाता है, जो उनके बैंड का स्वामी है।
यह महत्वपूर्ण है कि दिवोदास, भी, भरत के प्रमुख थे। कई स्थानों पर भारतियों के नामचीन संस्थापक प्रमुख के नाम के बाद अग्नि को भरत कहा जाता है। पुरु रेखा के त्रसदासियु के यज्ञ की अग्नि को त्रसदासिवम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार, यह प्रमुख के नाम से कबीले की बलिदान अग्नि का वर्णन करने के लिए प्रथा थी और देवता कबीले प्रमुख थे। यह भजन उनके बड़े भाई देवश्रवा द्वारा सहायता प्रदान की गई अग्नि को नमस्कार के रूप में बोलता है, जिन्होंने उनके पुजारी के रूप में काम किया।
यद्यपि परंपरागत रूप से देवश्रव और देवता दोनों का उल्लेख ऊपर उल्लिखित भजन में किया गया है, उन्हें भाई और संगीतकार के रूप में माना जाता है, केवल दशहराव का नाम बौधायन श्रौतसूत्र में दिए गए विश्वामित्रों के परिवार की प्रवर रानियों की सूची में दिखाई देता है।
दूसरी ओर, ऋग्वेद एक योद्धा प्रमुख के रूप में, देवता के पुत्र, सृंजय की बात करता है। उन्हें अग्नि को जलाने के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्राचीन काल में देववत द्वारा संकलित किया गया था। देवत्व के पुत्र सर्जय ने वैंकिवंतों को हराया। ये संदर्भ इंगित करते हैं कि कम से कम कुछ मामलों में मुख्य-जहाज का उत्तराधिकार वंशानुगत था। बाद के वैदिक काल और बाद के वैदिक ग्रंथों में श्रीजय और कौरवों के रुझान को एक साथ क्षत्रिय वंश के रूप में उल्लिखित किया गया है। लेकिन मुख्य और पुजारी की रिश्तेदारी की पहले की एकता भजन में परिलक्षित होती है, जो भरत के प्रसिद्ध पुजारी भरत के पुत्रों के रूप में, विश्वामित्र के वंशजों का वर्णन करता है। एक और वैदिक द्रष्टा परुछेपा, जो पहले मंडल के कई भजनों के लेखक हैं, खुद को भारत के प्रमुख दिवोदास के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं।
इस प्रकार ऐसा लगता है कि कम से कम भरतों में पुजारी और प्रमुख शुरू में एक ही गोत्र के थे। हमारी राय में यह पुराण मिथक की जड़ में निहित है कि विश्वामित्र क्षत्रिय राजकुमार पैदा हुए थे, लेकिन गंभीर तपस्या करके ब्राह्मण ऋषि बन गए। यह तर्क दिया जा सकता है कि हालांकि यज्ञ अनुष्ठान में कुछ दूरस्थ अवधि में भागीदारी एक समतावादी सांप्रदायिक गतिविधि हो सकती है, जैसा कि सत्तरा / अहिना बलिदानों द्वारा सुझाया गया है, देवपती-संतनु और देवश्रव-देवता के उदाहरण बताते हैं कि पुजारी और कार्यालय प्रमुख कुछ विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों में रहते हैं, जिन्होंने उच्च स्थिति का आनंद लिया हो सकता है, जैसा कि कई आदिवासी समाजों के मामले में है। वास्तव में ऋग्वेद एपिटेट सुजाता का अर्थ born अच्छी तरह से जन्मे ’पुरुषों पर चार बार लागू होता है, जिन्हें विभिन्न प्रकार से सुरि नर और वारस कहा जाता है और उन्हें एक साथ बैठने और यज्ञ अग्नि को प्रवृत्त करने के रूप में वर्णित किया जाता है।
हालाँकि, हमारे विचार में इन मार्गों में सुजाता शब्द को 'उच्च जन्म' या 'श्रेष्ठ वंश' के अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि ग्रिफ़िथ ने किया है, लेकिन एक भौतिक अर्थ में 'अच्छी तरह से निर्मित', 'सुंदर', 'अच्छी तरह से विकसित', 'लंबा', आदि, इस प्रकार, यह पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र के लिए कहा जाता है कि "जल से एक मजबूत, युवा (सुजाता) नायक (नारु) पैदा हो, अग्नि को कई संख्या में कहा जाता है समय, और एक स्थान पर वह स्पष्ट रूप से 'सुवर्ण' (तन्वा सुजाता) के रूप में वर्णित है।
एक अन्य स्थान पर another शुद्ध वाले ’(सुकाहा), जाहिरा तौर पर मारुतस, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि की पूजा करके अपने शरीर को अच्छी तरह से विकसित (तनवा सुजाता) बनाया था, इस प्रकार अमर लोगों के लिए अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अग्नि और मारुत के अलावा, कई अन्य देवता भी, जैसे मित्रा। वरुण, आर्यमान। भगा और इंद्र को सुजाता कहा जाता है और इसलिए देवी अदिति, रोदासी और उस्सा हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कवियों ने इन देवताओं की अच्छी तरह से बनाई गई शारीरिक उपस्थिति को ध्यान में रखा था, न कि उनके 'कुलीन वंश'।
ऋग वैदिक भजनों में क्षत्रिय और क्षत्रिय के संदर्भ में अक्सर एक 'योद्धा अभिजात वर्ग' या 'बड़प्पन' के वैचारिककरण के कारण प्रोटो-इंडो-यूरोपियन समय में वापस आ गया है। फिर भी, यह सही तरीके से आयोजित किया जाता है, अर्थात, यह पाठ ksatra 'शासक' या 'शासक' या प्राधिकरण, मानव या परमात्मा के लिए 'वीरता' और 'क्षत्रिय' के लिए खड़ा है।
यह लगभग राजन का पर्याय है, लेकिन व्यक्ति के उन गुणों पर जोर देता है, जो केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि अपने कबीले के अन्य सदस्यों के साथ लड़ने वाले उच्च पद के व्यक्ति थे। साधारण सेनानियों को बलम यानी बल के रूप में नामित किया जाता है। ऋग्वेद में एक कॉम्पैक्ट समूह, वर्ग या जाति को निरूपित करने के लिए 'क्षत्रिय' का कोई सबूत नहीं है।
यह महत्वपूर्ण है कि जब वर्ण / जाति संरचना उभरती है तो शुरू में यह anya राजन्य ’होता है, जो कि राजन के साथ रिश्तेदारी संबंध पर जोर देता है, न कि s क्षत्रिय’ के रूप में, जो दूसरे वर्ण को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ण योजना में K क्षत्रिय ’के साथ राजयोग का प्रतिस्थापन एक क्षैतिज और शायद यह भी है कि अंतरिक्ष और लोगों दोनों के मामले में शोषक सामाजिक व्यवस्था का ऊर्ध्वाधर विस्तार है और वर्तमान अध्ययन के दायरे से परे है।
यह माना जाता है कि ऋग्वेदिक राजान एक आदिवासी प्रमुख था, जिसका कार्य काफी हद तक अपने कबीले और उसके मवेशियों को संरक्षण देने और युद्धों और मवेशियों के छापे में नेतृत्व तक सीमित था। उन्होंने मवेशी छापे की लूट या लूट को भी वितरित किया, जाहिर तौर पर खुद के लिए एक बड़ा हिस्सा बनाए रखा। ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति थी, यह मघवन शब्द से संकेत मिलता है।
सूरी भेद का एक और शब्द था और अक्सर मुख्य के अर्थ में व्याख्या की जाती है। हालांकि, पोद्दार बताते हैं कि प्रार्थना में जब लंबे जीवन की उम्मीद की जाती है, तब सूरी शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब भोजन या धन की प्रार्थना की जाती है तो मघवन का उपयोग किया जाता है। दोनों पुजारियों के संरक्षक के रूप में हैं। कई श्लोकों में असुर शब्द, ऋग वैदिक राज के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
असुरशिप और क्षत्रप कुछ मामलों में एक साथ प्राप्त होते हैं, और एक भजन में लोगों के असुर को "वितरक" के रूप में भी वर्णित किया जाता है। असुर के अपने स्वयं के वर (असुर विराट) हैं। हेल के निष्कर्ष ध्यान देने योग्य हैं। ऋग्वेद के पहले के भागों में उनके विचार में एक असुर जन्म से या किसी के स्वभाव से नहीं बल्कि एक असुर के रूप में "उनके अनुसरण करने वालों की सहमति और समर्थन" से बन गया था। वह अपने कमांड में कुछ प्रकार के सैन्य बल के साथ एक प्रमुख या "भगवान" था।
जबकि असुर, मघवन, सूरी और रजन शब्द उच्च पद को इंगित करने वाले शब्द हैं, सामान्य रूप से योद्धाओं को नर या विरस / सुवीर कहा जाता है, जिसका अर्थ शक्तिशाली पुरुष या नायक होता है। जाहिर तौर पर युद्ध मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक आर्य जनजातियों के युवकों की चिंता थी। लिंकन योद्धा बैंड, मेरी और व्रका को इंगित करने वाले दो दिलचस्प शब्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्राचीन ईरानी यासन में उनके पत्राचार हैं।
शाब्दिक रूप से, पूर्व का अर्थ 'युवा पुरुष' और बाद का 'भेड़िया' था। यह विशेष रूप से पशु-छापे के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, क्योंकि योद्धा को एक क्रूर शिकारी होना चाहिए था। योद्धा बैंड की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं जैसे गदा (वज्र) और बैनर (ध्वाजा या ड्रेप्स)।
लिंकन ने यह भी सुझाव दिया कि योद्धा को किसी प्रकार की दीक्षा से गुजरना पड़ा। बहरहाल, वह स्वीकार करते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये बैंड "आयु-सेट, गुप्त समाजों के साथ, या पूरी तरह से अलग-अलग लाइनों" के रूप में आयोजित किए गए थे, हालांकि यह तथ्य कि मारुत एक ही उम्र के संगठन के लिए इंगित करेंगे ।
युवाओं पर जोर देने से उनकी भर्ती खुली होगी और कुछ तथाकथित राजभाषाओं तक सीमित नहीं होगी, विशेष रूप से जनसांख्यिकी के रूप में यह अभी भी एक छोटे पैमाने पर समाज था जो अपनी जनशक्ति की वृद्धि के लिए हमेशा के लिए प्रार्थना कर रहा था।
रिग वैदिक डेटा द्वारा बनाई गई समग्र धारणा यह है कि रैंक को बंद नहीं किया गया था और कोई भी एक पुजारी या एक युद्ध प्रमुख बनने की आकांक्षा कर सकता था। अक्सर उद्धृत कविता में कवि कहता है: "ए बार्ड एम आई, माई डैड (तातह) एक जोंक है, मम्मी {नाना] पत्थरों पर मक्का लगाती है। धन के लिए प्रयास, विभिन्न योजनाओं के साथ, हम परिजनों की तरह हमारी इच्छाओं का पालन करते हैं।
पहले के मंडला में एक कवि इंद्र को संबोधित करता है: “क्या तुम मुझे (जनादेश), उनके शासक (राजानम), हे मघवन पर विजय प्राप्त करोगे? या आप मुझे सोम का रस पिलाते हुए एक आरसीआई बना लेंगे? या आप मुझे चिरस्थायी धन देंगे ”?
इस तरह के सामान्य कथन हमें ऋग वैदिक जनजातियों की संगठनात्मक संरचना के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन सामाजिक पारिस्थितिकों के बीच कठोर सीमांकन की कमी बताती है कि यद्यपि सामाजिक संगठन विशुद्ध रूप से समतावादी स्तर से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। विरासत के बजाय रैंक अभी भी काफी हद तक उपलब्धि का विषय थे।
प्रश्न उठता है: वह कौन सी प्रक्रिया थी जिसने स्थितियों को सटीक रूप से परिभाषित करने और संस्थागत रूप देने के लिए, वर्ना श्रेणियों में उनका क्रिस्टलीकरण किया? डीडी कोसंबी का विचार था कि ब्राम्हण वर्ण अपने गोत्र संगठन के साथ "आर्यन पुरोहितवाद और सिंधु संस्कृति के श्रेष्ठतम पुरोहितवाद के बीच बातचीत का एक परिणाम" के रूप में विकसित हुआ।
हड़प्पा संस्कृति के बचे हुए लोग समग्र आर्य समाज में विभिन्न स्तरों पर समाहित थे, जिसके परिणामस्वरूप चार गुना वर्ना संरचना विकसित हुई। सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा के पुजारी की अस्मिता थी। पूर्व-आर्यन पुजारियों के छोटे समूह आर्यन पितृसत्तात्मक कबीले समूहों को जीतने में शामिल हो गए, जो उन्हें अपनी पुरोहिती सेवा प्रदान कर रहे थे।
इसके परिणामस्वरूप इन पुरोहित समूहों ने अपने संरक्षक के रूप में उसी कबीले के नाम को अपनाया, जो वास्तव में वैदिक कबीले के नाम (उदाहरण के लिए, विकर्ण, मत्स्य, कुत्सा, विथवैया, आदि) के ब्राह्मणवादी गोत्रों में सूचीबद्ध हैं। श्रौतसूत्र और मत्स्य पुराण।
पुनर्संबंधित पुरोहितवाद ने मूल वैदिक पुरोहितत्व को क्षत्रिय कुलीन वर्ग से अलग करने के लिए बदल दिया, एक संरचनात्मक विकास जो दासा / सुद्रा जाति के उद्भव के समानांतर था और जिसके कारण अंतःसम्प्रदाय हुआ। खानाबदोश देहाती आर्यों के बीच व्यक्तिगत संपत्ति पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई थी।
इसलिए, कोसंबी के अधीनस्थ हड़प्पा कृषि आबादी की पहचान दासों के रूप में की जाती है, इसलिए वे अपने से अलग समूह बनाते हुए विजयी जनजातियों के थे। यह एक दास / सुद्र वर्ण और एक जातिगत जाति व्यवस्था का मूल था।
कोसंबी की थीसिस शानदार और प्रेरक है और यद्यपि उनकी कुछ दलीलें दूर की कौड़ी लगती हैं, घोरी के विपरीत वह ब्राह्मणवादी गोत्रों की उत्पत्ति का तर्कसंगत विवरण देने की कोशिश करते हैं। थापर ने कोसंबी को एक 'वंश समाज' के अपने मॉडल को चित्रित करने के लिए अपनी ऋणीता स्वीकार की जिसमें ब्राह्मण और शूद्र को एडेंडा माना जाता है; लेकिन वह अपनी थीसिस के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज करती है, जो कि दासों / सुदास वर्ण, 'अधिशेष उत्पादक श्रम', और आर्यन के आत्मसात और पूर्व के गठन के परिणामस्वरूप आर्य जनजातियों के आंतरिक स्तरीकरण की व्याख्या करता है। आर्य पुरोहितवाद ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलगाव के परिणामस्वरूप था, एक सामाजिक पैटर्न जो बाद के वैदिक चरण के यजुर्वेद के भजनों में परिलक्षित होता था न कि ऋग्वेद (पुरुसूक्त के अपवाद के साथ) में।
कुछ हड़प्पा तत्वों के जीवित रहने और आर्य समाज के विस्तार में उनके आत्मसात होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन कोसंबी की यह धारणा कि "आर्य विजेता के पुजारी वर्ग को बड़े पैमाने पर विजय प्राप्त की गई थी" अत्यधिक अतिरंजित प्रतीत होता है।
कुछ वैदिक ऋषियों जैसे कावासा, ऐलूसा और दुर्घाटमास के बारे में कहा जाता है कि ये दशपुत्र, दासा महिलाओं के पुत्र हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों के साथ दासों की पहचान कायम है, और कोसंबी का दृष्टिकोण सात ऋषियों में से माना जाता है ब्राह्मणवादी गोत्र-वंश के प्राथमिक संस्थापक, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, आरती, वसिष्ठ और कश्यप, विश्वामित्र "एक वास्तविक भोगवादी आर्यन" थे, और बाकी गैर-आर्यन थे - अत्यधिक सट्टा है। एक को नहीं पता कि जमदग्नि के पिता भृग को गोत्र सूचियों में एक द्वितीय स्थान दिया जाता है, लेकिन ऐसा ही विश्वामित्र के पिता कुसिका के साथ हुआ।
हालाँकि, ऐसा लगता है कि कोसंबी के पास भृगु-जमदग्नि के गैर-आर्यन के संबंध में एकमात्र कारण यह है कि 'दस राजाओं' की लड़ाई में भृगु, त्रस के नेता सुदास के शत्रु के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे इंद्र, "मित्र" आर्यन की मदद करता है।
लेकिन इंद्र की शत्रुता एक गैर-आर्यन पहचान का एक निश्चित संकेत नहीं है, क्योंकि कई स्थानों पर इंद्र को आर्य दुश्मनों को मारने के लिए प्रशंसा की जाती है। बेशक, कोसंबी भृगु के संबंध में ऋग्वेद में 'एक पूर्ण जनजाति' के रूप में सही है, जिसमें युद्ध, रथ निर्माण और मिट्टी के बर्तनों सहित गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला है, शब्द भार्गव के लिए अंतिम उल्लेख किए गए पेशे में विशेषज्ञता, जिसका अर्थ है संस्कृत और पाली दोनों में कुम्हार। यह स्पष्ट है कि भृगु की इस बहु-आयामीता के कारण, मैकडोनेल और कीथ यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें पुजारियों या योद्धाओं के रूप में माना जाए या नहीं।
परंपरागत रूप से, अंगिरस भृगु के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक गोत्रकार, भारद्वाज और गौतम में से दो, गोट्रा सूचियों में अंगिरिस के रूप में हैं, और वामदेव, जिन्हें चतुर्थ मंडल के लेखक के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया है, गोतम के पिता के रूप में बोलते हैं। कई भजनों में, अंगिरिस को रहस्यमय रूप से विरुपस (भगवान के विभिन्न रूपों और देवपुत्र देव पुत्रों के रूप में) के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन एक भजन में वे विश्वामित्र के संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन को लंबे समय तक समृद्ध उपहार देकर समृद्ध किया। हजार गुना सोमा दबाव, अर्थात्, घोड़े का बलिदान। निम्नलिखित श्लोक यह स्पष्ट करते हैं कि यह सुदास का घोड़ा बलिदान था, जो भरत के प्रमुख थे, जिस पर कुसिकों ने अधिकार किया। विश्वमित्र ने इंद्र की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भरत जन।
इस प्रकार, कम से कम इस भजन में अंगरेजों को भरत के साथ निकटता से जोड़ा जाता है, अगर उनके साथ पहचान नहीं की जाती है, और उन्हें विश्वामित्र पर धन देने वाले संरक्षक के रूप में उल्लेख किया जाता है, न कि पुजारी के रूप में। उनके गैर-आर्यन मूल का संकेत शायद ही कुछ हो।
कोसंबी ने सातवीं मंडली में उल्लेखित वसिष्ठ के चमत्कारी जन्म के मिथक को आर्य वंश में अपनाए जाने के एक निश्चित संकेत के रूप में माना है और उनका तर्क है कि वसिष्ठ को गोद लिया गया था, न कि कृतिका गोत्र में "मूल आदिवासी पुजारी का गेंस" विश्वामित्र ”, लेकिन ऋग्वेदिक संस्करण के रूप में तृत्सु-भरत जनजाति में पता चलता है कि“ ब्राह्मणवाद मूल आर्यन प्रणाली के लिए विदेशी था ”, हालांकि विश्वामित्र के लिए, एक पुजारी, पहला ब्राह्मण नहीं था।
उन्हें एक क्षत्रिय माना जाता है जिन्होंने बाद की किंवदंतियों के अनुसार घोर तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, जो वशिष्ठ के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता की बात करते हैं। यह वशिष्ठ है जिसे प्रथम ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ कोसंबी का अर्थ है कि एक अलग ब्राह्मण वामा का बहुत विचार हड़प्पा संस्कृति से लिया गया था।
यह उनके अपने विचार के विरुद्ध है कि वर्ना / जाति संगठन की शुरुआत के उत्पादन और दासा / सुद्रा वर्ना के एक सहायक वर्ग के गठन के संबंधों में परिवर्तन का पता लगाया जाना है। "दसा" वास्तव में ऋग्वैदिक आर्यों के हाथों दासों की हार के बाद एक दास श्रेणी बन गई। यह उत्पादन संबंधों के पहले के नेटवर्क में उनकी पहले से मौजूद स्थिति की निरंतरता नहीं थी।
ऋग्वेद में कई दसा प्रमुखों के बारे में पता है, जिनकी संपत्ति आर्यों द्वारा प्रतिष्ठित थी। इसके अलावा, यहां तक कि अगर यह अनुमति दी जाती है कि वसिष्ठ भरत द्वारा संरक्षित एक पूर्व-आर्यन पुजारी थे, तो यह एंडोगैमी की गूढ़ विशेषता को नहीं समझाएगा जो कोसंबी इस परिकल्पना के साथ करने की कोशिश करता है; विश्वामित्रों और वाशिष्ठों के लिए, कोसंबी की थीसिस के तथाकथित आर्यन और पूर्व-आर्यन पुजारियों ने, एक विलक्षण जाति की इकाई बनाने के लिए आत्मसात किया और इसके भीतर विलुप्त हो चुके गोत्र या वंश थे।
ब्राह्मणों की गणतन्त्र प्रणाली में विश्वामित्रों का एक बहुत बड़ा स्थान है और एंडोगैमी उन्हें वसिष्ठों से चिह्नित नहीं करता है; वे एक साथ एक पूरे पूरे एक गठन के रूप में दूसरे व्यावसायिक समूहों से अलग हो जाते हैं, जो अलग-अलग वर्णों और अंतःसक्रिय इकाइयों में क्रिस्टलीकृत होते हैं।
यह तर्क करना संभव है कि वशिष्ठ का 'प्रथम ब्राह्मण' के रूप में वर्णन उनके सबसे महत्वपूर्ण होने के अर्थ में है, या वैकल्पिक रूप से यह ब्राह्मण पुरोहित के रूप में नामित ब्राह्मण पुरोहितों में से पहला है और बस उल्लेख किया गया है ऋग्वेद 1.15.5 में 'ब्राह्मण' के रूप में, क्योंकि उन्हें सोम पीने के लिए ब्राह्मण नामक विशेष कप आवंटित किया गया था।
ब्राह्मण वामा के ढांचे के भीतर आदिवासी पुजारियों का आत्मसात और आवास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जाति व्यवस्था के विस्तार की अवधि के दौरान हुई है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण के भीतर एंडोगामस उप-जाति का उदय एक उत्तर-वैदिक घटना है और संभवतः प्रारंभिक मध्ययुगीन।
जातीय प्रतिकर्षण या अलगाव वैदिक काल में एक अंतिम ब्राह्मण वर्ण के उद्भव की व्याख्या नहीं करता है। यदि पुरोहिती के स्तर पर आर्यन और पूर्व-आर्यन की अस्मिता थी, तो इस बात को रखने के लिए मजबूत आधार थे कि सत्तारूढ़ वंशावली के स्तर पर, अस्मिता थी और सुदास भी; लेकिन यह वर्ण प्रणाली और एंडोगैमी की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करेगा।
हमारी राय में एंडोगैमी को वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हमारी राय में एंडोगैमी को वर्ग और लिंग शोषण के चरम प्रकटीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए जो जाति व्यवस्था में एक साथ चलते हैं। इस प्रणाली ने अपने स्वयं के अंत की सेवा करने के लिए कुछ व्यापक धर्म-सामाजिक धारणाओं को अपनाया है।
हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व के रूप में वैदिक और पश्चात वैदिक काल के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की विशिष्ट वस्तुओं की पहचान करना एक खतरनाक कवायद है। स्टुअर्ट पिगॉट की टिप्पणी को ध्यान में रखना सार्थक है, "इतिहासकारों के लिए उपलब्ध सामग्री के सामान्य रन की तुलना में प्रागितिहास के अवलोकन डेटा मुझे लगभग हर तरह से अधिक अस्पष्ट और अधिक व्याख्या करने में सक्षम हैं"। हड़प्पा के सामाजिक-राजनीतिक संगठन के बारे में सिद्धांत अक्सर विरोधाभासी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए समान कलाकृतियों का उपयोग करते हैं।
उनके धर्म के अनुसार, कोसंबी के पास कालीबंगन (राजस- की तुलना में) और लोथल (गुजरात) की उत्खनन रिपोर्टों का लाभ नहीं था, जो हड़प्पा के सांस्कृतिक परिवेश में अग्नि-वेदियों के अस्तित्व और अग्नि-संस्कार को सामने लाती हैं। लेकिन यह उचित है कि मोहनजो-दारो, हड़प्पा या चान्हू-दारो जैसे हड़प्पा संस्कृति के उत्तर-पश्चिमी स्थलों में से कोई भी आग-पंथ का कोई संकेत नहीं देता है।
हड़प्पा लोगों से मिलने वाले कुछ दखल देने वाले इंडो-ईरानी या आर्य तत्वों के संदर्भ में क्षेत्रीय विचलन की व्याख्या की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक सांस्कृतिक संश्लेषण हुआ, लेकिन यह दलील देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हड़प्पा के पुजारी आर्यन अग्नि-अनुष्ठान का जिम्मा लेते थे। और ऋग्वेदिक आर्यों के सामाजिक और धार्मिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मार्शल की परिकल्पना है कि हड़प्पावासी महिला-सिद्धांत-शक्ति की पूजा करते हैं, एक मातृ-देवी के रूप में, साथ ही पुरुष-सिद्धांत, भगवान शिव के प्रोटोटाइप, दोनों ने अपने मानवशास्त्रीय और साथ ही अराजक रूपों में व्यापक रूप से स्वीकार किया है। किसी भी महत्वपूर्ण मूल्यांकन के बिना, और विस्तृत सिद्धांत इस धारणा पर बनाए गए हैं कि हड़प्पा धर्म हिंदू धर्म का प्रत्यक्ष पूर्वज था।
इस प्रकार, व्हीलर ने डेटा की मार्शल की व्याख्या को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए, यह अनुमान लगाया कि मातृ-देवी का पंथ निम्न वर्गों द्वारा देखा गया था और उच्चतर वर्गों ने पुरुष-देवता की पूजा की थी, जो कि 'प्रोटो-शिवा' मुहरों पर दर्शाया गया था। यह दिलचस्प है कि 'प्रोटो-सिवा' पहचान के लिए मामला मुख्य रूप से मार्शल द्वारा मोहनजो-दारो में पाए गए एक सील की व्याख्या पर टिकी हुई है।
मैके द्वारा खोजे गए दो अन्य मुहरों और उनके द्वारा 'प्रोटो-शिव' सील के समान माना जाता है जो महत्वपूर्ण बदलाव दिखाते हैं। मोहनजो-दारो सील पर आकृति एक भैंस-सींग का हेडड्रेस पहनती है, कई कंगन और, मार्शल के अनुसार, इसके तीन चेहरे हैं और इथिपैलिक है; लेकिन ये विशेषताएं अन्य दो मुहरों पर अनुपस्थित हैं।
विभिन्न पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के विचारों का उल्लेख करते हुए, घुरे ने दिखाया कि मोहनजो-दारो मुहर के संबंध में भी अंतिम दो विशेषताओं के बारे में एकमत नहीं है; और वह निष्कर्ष निकालता है कि न केवल "तथाकथित ithyphallism of the आंकड़ा लगभग एक कल्पना या कल्पना का एक कार्य है", लेकिन आंकड़े के तीन चेहरों का प्रतिलेखन भी, बहुत ही अनुचित है।
वह इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित करता है कि जबकि ऐतिहासिक शिव बैल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, यह जानवर सील पर देवता के आसपास के जानवरों के बीच स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इस प्रकार शिव-पंथ के हड़प्पा मूल की थीसिस को खारिज करने में घोरी काफी न्यायसंगत है।
एक दशक से भी अधिक समय पहले, एचपी सुलिवन ने भी, हड़प्पा के लोगों के धर्म के बारे में मार्शल की पहचान और मान्यताओं पर सवाल उठाया था। वह काफी जोरदार है कि मोहनजो-दारो सील पर आंकड़ा न तो ithyphallic है और न ही तीन-प्रमुख है; यह वास्तव में एक मादा देवता है, वनस्पतियों और उर्वरता की एक ही महान देवी है जो पवित्र वृक्ष में खुद को प्रकट करती है और तीन-बिंदुओं वाली हेडड्रेस पहने हुए दिखाई देती है।
वह बताते हैं कि मार्शल ने खुद स्वीकार किया था कि एक इरेक्ट फालूस को जो दिखाई दिया, वह वास्तव में कमरबंद का अंत हो सकता है। सुलिवन के दृश्य में कमरबंद और कमरबंद केवल महिला मूर्तियों और हाथ की चूड़ियों और हार पर पाए जाते हैं, जो हड़प्पा कला में महिला आकृतियों पर आकर्षक रूप से सुशोभित हैं। उनके अनुसार, दो अन्य तथाकथित 'प्रोटो-शिवा' द्वारा पहने गए कॉइफ और पिगलेट महिला मूर्तियों द्वारा पहने गए हैं और हड़प्पा संस्कृति में पुरुष देवता की पूजा का कोई सबूत नहीं है।
सिंधु स्थल पर फाल्स या लिंगो के रूप में पाए गए कई शंक्वाकार पत्थरों की पहचान भी संदिग्ध है और यह सही रूप से आयोजित किया गया है कि भले ही 'फालूस पूजा' को हड़प्पा धर्म का एक हिस्सा माना गया हो, यह प्रचलन नहीं साबित होगा शिव की पूजा, लिंगो के साथ शिव के संबंध के लिए, प्रतीक वैदिक के बाद का है और शायद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की तुलना में
इस प्रकार, सुलिवन और घोरी की दलीलें पर्याप्त रूप से संदिग्ध आयात की कुछ सामग्री कलाकृतियों के आधार पर धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के क्षेत्र में व्यापक सामान्यीकरण की गिरावट को प्रदर्शित करती हैं। जो लोग शिव और शक्ति के महाकाव्य-पुराणिक पंथों के साथ-साथ हड़प्पा संस्कृति की जाति व्यवस्था का पता लगाते हैं, वे इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि इन दोनों देवताओं के दोष मूल रूप से ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के प्रति शत्रुता रखते थे।
शिव और माँ देवी दुर्गा-शक्ति दोनों ब्राह्मणवादी पैंठ में देर से प्रवेश करते हैं। दक्ष-प्रजापति के यज्ञ के बलिदान और देवताओं के बीच उनके गैर-समावेश के शिव के विनाश की कहानी जो स्पष्ट रूप से यज्ञ के एक हिस्से को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण-विरोधी एंटीकाइड को स्थापित करते हैं।
इसी तरह भारतीय गांवों में देवी देवताओं की पूजा ब्राह्मणवादी वर्ण-व्यवस्था से मुक्त होने के बाद इसकी पुरानी परंपरा के निशान को बनाए रखती है। इस प्रकार, यह बनाए रखना मुश्किल है कि इन ब्राह्मणवादी पंथों की जड़ें और वर्ण व्यवस्था सिंधु सभ्यता में वापस चली जाती है, जिसे ब्राह्मण पुजारियों ने धर्म और अनुष्ठान के माध्यम से जोड़ दिया था। हड़प्पा संस्कृति से काल्पनिक उत्तरजीविता को पोस्ट करके इस तरह से प्रश्नों को भीख माँगने के बजाय, ऋग्वेदिक समाज की आंतरिक गतिकी में स्पष्टीकरण की तलाश करना अधिक उपयोगी होगा।
एक शक्तिशाली पुरोहितवाद के विकास और ब्राह्मण वर्ण के गठन को केवल जातीय पूर्वाग्रह के मामले के रूप में नहीं समझाया जा सकता है; अधिशेष और लागू अवकाश की अधिक उपलब्धता अनुष्ठान के प्रसार और विशेषज्ञों के एक वर्ग की वृद्धि के लिए आवश्यक शर्तें हैं जो पहले महान प्रजनन संस्कार पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और फिर कुलों और पूर्वजों और देवताओं के बीच मध्यस्थों की भूमिका ग्रहण करते हैं।
इस प्रक्रिया को ऋग्वेद में देखा जा सकता है। आम तौर पर यह माना जाता है कि एक पुरोहिती कार्य को निरूपित करने के लिए सबसे प्रारंभिक शब्द rtvij और hotr हैं, दोनों को अवेस्ता में रथवी और ज़ोतार के रूप में जाना जाता है। पूर्व का कार्यकाल नियमित अंतराल पर दी जाने वाली मौसमी कुर्बानियों से जुड़ा होता है और हम पहले ही दिखा चुके हैं कि शुरू में रतिविज का कार्य किसी पुरोहित वंश तक सीमित नहीं था। ये बलिदान शायद सामूहिक रूप से आदिवासियों द्वारा किए गए थे; इसलिए भरत जनजाति को rtvij के रूप में जाना जा सकता है।
बाद में, rtvij एक बलिदान में पुजारी की सामान्य पदनाम बन गया। होटर के मामले में समान विकास देखा जा सकता है। यह एक इंडो-यूरपोनियन रूट हू से आशय है जिसका अर्थ है 'डालना'। इस प्रकार हॉट्र का मूल कार्य आग में परिवाद डालना था। It also denoted one who invoked the gods by reciting the hymns and is regarded by some as the earliest priest.
In ancient Iran, Zaotar was the designation of a class of priests. However, originally hotr does not seem to have belonged to a distinct priestly class but was identical with yajamana the sacrificer, and this position he retains in the paka yajnas of the grhya ritual. Later, with the growth of a more complicated sacrificial ritual, hotr becomes one of the four rtvijs having three priest assistants or helpers. In some hymns of the Rig-Veda, the hota and the yajamana are clearly distinguished and at two places he is one of the seven priests named along with Brahman.
It is interesting that priestly specialization is related not to the monopoly of or greater expertise in worshipping certain deities or to officiating for certain specific clans or people but to certain ritual matters such as the use of specific vessels for offering the soma drink to various divinities. This seems to suggest that elaboration of ritual, rather than assimilation of different ethnic groups, resulted in the development of a class of specialists which later crystallized as the Brahmana varna. The earlier terms used for the priests such as stotr, jaritr, vipra, kavi, rsi and Brahman in the masculine are connected with the function of composing or singing of the hymns or prayers.
The term 'Brahmana' is of rare occurrence in the Rig-Veda and with the exception of the Purusasukta hymn it does not seem to have been used anywhere else to denote a member of the priestly class. At least at two places it means the cup allotted to the Brahmati priest for drinking soma. At several other places it is used as an adjective. Similar is the case of vipra, a term which later came to mean exclusively a member of the Brahmana varna but is often used as an adjective in the Rig-Veda signifying a state of exhilarated ecstasy or inspired eloquence. At one place the term seems to stand for Brhaspati and at another place the vipras and adhvaryus are clearly distinguished.
A semantic study of the four key words, vipra, rsi, purohita and brahman comes to the conclusion that a professional class of priests evolved gradually in the Rig Vedic period “from functional notions of sacerdocy” and only towards the end of this period it became a closed order known as the brahmana varna.
Beginnings of this process may be seen in the hymns which clearly distinguish between the singers (stotr) and the bounteous patrons (maghavans or suris) and thank the gods for bringing food (anadu) to both. The vipras create hymns and are contrasted with the naras or viras who go to the battlefield and fight hand to hand while their chief rides on a horse or, as is more likely, a chariot.
So the occupational category of the composer-chanter-priest is well-marked. In a hymn of the VIII mandala the vipras claim to be 'kinless' (ahandhavah) and pray to God Indra who has 'numerous kin' (bandhumantam) to protect them. The statement appears significant and may show that the priestly functionaries were the first to renounce or transcend kinship ties in a society organized on kin-principle.
Their activities were not confined to one clan or tribe and in a verse of the IX mandala the seven priests are described as “united in consanguineous brotherhood”. Another verse of the X mandala clearly distinguishes between the vipra and the yajamana.
Thus, in the latest stratum of the Rig-Veda, the priesthood may be said to have acquired the characteristics of a separate order claiming the highest position in society by virtue of its control over ritual. It is argued that the term brahmana was preferred to other terms to indicate the generality of priesthood, for its etymon Brahman was more comprehensive and covered every type of priestly activity. Its use also emphasized the factor of heredity, so that whereas Brahman was one of the seven priests, Brahmana was an inherited status.
The transitional character of the Rig Vedic society may be noticed also in the changing pattern of family system. In our opinion the Rig Vedic family, as reflected in the earlier stratum of the text, was nuclear or 'elementary' consisting of not more than two generations; and it was closely embedded in a wider grouping of 'clan'.
The authors of the Vedic Index express the view that the Rig Vedic evidence does not show whether a son grows up to set up his own house or continued to stay with his father, his wife becoming a member of the father's household; perhaps the custom varied. But allusions to a joint family system occur in the interpolated or latest stratum of the Rig-Veda and we are not wrong in advancing a rather uncommon view that the joint family system emerges only towards the close of the Rig Vedic phase.
Although the Rig Vedic society is clearly patrilineal, there is hardly any evidence of 'patriarchal' authority or control exercised by the father or the head of the family. The story of Sunahsepa is found in later Vedic texts. The Rig-Veda does not mention it and it seems to have been a later invention. The blinding of Rjrasva by his father mentioned in two hymns is sometimes cited to prove a developed patria potestas but Mac- donell and Keith are quite right in warning that “to lay stress on this semi-mythical incident would be unwise”.
On the other hand, they point out that there is nothing to show that a father controlled the marriage of his son or daughter. “… any excessive estimate of the father's powers over a son who was no longer minor and naturally under his control must be qualified by the fact that in his old age the sons might divide their father's property.In support they refer to a verse addressed to God Agni: “Parting you, men have served you in many places as are the goods of an aged father (parted)”. In our opinion, this verse alludes not merely to the division of an aged father's possessions among his sons, but also indirectly to their separate households.
References to individual couples (mithuna dampati) washing and pressing the soma juice, offering oblations together and tending the fire in their house (dama) are numerous in the Rig-Veda. At one place Agni is called common to all, the protector of the vis and of dampatis.
Another hymn speaks of the equal age (savayasa) of their (mithuna) dwelling in the same place tending the sacrificial fire night and Benveniste has shown that the Indo-European roots dem and vis from which early Vedic dampati and vispati are derived were initially genealogical terms, which later assumed the meaning of physical habitat. Thus dama would mean family and dampati the master of the house qua family. In our view this was the smallest social unit, an elementary family.
Another crucial word having the sense of family or household is grha. In many Rig Vedic passages it is clearly the material abode or place of residence. The gods are described as going to the grha of the benefactor. Elsewhere, Agni is said to be in every dama (house).
However, at one place grha, too, appears to be a consanguineous unit. The usage of grhini (housewife) and grhastha (householder) continues to this day in Hindi. The terms grhapati and grhapatni have been translated as the head and the mistress of the household. RS Sharma is of the view that grha in the Rig-Veda was the lowest social unit but it was a “large family containing members of four generations.”
Thus grhapati would be the head of one such family, although elsewhere he suggests that the tribal chief could have been known by the title of grhapati. Romila Thapar thinks that the grhapatis were of 'higher lineage' in the Rig-Veda, that is, of the rajanya lineage, “since the term is brought in when describing the nuptials of the daughter of Surya …. Agni is called the grhapati and the sacred household fire is grhapatya.
Grhapatya here is obviously a mistake for the garhapatya fire and not for grhyagni. The garhapatya fire was not a sacred 'household fire', but one of the three srauta or public fires, the other two being ahavaniya and daksinagni. It is always differentiated from grhyagni, the household fire, also called vaivahika or smartagni.
The latter is meant for the purpose of daily offerings made twice, morning and evening. It is significant that the Grhyasutras speak of it as the nuptial (vaivahika) fire to be kindled on the day of marriage by the newly married couple, who are to keep it burning constantly. It may be allowed to go out if the wife is dead and the man wishes to remain a widower. Thus the distinction between the grhyagni and the garhapatyagni lies not in the fact that one represents the 'popular' and the other 'elite' diety, but that the former is the fire of the individual household for the purpose of daily offerings, and the latter a communal fire meant for seasonal or occasional purposes.
In the yatsattras, which were long sacrificial sessions ritualizing the eastward march of the Vedic Aryans, the garhapatya fire is to be built on the place where the yoke-pin of the chariot (samya) comes down. It is contend that the grhya, ritual built around the domestic fire seems to be a 'substitute' or 'replacement' of the cumbersome and elaborate srauta ritual, as there Is a basic similarity o structure and procedura.
Nevertheless, the practice of making daily offerings into the domestic fire may go back to Rig Vedic times. It was, however, quite distinct from the fire of the grhapati or garhapatyagni, which is mentioned in connection with the seasonal soma sacrifice in a Rig Vedic hymn addressed to the personified season (Rtu.)
The clue to the original significance of grhapati may be found in the sattra sacrifices. These are collective sacrifices to be performed by a band of sacrifices between the age of seventeen and twenty-four in company with their wives, who are given diksa along with their husbands.
In a sat- sacrifice there are no priests, the yajamanas or the sacrifices themselves act as priests and they choose one among them as their grhapati to perform all the necessary sacred acts in the course of the sacrifice, others merely touching him.
Nevertheless, the merit accruing out of the sacrifice is supposed to go to all of them equally. A passage of the Atharvaveda says that the sattras had become utsanna, that is, were no longer in vogue. This confirms their anarchic character. The rule that a sattra is to be performed by the brahmanas only was apparently formulated when the priestly function was confined to the brahmana varna. But the fact that the sacrificial utensils prepared for use in the course of the sacrifice were common to all sacrifices and also the stipulation of some sutras that all the participants of a sattra should belong to the same gotra indicates that originally the sattras must have been performed by bands of young men having common bonds of kinship.
The grhapati was the leader or chief of one such band. The inference tallies with the description of Agni-grhapati found in the first hymn of the VII mandal in which well-formed men (narah sujatah) and brave heroes (suvirah) are described as sitting together around the fire in the dwelling place. Perhaps, the offering of the grhamedha sacrifice to the Maruts, who are described as grhamedhasa, the sharers of grhamedha in the Rgveda is a reference to a sattra. The connection of the Maruts with grhamedha, is significant, as they are all young and form one collectivity (gana) and as such are especially connected with grha.
The Rig Vedic vocabulary is quite poor in kinship terms denoting an extended or joint family system. The wedding hymn found in the X mandala, in which it is wished that the bride may preside over a large joint family consisting of father-in-law, mother-in-law, sister-in-law and other kinsmen, appears to have been recast more than once by priestly hands and it has been pointed out that the language of the latter part of the hymn, which contains allusions to the joint family structure, is more akin to modern Sanskrit than to the Vedic. The solitary description of a large household with father, mother, kinsmen (jnatayah) and a number of women sleeping in the courtyard is found in a hymn of the VII mandala, but Ghate quotes it as an example of later interpolation.
It is also found in the Atharvaveda. It is held that the kin-based collectives are very prominent in the Rig-Veda although their precise nature is difficult to define. But unlike Atharvaveda, the Rig Vedic vocabulary is quite poor in kinship terms expressive of an extended family system.
We may suggest that owing to the solidarity of clan as a social and functional unit it may not have been very necessary to have specific terms distinguishing the elders and the juniors of different generations and lineages. Hence, Rig Vedic kinship terminology is classificatory. The term pitr stands for the father or ancestors as a whole and janitr is added to distinguish one's own father.
Similarly, while the terms sunu, tanaya and putra are used in the Rig-Veda to denote all descendants, the Atharavaveda uses them in a more restricted sense. The latter text has specific terms for grandfather (pi- tamaha), grandmother (matamaha), great grandfather iprapitamahd) and grandchild (naptr) which are absent in the Rig-Veda.
Kapadia has shown that whereas in the Rig-Veda offerings are made to the collectivity of ancestors known as pitrs, the Atharvaveda lays down in a more specific manner that three ascendant ancestors of the ego constitute his pitrs and they are to receive offerings for the manas.
A kinship terminology is a means of ordering relationships for social purposes. The Rig Vedic social structure seems to have been what the sociologists call the Omaha type in which ancestral lineages of several generations constituted one single united group, the principle of the unity of lineage-generations being “a method of expressing and emphasizing the unity and the solidarity of the patrilineal lineage group In any case, there is nothing to warrant the assertion that sons were treated as items of property for the labour power they provided for the family, for it is not shown that the family was the basic unit of production and the head of the family had patriarchal authority. References to pitrvitta or 'patrimonial wealth' should not be interpreted in the sense of individual inheritance but related to the conception of pitr in the Rig-Veda and hence would mean the “wealth bequeathed by the ancestors”.
The clan, also called 'sib' or 'gens', is the basic social unit among the people who are relatively settled but have not yet developed sufficient agriculture to support full political organization. The use of the term 'clan' with reference to the Rig Vedic people has been questioned recently on the ground that the case of exogamy is not proved. The objection is not very serious. In anthropological usage this term has been applied to societies which have gone beyond the “band” stage but have not developed a unilineal lineage structure.
In his definition of 'clan' Radcliffe-Brown remarks that the term clan “should be used only for a group having unilineal descent in which all the members regard one another in some specific sense kinsfolk. Frequently, but-not-universally, the recognition of the kinship bond uniting the members of the clan takes the form of a rule of exogamy which forbids marriage between the members of the same clan.”
We have avoided the use of the term 'lineage' in the Rig Vedic context as there is greater stress on genealogy and unilineal descent in lineage than in 'clan', though both models trace the descent from a real or mythical ancestor. In the Rig Vedic vocabulary it is the term vis. which seems to approximate to 'clan' and is generally interpreted as such by the Vedic scholars although some would prefer to interpret it simply as 'people' or 'settlement'. But the general trend of evolution being from a social entity to a physical, territorial entity, as is demonstrated in the rase of dama, vis seems to have been a kin unit. In the ancient Iranian its cognate vis denotes 'clan' or a group of several families, and it is quite likely that this was the case with early Vedic too.
On the other hand, the term jana which could mean both 'a person' as well as 'community', is also sometimes used in the sense of an exogamous social unit at least in the later Vedic sources. The Latyayana Srautasutra equates sagotra with samanajana and the janya or janyamitra mentioned in connection with the consecration ceremony is taken to stand for a person allied by marriage. The wife is called jani in the Rig-Veda.
The case for exogamy among the Indo-Aryans has been argued by a number of scholars including Benveniste, who remarks that the term and has a rather ambivalent meaning in the Rgveda-, it is used in the sense of a 'friend' or 'ally' in one context and 'enemy' or 'stranger' in another.
This suggests that ari formed a moiety in an exogamous society and hence its relationship was sometimes one of friendship and sometimes that of rivalry. 'Arya' was the common reciprocal term used by the members of moieties constituting one community to designate each other and “Aarya”, which meant the descendant of 'art' or 'arya' came to signify ail those tribes which belonged to the same cultural complex, recognized the same ancestors and worshipped the same gods.
Benveniste holds that the God Aryaman is the God of marriage and hospitality in the Rgveda and his function is to admit individuals into an exogamous community through marriage. “Aryaman intervenes when a woman taken from outside the clan is introduced for the first time as a wife into her new family.” In support of his thesis, Benvensite cites a verse of the Rig-Veda in which Indra's daughter-in-law states that all the aris have arrived but her father-in-law, Indra, is yet to come, meaning thereby that Indra was to her an ari, member of an exogamous clan.
The meaning of the term aril- larya continues to rouse controversy, and although some attribute to it the meaning of 'owner or possessor of wealth'. Paul Thieme's interpretation of the term as 'foreigner' or 'stranger' has given rise to a suggestion that the Arya/Dasa dichotomy should be seen as that between the 'invader' and the 'dweller' or 'native'.
Whatever the case may be, we have already shown that the contrast between Arya and Dasa at least in the initial stages is of an ethnic nature, the latter term acquiring a pejorative connotation due to this conflict. It could have been only with the complete subjugation of the Dasas that the term acquired the generic significance of 'slave' or servant and may have included such aborigines as Ibhyas, who are said to receive the reward of their labour once the charioteer is back and settled at home presumably after a hunting expedition. To conclude, the Rig-Vedic society was a simple society in which the ranking of individuals depended more upon personal qualities and skills than upon inherited wealth or status by birth.